सुरेन्द्र मोहन पाठक आज हिन्दी अपराध साहित्य के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले लेखक हैं। सन 2018 में जब उनकी आत्मकथा का पहला भाग न बैरी न कोई बैगाना प्रकाशित हुआ था तो मित्र राशीद शेख ने पुस्तक पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखी थी। उस वक्त यह लेख एक हिन्दी अखबार में भी प्रकाशित हुआ था। राशीद शेख का लिखा यह लेख बहुत ही खूबसूरत तरीके से किताब के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। आप भी पढ़िए।
*******
 |
| ना बैरी न कोई बैगाना – सुरेन्द्र मोहन पाठक |
 |
| राशीद शेख |
सुरेंद्र मोहन पाठक, एक ऐसा नाम जो लोकप्रिय साहित्य के क्षेत्र में विगत साठ वर्षों से सितारे की मानिंद चमक रहा है । पाठक साहब की पहली लघुकथा सन 1959 में “57 साल पुराना आदमी” के नाम से मनोहर कहानियाँ में छपी । उसके बाद से तो अब तक लगभग 300 किताबें उनकी छप चुकी हैं । इन दिनों सुरेंद्र मोहन पाठक अपनी आत्मकथा के पहले भाग “न बैरी न कोई बेगाना” के लिए चर्चा में हैं । आत्मकथा का शीर्षक गुरुग्रंथ साहिब में सिक्खों के पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव जी के लिखे शबद “ना कऊ बैरी-नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई” से लिया गया है । अपने आप में ये शबद जितना मानीखेज है उतनी ही मानीखेज इसकी शीर्षक में उपस्थिति भी है । लेखक ने अधिकांशतः सकारात्मक बातों का, घटनाओं का समावेश ही अपनी आत्मकथा में किया है या फिर कहा जा सकता है कि लेखक ने एक सकारात्मक जीवन जिया । आत्मकथा लिखने में सामने आने वाली मजबूरी के विषय में पाठक साहब लिखते हैं, “आत्मकथा लिखना, लोगों को दुश्मन बनाने का बेहतरीन तरीका है । मैं नहीं समझता ये खतरा मोल लिए बिना ईमानदाराना आत्मकथा लिखी जा सकती है” । वहीं वो हॉलीवुड के मूवी मुगल सैमुअल गोल्डविन को उद्धृत करते हैं, जिन्होंने कहा था “मेरी राय में आदमजात को अपनी आत्मकथा तब तक नहीं लिखनी चाहिए जब तक वो इस फानी दुनिया से रुख़सत ना पा जाए”, अर्थात कभी लिखनी ही नहीं चाहिए । लेखक ने लोगों को दुश्मन बनाने के इस काम को जिस जांमारी से पूरा किया है, वो काबिले तारीफ़ है ।
पाठक साहब ने अपनी आत्मकथा के पहले भाग में अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत की जो तस्वीर खींची है, वो बड़ी दिलकश है । पाठक साहब लिखते हैं:
“19 फरवरी , 1940 में जन्मा मैं अपने जीवन सफर में बस इतना पीछे जा सकता हूँ कि लाहौर की याद आती है जहाँ मेरे पिता की एक ब्रिटिश कंपनी में स्टेनोग्राफर की नौकरी थी और जहां वो मेरी मां और मेरी दो छोटी बहनों के साथ रहते थे । मुल्क के बंटवारे के वक़्त मैं साढ़े सात साल का था इसलिए जाहिर है कि जो भी याद जन्म से लेकर तब तक के वक़्फे के साथ वाबस्ता है वो लाहौर की है । लाहौर का शाह आलमी गेट एक दिल्ली के दरीबा, किनारी बाजार जैसा घनी आबादी वाला इलाका था । राहगुज़र गेट के भीतर से थी जिसके आगे दूर तक जाता घना बाज़ार था”
लेखक आज जीवित उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने बँटवारे का दर्द झेला, दोनों ओर मची मार-काट और लूट-पाट देखी । लेखक ने शायद सकारात्मक लेखन की अपनी जिद के तहत बँटवारे का उल्लेख बड़ा संक्षिप्त किया है और लिखते हैं:
“हर कोई खुद को तसल्ली देता था कि सच में ही कोई अनहोनी नहीं होने वाली । कैसे हो सकती थी ? हिन्दू-मुसलमानों में बेमिसाल भाईचारा था, रोटी-बोटी का रिश्ता था, कैसे कोई अनहोनी हो सकती थी ? हकीकतन तो ऐसा न हुआ ! हकीकतन तो तबाही, बरबादी और विस्थापन का ऐसा हाहाकार खड़ा हुआ जिसकी दूसरी मिसाल आज भी दुनिया में नहीं है।”
बँटवारे के बाद एक शरणार्थी के रूप में बिताए जीवन को भी पाठक साहब ने पन्नों पर यूँ उतारा है जैसे अपनी उँगली पकड़ा कर सैर कराई हो । बँटवारे के बाद लेखक ने दिल्ली में सपरिवार पनाह पाई और तत्कालीन दिल्ली और शरणार्थियों की समस्याओं, उनकी जीवनचर्या, ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाने की उनकी जद्दोजहद का बड़ा सजीव चित्रण किया है, वे लिखते हैं
“बँटवारे के बाद दिल्ली में शरणार्थियों का इनफ्लक्स इतना वसीह था जैसे कि खलकत का कोई सैलाब उमड़ आया था । तकरीबन शरणार्थी ऐसे थे जो कि पीछे सब कुछ गँवा कर आए थे, जिन का दिल्ली में कोई ठिकाना नहीं था और न ही -अस्थायी या स्थायी- ठिकाना बना पाने की हैसियत थी । ऐसे हुजूम के हुजूम परिवारों की पनाहगाह तब या पुराना किला थी या किंग्सवे कैम्प थी जहाँ शरणार्थियों के लिए विशेष रूप से बेशुमार तम्बू खड़े किए गए थे । जो बिल्कुल ही लुट पिट कर नहीं आए थे, या जो मेरे पिता की तरह कदरन किस्मत वाले थे कि फौरन नया रोजगार पा गए थे, उन्होंने शाहदरा जैसी जगहों पर किराए के मकान लिये और इस सिलसिले में पहले से लूटे लोगों को स्थानीय मकान मालिकों ने खूब लूटा । जिस पोर्शन का पाँच रुपया माहाना किराया मुश्किल से मिलता था, उन्हें रिफ्यूजियों को पचास रुपये माहाना किराये पर उठाया”
उस दौर के शाहदरा जहाँ कि लेखक की रिहायश थी में उपलब्ध खान-पान का भी लेखक ने बड़ा विवरणात्मक वर्णन किया है जिसे पढ़कर पढ़ने वाले के मुँह में भी बरबस पानी भर आता है । लेखक ने वहाँ मिलने वाले गोलगप्पों, आलू की टिक्की, छोले-भटुरों, बालूशाही, देसी घी, दाल के लड्डू, स्पंजी रसगुल्लों और मटका कुल्फी का जिक्र किया है। मटका कुल्फी बेचने वालों को विशेष रूप से याद करते हुए लेखक लिखते हैं:
“ऐसे फेरीवालों के साथ मटका उठाने के लिए एक नौकर होता था जिसके आगे-आगे वो चलता था । कोई ग्राहक रोकता था तो कुल्फी उसे वो सर्व करता था लेकिन अदायगी के पैसों को वो हाथ नहीं लगाता था, वो नौकर को थमाने होते थे । वो मालिक था आखिर, मुनीमी भला वो कैसे कर सकता था !”
तत्कालीन मनोरंजन के साधनों का बड़ा मजेदार उल्लेख लेखक ने किया है । शाहदरा, दिल्ली के सिनेमाहालों, उनकी व्यवस्था, टिकट लेने आदि का बड़ा खुबसुरत वर्णन लेखक ने किया है । वहीं कठपुतली के तमाशे, रामलीला के मंचन, उनके कलाकारों की संवाद अदायगी वगैरह पढ़ के आनंद ही आ जाता है और पाठक उनमें खो सा जाता है । लेखक अपने स्थाई पात्र सुनील, जो कि एक पत्रकार है कि तरह यारबाश भी है । अब क्योंकि सुनील का जिक्र आया है तो साथ-साथ ये बताना संदर्भहीन न होगा कि एक ऐसे दौर में जब जासूसी उपन्यासों के अधिकांश हीरो पुलिस इंस्पेक्टर, सीआईडी के जासूस, सेना के कर्नल जैसे थे वहाँ लेखक ने एक प्रेस रिपोर्टर को अपना हीरो बनाया, न सिर्फ बनाया बल्कि उसके एक नहीं, दो नहीं पूरे 121 नावेल अब तक छप चुके हैं जो शायद एक रिकार्ड होगा । कम से कम मेरी जानकारी में आज तक सिर्फ एक पात्र को लेकर इतनी रचनाएं प्रकाशित नहीं हुई हैं । बहरहाल बात फिर से पाठक साहब की यारबाशी की । पाठक साहब ने बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था के यारबाशी के किस्से बड़ी खूबी से सुनाए हैं । यारबाशी के ये किस्से हमको-आपको भी अपनी यारबाशी याद दिला देते हैं। पाठक साहब के जो दोस्त बाद में नामी-गिरामी शख्सियत बने उनमें उपन्यास लेखक वेदप्रकाश काम्बोज और गजल गायक जगजीत सिंह प्रमुख हैं । हालाँकि उनके दोस्तों की फेहरिस्त में जनप्रिय लेखक ओमप्रकाश शर्मा का भी नाम शामिल है लेकिन उन्हें दोस्त से अधिक एक प्रेरक के रूप में ही पाठक साहब ने याद किया है । जगजीत सिंह के साथ पाठक साहब ने डीएवी कालेज जालंधर में तीन साल पढ़ाई की । जगजीत सिंह के साथ गुजारे समय को पाठक साहब ने बहुत ही अच्छे से लिखा है, विशेष रूप से लोहड़ी के अवसर को याद करते हुए वो लिखते हैं :
“लोहड़ी पंजाब का एक विशिष्ट त्योहार है जो पंजाब के अलावा कहीं नहीं होता । वो कोई बड़ा त्योहार नहीं माना जाता था इसलिए उस रोज कालेज में छुट्टी तक नहीं होती थी लेकिन शाम को वार्डन की ओर से बोर्डर्स के लिए लोहड़ी का विशिष्ट आयोजन होता था । सेंट्रल लॉन में बाकायदा अलाव जलाया जाता था और बोर्डर्स में मूँगफली, रेवड़ी, गजक बांटी जाती थी । साथ में कोई दो-ढाई घन्टे का रंगारंग प्रोग्राम होता था जिसके लिए खासतौर से आल इन्डिया रेडियो जालंधर से नामी, एंटरटेनमेंट में सिद्धहस्त कलाकार बुलाए जाते थे जिस में बतौर लोकल टैलेंट हमेशा जगजीत सिंह की शिरकत होती थी अलबत्ता स्टेज पर उसकी बारी तभी आती थी जब कि आमंत्रित नामी कलाकार अपने हुनर की बानगी पेश कर चुके होते थे । तब तक काफी हद तक महफिल उखड़ चुकी होती थी और ओपन एयर की सर्दी से निजात पाने के लिये विद्यार्थी उतावले होने लग चुके होते थे । ऐसे अनमने माहौल में जगजीत सिंह को स्टेज पर आकर कुछ सुनाने को बोला जाता था । होस्टल में मेरे स्टे के दौरान तीन साल में तीन बार लोहड़ी आयी और तीनों बार जगजीत सिंह ने लोहड़ी का एक स्वरचित गीत सुनाया । पहली बार जब ऐसा हुआ तो जगजीत सिंह ने अभी पहली लाइन गायी थी कि उंघते उकताये सारे विद्यार्थी तत्काल सजग हो गये, अनमनापन पता नहीं कहां गायब हो गया, सब मंत्रमुग्ध टेलएण्ड पर स्टेज पर अवतरित हुए जगजीत सिंह को सुनने लगे:
एह तां जग दियां लोहड़ियां,
साडी कादी लोहड़ी अक्खां सजना ने मोडियां ।
जब तक गाना खत्म होता था तब तक वहाँ एक भी आँख ऐसी नहीं होती थी जो कि नम न हो । कितने ही विद्यार्थी तो बेकाबू होकर जार जार रो रहे होते थे ।
फिर गगनभेदी करतल ध्वनि होती थी ।
ऐसी जैसी कि उस शाम की किसी भी आइटम पर नहीं हुई होती थी ।
और दो साल वो गाना जगजीत सिंह ने लोहड़ी के उपलक्ष्य में गाया । सबको पता होता था कि आगे क्या आने वाला है, फिर भी गाना शुरू होते ही श्रोताओं के गले रूंध जाते थे और हर कोई सुबकने लगता था । आवाज जगजीत सिंह की होती थी, दिल हर किसी का हूक मारता था ।“
आमतौर पर आत्मकथाओं को बोर माना जाता है लेकिन अपने जासूसी उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध सुरेन्द्र मोहन पाठक की आत्मकथा भी उनके जासूसी उपन्यासों की ही तरह रोचक और मनोरंजन से भरपूर है । सुरेन्द्र मोहन पाठक को पाठकों का प्रिय लेखक जिन हालातों, जिन जिजीविषाओं ने बनाया, उन्हें पढ़ना बहुत रूचिकर है । सुरेन्द्र मोहन पाठक को पढ़ने वाले पाठकों का का एक विशिष्ट वर्ग है, जिनकी संख्या लाखों में है और शायद यही कारण है कि ऐसे समय में जब बड़े से बड़े साहित्यकार की नवीनतम किताब की अधिकतम 5-10 हजार प्रतियां छपतीं हैं वहीं सुरेन्द्र मोहन पाठक के उपन्यासों का पहला प्रिंट आर्डर ही 50 हजार प्रतियों का होता है जो हाथों-हाथ बिक जाता है । मेरी जानकारी में भारत वर्ष में सुरेन्द्र मोहन पाठक ही ऐसे लेखक हैं जिनके फैंस क्लब स्थापित हैं। ऐसे लेखक की आत्मकथा यदि तीन भागों में आ रही है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं।
– राशीद शेख
********
राशीद शेख के ‘एक बुक जर्नल’ में प्रकाशित अन्य लेख:
राशीद शेखलेखक सुरेन्द्र मोहन पाठक की आत्मकथा का दूसरा भाग
‘हम नहीं चंगे बुरा न कोय’ भी प्रकाशित हो चुका है। उसे आप निम्न लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं:
किंडल |
पेपरबैकनोट: अगर आप भी हमें लेख भेजना चाहें तो उन्हें contactekbookjournal@gmail.com पर भेज सकते हैं।
नोट: लेख पर लेखक का कॉपीराइट है। उनकी अनुमति के बिना इसे कहीं और प्रकाशित न किया जाए।
© विकास नैनवाल ‘अंजान’
-
'एक बुक जर्नल' साहित्य को समर्पित एक वेब पत्रिका है जिसका मकसद साहित्य की सभी विधाओं की रचनाओं का बिना किसी भेद भाव के प्रोत्साहन करना है।
सन् 2012 से हम यह कार्य निरंतर रूप से कर रहे हैं। यह प्रोत्साहन रचनाओं के ऊपर पाठकीय टिप्पणी प्रकाशित करके, नयी साहित्यिक कृतियों की जानकारी साझा करके, साहित्य से जुड़ी खबरे साझा करके और लेखकों द्वारा भेजी गयी उनकी रचनाओं को प्रकाशित करके किया जाता है। हमारी कोशिश है एक वृहद पाठक वर्ग तक इन जानकारियों को पहुँचाया जाए।
आप भी साहित्य और लेखन से सम्बंधित लेख, अपनी पुस्तक का अंश और अपनी रचनाएँ हमें भेज कर इस मुहिम में सहयोग दे सकते हैं।
हमारा पता है: contactekbookjournal@gmail.com


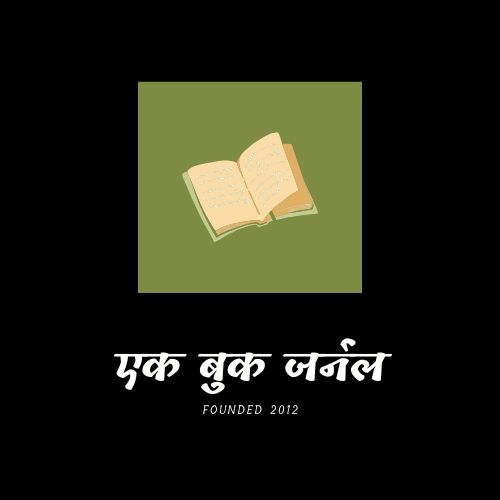

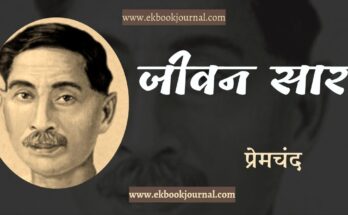
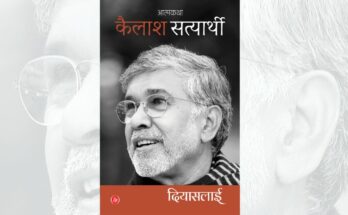
आपकी इस प्रविष्टि् की चर्चा कल बुधवार (18-11-2020) को "धीरज से लो काम" (चर्चा अंक- 3889) पर भी होगी।
—
सूचना देने का उद्देश्य है कि यदि किसी रचनाकार की प्रविष्टि का लिंक किसी स्थान पर लगाया जाये तो उसकी सूचना देना व्यवस्थापक का नैतिक कर्तव्य होता है।
—
हार्दिक शुभकामनाओं के साथ।
सादर…!
डॉ.रूपचन्द्र शास्त्री 'मयंक'
—
चर्चाअंक में मेरी प्रविष्टि को शामिल करने के लिए आभार, सर।
इतने सजग अनुभव अब इतिहास बन गए हैं.
जी आभार….
बेहतरीन….
जी आभार…