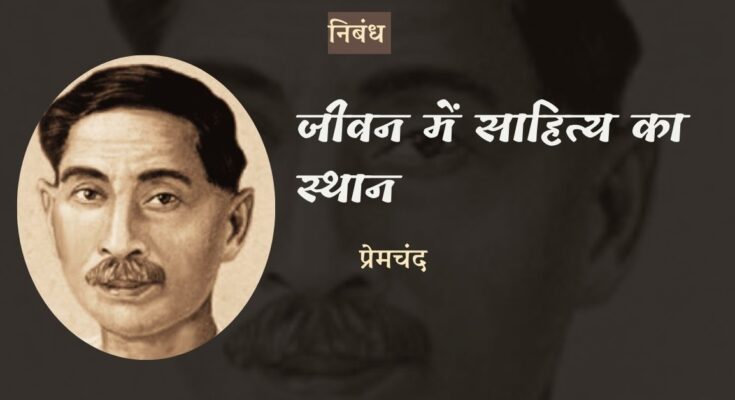साहित्य का आधार जीवन है। इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटरियाँ, मीनार और गुम्बद बनते हैं लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। उसे देखने को भी जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं, हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून हैं, जिनसे वह इधर-उधर नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवनपर्यंत आनंद ही की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे-पूरे परिवार में, किसी को लम्बे-चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊँचा है, इससे पवित्र है, उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है, उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य या भोग के आनंद में ग्लानि छिपी होती है। उससे अरूचि भी हो सकती है, पश्चात्ताप भी हो सकता है पर सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है, वह अखंड है, अमर है।
साहित्य के नौ रस कहे गए हैं। प्रश्न होगा, वीभत्स में भी कोई आनंद है? अगर ऐसा न होता, तो वह रसों में गिना ही क्यों जाता? हाँ, है। वीभत्स में सुंदर और सत्य मौजूद है। भारतेंदु ने श्मशान का जो वर्णन किया है, वह कितना वीभत्स है! प्रेतों और पिशाचों का अधजले मांस के लोथड़े नोचना, हड्डियों को चटर-चटर चबाना, वीभत्स की पराकाष्ठा है लेकिन वह वीभत्स होते हुए भी सुंदर है क्योंकि उसकी सृष्टि पीछे आने वाले स्वर्गीय दृश्य के आनंद को तीव्र करने के लिए ही हुई है। साहित्य तो हर एक रस में खोजता है राजा के महल में, रंक की झोपड़ी के शिखर पर, गंदे नालों के अंदर, ऊषा की लाली में, सावन-भादों की अँधेरी रात में। और यह आश्चर्य की बात है कि रंक की झोपड़ी में जितनी आसानी से सुंदर मूर्तिमान दिखाई देता है, महलों में नहीं। महलों में तो वह खोजने से मुश्किलों से मिलता है।
जहाँ मनुष्य अपने मौलिक, यथार्थ, अकृत्रिम रूप में है, वहीं आनंद है। आनंद कृत्रिमता और आडम्बर से कोसों दूर भागता है। सत्य का कृत्रिम से क्या सम्बंध? अतएव हमारा विचार है कि साहित्य में केवल एक रस है और वह शृंगार है। कोई रस साहित्यिक दृष्टि से रस नहीं रहता और न उस रचना की गणना साहित्य में की जा सकती है, जो शृंगारविहीन और अ-सुंदर हो, जो रचना केवल वासना-प्रधान हो, जिसका उद्देश्य कुत्सित भावों को जागाना हो, जो केवल बाह्य जगत् से सम्बंध रखे, वह साहित्य नहीं है। जासूसी उपन्यास अद्भुत होता है। लेकिन हम उसे साहित्य उसी वक्त कहेंगे, जब उसमें सुंदर का समावेश हो। खूनी का पता लगाने के लिए सतत उद्योग, नाना प्रकार के कष्टों का झेलना, न्याय-मर्यादा की रक्षा करना, ये भाव हैं, जो इस अद्भुत रस की रचना को सुंदर बना देते हैं।
सत्य से आत्मा का सम्बंध तीन प्रकार का है। एक जिज्ञासा का सम्बंध है, दूसरा प्रयोजन का सम्बंध है और तीसरा आनंद का। जिज्ञासा का सम्बंध दर्शन का विषय है, प्रयोजन का सम्बंध विज्ञान का विषय है और साहित्य का विषय केवल आनंद का सम्बंध है। सत्य जहाँ आनंद का स्त्रोत बन जाता है, वहीं वह साहित्य हो जाता है। जिज्ञासा का सम्बंध विचार से है, प्रयोजन का सम्बंध स्वार्थ-बुद्धि से। आनंद का सम्बंध मनोभावों से है। साहित्य का विकास मनोभावों द्वारा ही होता है। एक ही दृश्य या घटना या कांड को हम तीनों ही भिन्न-भिन्न नजरों से देख सकते हैं। हिम से ढँके हुए पर्वत पर ऊषा का दृश्य दार्शनिक के गहरे विचार की वस्तु है, वैज्ञानिक के लिए अनुसंधन की और साहित्यिक के लिए विह्नलता की! विह्नलता एक प्रकार का आत्म-समर्पण है। यहाँ हम पृथकता का अनुभव नहीं करते। यहाँ ऊँचे-नीच, भले-बुरे का भेद नहीं रह जाता। श्रीरामचंद्र शबरी के जूठे बेर क्यों प्रेम से खाते हैं, कृष्ण भगवान् विदुर के शाक को क्यों नाना व्यंजनों से रूचिकर समझते हैं इसलिए कि उन्होंने इस पार्थक्य को मिटा दिया है। उनकी आत्मा विशाल है। उसमें समस्त जगत् के लिए स्थान है। आत्मा आत्मा से मिल गई है। जिसकी आत्मा जितनी ही विशाल है वह उतना ही महापुरूष है। यहाँ तक कि ऐसे महान् पुरूष भी हो गए हैं, जो जड़ जगत् से भी अपनी आत्मा का मेल कर सके हैं।
आइए देखें, जीवन क्या है? जीवन केवल जीना, खाना, सोना और मर जाना नहीं है। यह तो पशुओं का जीवन है। मानव-जीवन में भी यह सब प्रवृत्तियाँ होती हैं, क्योंकि वह भी तो पशु है। पर इसके उपरांत कुछ और भी होता है। उसमें कुछ ऐसी मनोवृत्तियाँ होती हैं, जो प्रकृति के साथ हमारे मेल में बाधक होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं, जो इस मेल में सहायक बन जाती हैं। जिन प्रवृत्तियों में प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य बढ़ता है, वह वांछनीय होती हैं जिनसे सामंजस्य में बाधा उत्पन्न होती है, वे दूषित हैं। अहंकार, क्रोध या द्वेष हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियाँ हैं। यदि हम इनको बेरोकटोक चलने दें, तो निस्संदेह वह हमें नाश और पतन की ओर ले जाएँगी। इसलिए हमें उनकी लगाम रोकनी पड़ती है, उन पर संयम रखना पड़ता है, जिनसे वे अपनी सीमा से बाहर न जा सकें। हम उन पर जितना कठोर संयम रख सकते हैं, उतना ही मंगलमय हमारा जीवन हो जाता है।
किंतु नटखट लड़कों से डाँटकर कहना, तुम बड़े बदमाश हो, हम तुम्हारे कान पकड़कर उखाड़ लेंगे, अक्सर व्यर्थ ही होता है, बल्कि उस प्रवृत्ति को और हठ की और ले जाकर पुष्ट कर देता है। ज़रूरत यह होती है कि बालक में जो सद्वृत्तियाँ हैं, उन्हें उत्तेजित किया जाय कि दूषित वृत्तियाँ स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएँ। इसी प्रकार मनुष्य को भी आत्मविकास के लिए संयम की आवश्यकता होती हैं। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है। सत्य को रसों द्वारा हम जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते, उसी भाँति जैसे दुलार-चुमकारकर बच्चों को जितनी सफलता से वश में किया जा सकता है, डाँट-फटकार से सम्भव नहीं। कौन नहीं जानता कि प्रेम से कठोर से कठोर प्रकृति को नरम किया जा सकता है। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश असफल होता है, वहाँ साहित्य बाजी ले जाता है। यही कारण है कि हम उपनिषदों और अन्य धर्म-ग्रंथों को साहित्य की सहायता लेते देखते हैं! हमारे धर्माचार्यो ने देखा कि मनुष्य पर सबसे अधिक प्रभाव मानव-जीवन की वे दुख-सुख के वर्णन से ही हो सकता है और उन्होंने मानव-जीवन की वे कथाएँ रचीं, जो आज भी हमारे आनंद की वस्तु हैं। बौद्धों की जातक-कथाएँ, तोरेह, कुरान, इंजील ये सभी मानवी कथाओं के संग्रह-मात्र हैं। उन्हीं कथाओं पर हमारे बड़े-बड़े धर्म स्थिर हैं। वही कथाएँ धर्मो की आत्मा हैं। उन कथाओं को निकाल दीजिए, तो उस धर्म का अस्तित्व मिट जायेगा। क्या उन धर्म-प्रवर्तकों ने अकारण ही मानवी जीवन की कथाओं का आश्रय लिया? नहीं, उन्होंने देखा कि हृदय द्वारा ही जनता की आत्मा तक अपना संदेश पहुँचाया जा सकता है। वे स्वयं विशाल हृदय के मनुष्य थे। उन्होंने मानव-जीवन से अपनी आत्मा का मेल कर लिया था। समस्त मानव-जाति से उनके जीवन का सामंजस्य था, फिर वे मानव-चरित्र की उपेक्षा कैसे करते?
आदिकाल से मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। हम जिसके सुख-दुःख हँसने-रोने का मर्म समझ सकते हैं, उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, कृषक को कृषक जीवन से जितनी रूचि है, उतनी अन्य जातियों से नहीं, लेकिन साहित्य जगत् में प्रवेश पाते ही यह भेद, यह पार्थक्य मिट जाता है। हमारी मानवता जैसे विशाल और विराट् होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है। मानव जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन सभी उसके अधिकार में आ जाते हैं। उसे मानो विश्व की आत्मा पर साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। श्री रामचंद्र राजा थे, पर आज रंक भी उनके दुःख से उतना ही प्रभावित होता है, जितना कोई राजा हो सकता है।
साहित्य वह जादू की लकड़ी है, जो पशुओं में, ईंट-पत्थरों में, पेड़-पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मानव हृदय का जगत्, इस प्रत्यक्ष जगत् जैसा नहीं है। हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत् के प्राणियों में अपने को अधिक जानते हैं, उसके सुख-दुख, हर्ष और विषाद से ज्यादा विचलित होते हैं। हम अपने निकटतम बंधु-बांधवों से अपने को इतना निकट नहीं पाते, इसलिए कि हम उसके एक-एक विचार, एक-एक उद्गार को जानते हैं। उसका मन हमारी नजरों के सामने आईने की तरह खुला हुआ है। जीवन में ऐसे प्राणी हमें कहाँ मिलते हैं, जिनके अंतःकरण में हम इतनी स्वाधीनता से विचर सकें? सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भावों में व्यापकता हो, उसने विश्व की आत्मा से ऐसी ‘हारमनी’ प्राप्त कर ली हो कि उसके भाव प्रत्येक प्राणी को अपने ही भाव मालूम हों।
साहित्यकार बहुधा अपने देश-काल से प्रभावित होता है। जब कोई लहर देश में उठती है, तो साहित्यकार के लिए उससे अविचलित रहना असम्भव हो जाता है। उसकी विशाल आत्मा अपने देश-बंधुओं के कष्टों से विकल हो उठती है और इस तीव्र विकलता में वह रो उठता है, पर उसके रूदन में भी व्यापकता होती है। वह स्वदेश का होकर भी सार्वभौमिक रहता है। ‘टॉम काका की कुटिया’ गुलामी की प्रथा से व्यथित हृदय की रचना है, पर आज उस प्रथा के उठ जाने पर भी उसमें वह व्यापकता है कि हम लोग उसे पढ़कर मुग्ध हो जाते हैं। सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता। वह सदा नया बना रहता है। दर्शन और विज्ञान समय की गति के अनुसार बदलते हैं पर साहित्य तो हृदय की वस्तु है और मानव-हृदय में तबदीलियाँ नहीं होतीं। हर्ष और विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय, आज भी हमारे मन पर उसी तरह अधिकृत हैं, जैसे आदिकवि बाल्मीकि के समय में थे और कदाचित् अनंत तक रहेंगे। रामायण के समय का समय अब नहीं है, महाभारत का समय भी अतीत हो गया, पर ये ग्रंथ अभी तक नये हैं। साहित्य ही सच्चा इतिहास है, क्योंकि उसमें अपने देश और काल का जैसा चित्र होता है, वैसा कोरे इतिहास में नहीं हो सकता। घटनाओं की तालिका इतिहास नहीं है और न राजाओं की लड़ाइयाँ ही इतिहास है। इतिहास जीवन के विभिन्न अंगों की प्रगति का नाम है और जीवन पर साहित्य से अधिक प्रकाश और कौन वस्तु डाल सकती है, क्योंकि साहित्य अपने देशकाल का प्रतिबिम्ब होता है।
जीवन में साहित्य की उपयोगिता के विषय में कभी-कभी संदेह किया जाता है। कहा जाता है जो स्वभाव से अच्छे हैं, वह अच्छे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी पढ़ें। जो स्वभाव से बुरे हैं, वह बुरे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी पढ़ें। इस कथन में सत्य की मात्रा बहुत कम है। इसे सत्य मान लेना मानव-चरित्र को बदल देना होगा। जो सुंदर है, उसकी ओर मनुष्य का स्वाभाविक आकर्षण होता है। हम कितने ही पतित हो जाएँ पर असुंदर की ओर हमारा आकर्षण नहीं हो सकता। हम कर्म चाहे कितने ही बुरे करें, पर यह असम्भव है कि करूणा और दया और प्रेम और भक्ति का हमारे दिलों पर असर न हों। नादिरशाह से ज्यादा निर्दयी मनुष्य और कौन हो सकता है हमारा आशय दिल्ली में कत्लेआम करानेवाले नादिरशाह से है। अगर दिल्ली का कत्लेआम सत्य घटना है, तो नादिरशाह के निर्दय होने में कोई संदेह नहीं रहता। उस समय आपको मालूम है, किस बात से प्रभावित होकर उसने कत्लेआम बंद करने का हुक्म दिया था? दिल्ली के बादशाह का वज़ीर एक रसिक मनुष्य था। जब उसने देखा कि नादिरशाह का क्रोध किसी तरह नहीं शांत होता और दिल्ली वालों के खून की नदी बहती चली जाती है, यहाँ तक कि खुद नादिरशाह के मुँहलगे अफसर भी उसके सामने आने का साहस नहीं करते, तो वह हथेलियों पर जान रखकर नादिरशाह के पास पहुँचा और यह शेर पढ़ा
‘कसे न माँद कि दीगर ब तेग़े नाज कुशी।
मगर कि जिंदा कुनी खल्क रा व बाज कुशी।’
इसका अर्थ यह हुआ कि तेरे प्रेम की तलवार ने अब किसी को जिंदा न छोड़ा अब तो तेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि तू मुर्दो फिर जिला दे और फिर उन्हें मारना शुरू करे। यह फारसी के एक प्रसिद्ध कवि का श्रृंगार-विषयक शेर है पर इसे सुनकर कातिल के दिल में मनुष्य जाग उठा। इस शेर ने उसके हृदय के कोमल भाग को स्पर्श कर दिया और कत्लेआम तुरंत बंद कर दिया गया।
नेपोलियन के जीवन की वह घटना भी प्रसिद्ध है, जब उसने एक अंग्रेज मल्लाह को झाऊँ की नाव पर कैले का समुद्र पार करते देखा। जब फ्रांसीसी अपराधी मल्लाह को पकड़कर नेपोलियन के सामने लाये और उसने पूछा, तू इस भंगुर नौका पर क्यों समुद्र पार कर रहा था, तो अपराधी ने कहा, इसलिए कि मेरी वृद्धा माता घर पर अकेली है, मैं उसे एक बार देखना चाहता था। नेपोलियन की आँखों में आँसू छलछला आये। मनुष्य का कोमल भाग स्पंदित हो उठा। उसने उस सैनिक को फ्रांसीसी नौका पर इंग्लैंड भेज दिया।
मनुष्य स्वभाव से देवतुल्य है। जमाने के छल-प्रपंच या और परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह अपना देवत्व खो बैठता है। साहित्य इसी देवत्व को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है, उपदेशों से नहीं, नसीहतों से नहीं, भावों को स्पंदित करके, मन के कोमल तारों पर चोट लगाकर प्रकृति से सामंजस्य उत्पन्न करके। हमारी सभ्यता साहित्य पर ही आधारित है। हम जो कुछ हैं, साहित्य के ही बनाए हैं। विश्व की आत्मा के अंतर्गत भी राष्ट्र या देश की एक आत्मा होती है। इसी आत्मा की प्रतिध्वनि है – साहित्य।
योरप का साहित्य उठा लीजिए। आप वहाँ संघर्ष पाएँगे। कहीं खूनी कांडों का प्रदर्शन है, कहीं जासूसी कमाल का। जैसे सारी संस्कृति उन्मत्त होकर मरू में जल खोज रही है। उस साहित्य का परिणाम यही है कि वैयक्तिक स्वार्थपरायणता दिन-दिन बढ़ती जाती है, अर्थ-लोलुपता की कहीं सीमा नहीं, नित्य दंगे, नित्य लड़ाइयाँ। प्रत्येक वस्तु स्वार्थ के काँटे पर तौली जा रही है। यहाँ तक कि अब किसी यूरोपियन महात्मा का उपदेश सुनकर भी संदेह होता है कि इसके परदे में स्वार्थ न हो।
साहित्य सामाजिक आदर्शो का स्रष्टा है। जब आदर्श ही भ्रष्ट हो गया, तो समाज के पतन में बहुत दिन नहीं लगते। नयी सभ्यता का जीवन 150 साल से अधिक नहीं, पर अभी से संसार उससे तंग आ गया है, पर इसके बदले में उसे कोई ऐसी वस्तु नहीं मिल रही है, जिसे वहाँ स्थापित कर सके। उसकी दशा उस मनुष्य की-सी है, जो यह तो समझ रहा है कि वह जिस रास्ते पर जा रहे है, वह ठीक रास्ता नहीं है, पर वह इतनी दूर जा चुका है कि अब लौटने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। वह आगे ही जायेगा, चाहे उधर कोई समुद्र ही क्यों न लहरें मार रहा हो। उसमें नैराश्य का हिंसक बल है, आशा की उदार शक्ति नहीं।
भारतीय साहित्य का आदर्श उसका त्याग और उत्सर्ग है। योरप का कोई व्यक्ति लखपती होकर, जायदाद खरीदकर, कम्पनियों में हिस्से लेकर और ऊँची सोसाइटी में मिलकर अपने को कृतकार्य समझता है। भारत अपने को उस समय कृतकार्य समझता है, जब वह इस माया-बंधन से मुक्त हो जाता है, जब उसमें भोग और अधिकार का मोह नहीं रहता। किसी राष्ट्र की सबसे मूल्यवान सम्पत्ति उसके साहित्यिक आदर्श होते हैं। व्यास और वाल्मीकि ने जिन आदर्शो की सृष्टि की, वह आज भी भारत का सिर ऊँचा किये हुए हैं। राम अगर वाल्मीकि के साँचे में न ढलते, तो राम न रहते। सीता भी उसी साँचे में ढलकर सीता हुई। यह सत्य है कि हम सब ऐसे चरित्रों का निर्माण नहीं कर सकते, पर धन्वंतरि के एक होने पर भी संसार में वैद्यों की आवश्यकता है और रहेगी।
ऐसा महान् दायित्व जिस पर है, उसके निर्माताओं का पद कुछ कम जिम्मेदारी का नहीं है। कलम हाथ में लेते ही हमारे सिर पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है। हम साधारणतः युवावस्था में हमारी निगाह पहले विध्वंस करने की ओर उठ जाती है। हम सुधार करने की धुन में अंधाधुंध शर चलाना शुरू करते हैं। खुदाई फौजदार बन जाते हैं। तुरंत आँखें काले धब्बों की ओर पहुँच जाती हैं। यथार्थवाद के प्रवाह में बहने लगते हैं, बुराइयों के नग्न चित्र खींचने में कला की कृतकार्यता समझते हैं। यह सत्य है कि कोई मकान गिराकर ही उसकी जगह नया मकान बनाया जाता है, पुराने ढकोसलों और बंधनों को तोड़ने की जरूरत है, पर इसे साहित्य नहीं कह सकते। साहित्य तो वही है, जो साहित्य की मर्यादाओं का पालन करे।
हम अक्सर साहित्य का मर्म समझे बिना ही लिखना शुरू कर देते हैं। शायद हम समझते हैं कि मजेदार, चटपटी और ओजपूर्ण भाषा में लिखना ही साहित्य है। भाषा भी साहित्य का अंग है, पर स्थायी साहित्य विध्वंस नहीं करता, निर्माण करता है। वह मानव-चरित्र की कालिमाएँ नहीं दिखाता, उसकी उज्ज्वलताएँ दिखाता है। मकान गिरानेवाला इंजीनियर नहीं कहलाता। इंजीनियर तो निर्माण ही करता है। हममें जो युवक साहित्य को अपने जीवन का ध्येय बनाना चाहते हैं, उन्हें बहुत आत्मसंयम की आवश्यकता है, क्योंकि वह अपने को एक महान् पद के लिए तैयार कर रहे हैं, जो अदालतों में बहस करने या कुर्सी पर बैठकर मुक़दमे का फैसला करने से कहीं ऊँचा है। उसके के लिए केवल डिग्रियाँ और ऊँची शिक्षा काफी नहीं। चित्त की साधना, संयम, सौंदर्य-तत्व का ज्ञान, इसकी कहीं ज्यादा ज़रूरत है।
साहित्यकार को आदर्शवादी होना चाहिए। भावों का परिमार्जन भी उतना ही वांछनीय है। जब तक हमारे साहित्य-सेवी इस आदर्श तक न पहुँचेंगे, तब तक हमारे साहित्य से मंगल की आशा नहीं की जा सकती। अमर साहित्य के निर्माता विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य नहीं थे। वाल्मीकि और व्यास दोनों तपस्वी थे। सूर और तुलसी भी विलासिता के उपासक न थे। कबीर भी तपस्वी ही थे।
हमारा साहित्य अगर आज उन्नति नहीं करता, तो इसका कारण यही है कि हमने साहित्य-रचना के लिए कोई तैयारी नहीं की। दो-चार नुस्ख़े याद करके हकीम बन बैठे। साहित्य का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है और हमारी ईश्वर से यही याचना है कि हममें सच्चे साहित्य-सेवी उत्पन्न हों, सच्चे तपस्वी, सच्चे आत्मज्ञानी।
(हंस, 1932,अप्रैल अंक)