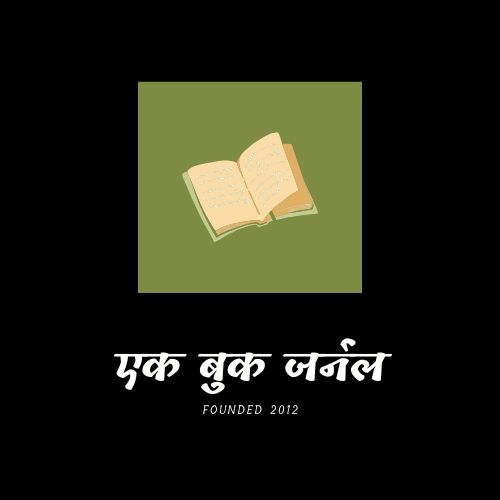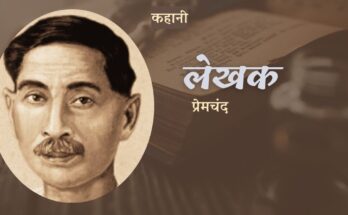लोग मुझे उन्मादिनी कहते हैं। क्यों कहते हैं, यह तो कहने वाले ही जानें, किंतु मैंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसमें उन्माद के लक्षण हों। मैं अपने सभी काम नियम-पूर्वक करती हूँ। क्या एक भी दिन मैं उस समाधि पर फूल चढ़ाना भूली हूँ? क्या ऐसी कोई भी संध्या गयी है जब मैंने वहाँ दीपक नहीं जलाया है? कौन सा ऐसा सबेरा हुआ है जब ओस से धुली हुई नयी-नयी कलियों से मैंने उस समाधि को नहीं ढँक दिया? फिर भी मैं उन्मादिनी हूँ! यदि अपने किसी आत्मीय के सच्चे और निःस्वार्थ प्रेम को समझने और उसके मूल्य करने को ही उन्माद कहते हैं, तो ईश्वर ऐसा उन्माद सभी को दे। क्या कहा–वह मेरा कौन था? यह तो मैं भी नहीं कह सकती, पर कोई था अवश्य, और ऐसा था, मेरे इतने निकट था कि आज वह समाधि में सोया है और मैं बावली की तरह उसके आस-पास फेरी देती हूँ। उसकी और मेरी कहानी भिन्न-भिन्न तो नहीं है। जो कुछ है यही है। सुनो–
बचपन से ही मुझे कहानी सुनने का शौक था। मैं बहुत–सी कहानियाँ सुना करती और मुझे उनका वह भाग बहुत ही प्रिय लगता, जहाँ किसी युवक की वीरता का वर्णन होता। मैंने वीरता की परिभाषा अपनी अलग ही बना ली थी। यदि कोई युवक किसी शेर को भी मार डाले, तो मुझे वह वीर न मालूम होता, मेरा हृदय सुनकर उछलने न लगता। किंतु यदि किसी युवती को बचाने के लिए वह किसी कुत्ते की टाँग ही क्यों न तोड़ दे तो मुझे बड़ा बहादुर मालूम होता, मेरा हृदय प्रसन्नत्रा से उछलने लगता। पहिले उदाहरण में स्वार्थ था, क्रूरता थी, और थी नीरसता। उसके विपरीत दूसरे उदाहरण में एक तरफ थी भयत्रस्त हरिणी की तरह दो आँखें और हृदय से उठने वाली अमोघ प्रार्थना और दूसरी ओर थी रक्षा करने की स्फूर्ति, वीर प्रमाणित होने की पवित्र आकांक्षा, और विजय की लालसा। इन सबके ऊपर स्नेह का मधुर आवरण था जो इस चित्र को और भी सुंदर बना रहा था। कहानी-प्रेम ने मेरे हृदय को एक काल्पनिक कहानी की नायिका बनने की आतुरता में उड़ना सिखला दिया था।
जवानी आयी और उसी के साथ मेरी कहानी की आशा भी। यों तो शीशे में अपना मुँह रोज ही देखा जाता है, परंतु आँखें कभी-कभी केवल अपने को ही देखती रह जाती हैं। गहरे आँधेरे में बंद हृदय भी कदाचित् अपना स्वरूप दर्पण में देखने के लिए मचलने लगता है, आँखों से लड़ जाता है और उसकी सौंदर्य-समाधि को तोड़ देता है। मैंने सुना है कि एक समय ऐसा आता है, जब कुरूप-से-कुरूप व्यक्ति भी अपने को सुंदर समझने लगता है, फिर मैं तो सुंदरी थी ही।
बचपन में माँ मुझे प्यार से ‘मेरी सोना’, ‘मेरी हीरा’, ‘मेरी चाँद’ कहा करती थीं। बड़ी होने पर एक दिन कलूटे कुंदन ने मुझसे लड़ाई में कह दिया, कि ‘हम तुम्हारी सरीखा गोरा-गोरा मुँह कहाँ से लावें?’ बेचारा कुंदन क्या जाने कि उसने इन शब्दों से कौन-सा जादू फूँक दिया, कि फिर मैं उससे लड़ न सकी; इस बात के उत्तर में उसे पत्थर फेंककर मार न सकी। हाँ, मैंने अंदर जाकर दर्पण के सामने खड़ी होकर कुंदन के मुँह से अपने मुँह की तुलना अवश्य की थी। सचमुच मेरा मुँह बहुत गोरा था, परंतु कुंदन-कुंदन भी तो काला न था, साँवला था। और मुझे साँवले पुरुष ही अच्छे लगते थे। बचपन में अनेक बार राधा-कृष्ण की कहानी सुनते-सुनते मैं भी अपने को राधा-रानी समझने लगी थी और कृष्ण? कृष्ण, बहुत तलाश करने पर भी सिवा कुंदन के और कोई न मिलता। कुंदन बाँसुरी भी बजाता था। और साँवला भी था, फिर भला मेरा कृष्ण सिवा कुंदन के और हो ही कौन सकता था?
युवती होने पर मेरे विवाह की चर्चा स्वाभाविक थी। मैंने सुन रखा था कि विवाह कुछ चक्कर लगाकर होता है। और एक अपरिचित व्यक्ति उन्हीं कुछ चककरों के बाद लड़की को अपने साथ लिवा ले जाता है। किंतु मुझे तो विवाह के चक्करों से वे चक्कर अधिक रुचते थे, जो कभी-कभी मैं कुंदन के लिए और प्राय: कुंदन मेरे लिए लगाया करता था। मैं चाहती तो यही थी कि मुझे अब और किसी के साथ चक्कर न लगाने पड़ें। मैं तथा कुंदन-दोनों ने मिलकर जितने चक्कर लगाए हैं, हमारी जीवन-यात्रा के लिए उतने ही पर्याप्त हैं। किंतु पिताजी तो चिट्ठी-पत्री से कुछ और ही तय कर रहे थे। सुना, कि कोई इंग्लैंड से लौटे हुए इंजीनियर हैं, उनके साथ पिताजी मुझे जीवन भर के लिए बाँध देना चाहते हैं।
सोचा, मुझे कौन-सी इमारत खड़ी करवानी है या कौन-सा पुल तैयार करवाना है, जो पिताजी ने इंजीनियर तलाश किया। मेरे जीवन के थोड़े से दिन तो कुंदन के ही साथ हँसते-खेलते बीत जाते, किंतु वहाँ मेरी कौन सुनता था? परिणाम यह हुआ कि यहाँ इतने चक्कर लगाकर भी मेरे ऊपर कुंदन का कुछ अधिकार न हो पाया और इंजीनियर साहब ने, जिनसे न मेरी कभी की जान थी न पहिचान, मेरे साथ केवल सात चक्कर लगाए और मैं उनकी हो गयी।
इधर मेरा विवाह हो रहा था उधर कुंदन बी०ए० की परीक्षा दे रहा था। सुना कि कुंदन परीक्षा-भवन में बेहोश हो गया। आह! बेचारा एक ही साथ दो-दो परीक्षाओं में बैठा भी तो था!
विवाह की आड़ में, न जाने कितने मित्र और रिश्तेदारों की जमघट में, मेरी उत्सुक आँखें सदा कुंदन को खोजती रहती, किंतु इन तीन-चार दिनों में वह मुझे एक दिन भी न दिखा। विदा के दिन तो मेरे धैर्य का बाँध टूट गया। कुंदन की बहिन से मैंने पूछा; मालूम हुआ कि वह कई दिनों से बीमार है। अब क्या करती, हृदय में एक पीड़ा छिपाए हुए मैं विदा हुई। स्टेशन पर पहुँची, व्याकुलता असंभव को भी संभव बनाने की उधेड़बुन में रहती है। मैं जानती थी कि बीमार कुंदन स्टेशन नहीं आ सकता, फिर भी आँखें चारों तरफ किसी को खोज रही थीं। इधर ट्रेन ने चलने की सीटी दी, उधर गेट की तरफ से कोई तेजी से आता हुआ दिखा। आँखों ने कहा, कुंदन है; हृदय ने समर्थन दिया, किंतु मस्तिष्क ने विरोध किया, वह बीमार है, भला स्टेशन पर कैसे आएगा।
पर वह मेरा कुंदन ही था। उसकी आँखों में निराशाजनक उन्माद, चेहरे पर विषाद की गहरी छाया और होंठों पर वही स्वाभाविक मुस्कराहट थी। सिर के बिखरे हुए रूखे बालों ने पूरा माथा ढँक रखा था। मैं चिल्ला उठी, “कुंदन, इतनी देर बाद!” पास ही बैठी हुई नाइन ने मेरा मुँह बंद कर दिया, बोली, “चिल्लाओ मत बेटी, बराती सुनेंगे तो क्या कहेंगे!” अब मुझे होश आया कि मैं कहीं जा रही हूँ, अपने कुंदन से बहुत दूर, बहुत दूर।
कटे वृक्ष की तरह मैं बेंच पर गिर पड़ी। हृदय जैसे डूबने लगा। ट्रेन चल पड़ी। जब मनुष्य के प्रति मनुष्य की ही सहानुभूति कम देखने में आती है, तब भला इस जड़ पदार्थ रेलगाड़ी को मुझसे क्या सहानुभूति हो सकती थी! उसने मुझे कुंदन से दो बातें भी न करने दीं और झुक-झुककर हवा के साथ उड़ चली। मैं ससुराल आयी, बड़ी भारी कोठी थी। बहुत-सी दास-दासियाँ थीं। वहाँ का रंग ही दूसरा था। पतिदेव को अंग्रेजियत अधिक पसंद थी। उनका रहन-सहन, चाल-ढाल, बात-व्यवहार सभी साहबाना था। वे हिंदी बहुत कम बोला करते और अंग्रेजी मैं जरा कम समझती थी; इसलिए उनकी बहुत-सी बातों में प्रायः चुप रह जाया करती। उनके स्वभाव में कुछ रूख़ापन और कठोरता अधिक मात्रा में थी। नौकरों के साथ उनका जो बर्ताव होता, उसे देखकर मैं भय से सिहर उठती थी।
वे मुझे प्रायः रोज शाम को कभी सबेरे भी अपने साथ मोटर पर बैठाकर मीलों तक घुमा लाते, अपने साथ सिनेमा और थिएटर भी ले जाया करते; किंतु अपने इस साहब बहादुर के पार्श्व में बैठकर भी मैं कुंदन को न भूल सकती। सिनेमा की तस्वीरों में रेशमी कुर्ता और धोती पहिने हुए मुझे कुंदन की ही तस्वीर दिखाई पड़ती।
पति का प्रेम मैं पा सकी थी या नहीं यह मैं नहीं जानती, पर मैं उनसे डरती बहुत थी। भय का प्रेत रात-दिन मेरे सिर पर सवार रहता था। उनकी साधारण-सी भावभंगिमा भी मुझे कँपा देने के लिए पर्याप्त थी। वे मुझसे कभी नाराज न हुए थे, फिर भी उनके समीप मैं सदा यही अनुभव करती कि मैं बंदी हूँ और यहाँ जबरदस्ती पकड़कर लायी गयी हूँ।
इस ऐश्वर्य की चकाचौंध और विभूतियों के साम्राज्य में भी मैं अपने बाल-सखा कुंदन को न भूल सकी। मैके की स्वच्छंद वायु में कुंदन के साथ खेलना, लड़ना‑झगड़ना और उसकी बाँसुरी की ध्वनि मुझे भुलाए से भी न भूलती थी। क्षण भर का भी एकांत पाते ही बचपन की सुनहली स्मृतियाँ साकार होकर मेरी आँखों के सामने फिरने लगतीं; जी चाहता कि इस लोक-लज्जा की जंजीर को तोड़कर मैं मैके चली जाऊँ। किंतु इसी बीच छोटे भाई के पत्र से मुझे मालूम हुआ कि कुंदन घर छोड़कर न जाने कहाँ चला गया है, उसका कहीं पता नहीं है। इसलिए मेरी कुछ-कुछ यह धारणा हो गयी कि अब इस जीवन के कैदखाने से निकलकर भी कदाचित् मैं कुंदन को देख न सकूँगी। मैके जाने की भी अब मुझे उत्सुकता न थी, अब तो किसी प्रकार अपने दिन काटने थे।
न तो जीवन से ही कुछ आकर्षण था और न किसी के प्रति किसी तरह का अनुराग ही शेष रह गया था; पर काठ की पुतली की तरह सास और पति की आज्ञाओं का पालन करती हुई नियम से खाती-पीती थी, स्नान और श्रृंगार करती थी, और भी जो कुछ उनकी आज्ञा होती उसका पालन करती।
इसी समय एक ऐसी घटना हुई जिससे मेरी सोई हुई स्मृतियाँ फिर से जाग उठीं, मेरा उन्माद और बढ़ गया। एक दिन दोपहर के बाद मैं अपने छज्जे पर खड़ी हुई अन्यमनस्क भाव से बाहर सड़क से आने-जाने वालों को देख रही थी। सहसा सामने से कपड़ा बेचता हुआ, कुछ कपड़े स्वयं कंधे पर धरे हुए, कुछ नौकर के सिर पर रखवाए हुए, मुझे कुंदन दिखाई पड़ा। विश्वास न हुआ, परंतु आँखें खुली थीं; मैं सपना नहीं देख रही थी। दौड़कर नीचे आयी, आते ही खयाल आया, कि मेरे पैरों में तो मर्यादा की बेड़ियाँ पड़ी हैं, मैं कुंदन के पास दौड़कर कैसे जाऊँगी। उसके बाद मैंने देखा कि कुंदन स्वयं ही मेरे यहाँ के एक नौकर के साथ हमारे अहाते में आ रहा है। बाहरी बरामदे में उसने कपड़े उतार दिए। सोफे पर सास बैठी थीं। मैंने उनके बुलाने की प्रतीक्षा न की, चुपचाप आकर सोफे के पीछे खड़ी हो गयी।
मेरी सास सामान खरीदने की बड़ी शौकीन थीं। हमारे दरवाजे पर से कोई फेरीवाला ऐसा न निकलता था जिससे वह कुछ-न-कुछ खरीद न लेती हों। सास की इस आदत की आज मैंने मुक्त हृदय से प्रशंसा की। यदि उन्हें सामान खरीदने का इतना शौक न होता तो शायद मैं इस कपड़े वाले (कुंदन) को इतने समीप से न देख पाती। मुझे अपने पीछे देखकर वह हँसकर बोली, “बहू क्या लेना है, जो कुछ लेना हो अपने मन का पसंद कर लो।” बेचारी सास कया जानती थीं कि कपड़ों से अधिक मुझे कपड़े वाला पसंद है। फिर भी उनके आग्रह से मैंने दो शांतिपुरी साड़ियाँ ले लीं; उन्होंने भी अपने लिए कुछ साड़ियाँ खरीदीं। उसे दाम देकर और कई तरह की साड़ियाँ लाने के लिए कहकर सास ने उसे विदा किया।
कुंदन में बड़ा परिवर्तन था। अब वह बहुत दुबला और अधिक साँवला हो गया था। चेहरे पर वह लालिमा न थी, किंतु वही मनस्विता और ‘तेज’ टपक रहा था जो पहिले था। इस घटना को करीब एक महीना बीत गया। लगातार प्रतीक्षा करते रहने के बावजूद मैं कुंदन को न देख सकी।
जेठ का महीना था, बगीचे का एक माली छुट्टी पर गया था। बूढ़ा माली एक मेहनती आदमी की तलाश में था। चार बजे तक घर में बंद रहकर, गर्मी के कारण घबराकर, मैं अपनी सास के साथ बगीचे में चली गयी। वहीं बगीचे में मौलसिरी की घनी छाया में चबूतरे पर मैं सास के साथ बैठी थी। बार-बार यही सोचती थी कि कुंदन कहाँ चला गया? कपड़ा लेकर फिर क्यों नहीं आया? बीमार तो नहीं पड़ गया? और अगर बीमार हो गया होगा, तो उसकी देखभाल कौन करता होगा? मेरी आँखों में आँसू आ गए। इसी समय पीछे से आकर बूढ़े माली ने कहा, “सरकार यह एक आदमी है जो माली का काम कर सकता है, हुकुम हो तो रख लिया जाए।” मैंने मुड़कर देखा तो सहसा विश्वास न हुआ। कुंदन! और माली का काम! मेरी बेसुध वेदना तड़प उठी। एक सम्पन्न परिवार का होनहार युवक दस रुपए माहवार की मालीगीरी करने आए! इतनी कड़ी तपस्या!! हे ईश्वर! क्या इस तपस्या का अंत न होगा?
दस रुपए माहवार पर कुंदन बगीचे में माली का काम करने लगा। मैं देखती, कड़ी दोपहरी में भी वह दिन-दिन भर कुदाल चलाया करता, पानी सींचता और टोकरी भर-भर मिट्टी ढोता। उसका शरीर अब दिन-दिन दुबला और साँवला पड़ता जाता था। उसके स्वभाव में कितनी नवाबी थी, वह मेहनत के काम से कितना बचता था, मुझसे छिपा न था, किंतु अब वह कितना परिश्रम कर रहा है। मुझे चिंता रहती थी कि उसका सुकुमार शरीर इस कठिन परिश्रम को सह न सकेगा। मैं चाहती थी कि किसी प्रकार उसे रोक दूँ, यह काम वह छोड़ दे; परंतु कैसे रोकती, उससे बात करने की मुझे इजाजत ही कहाँ थी? पहिले की अपेक्षा अब मैं बगीचे में अधिक आने-जाने लगी। पहिले आने-जाने पर किसी ने ध्यान न दिया? किंतु कुछ ही दिनों बाद टीका-टिप्पणी होने लगी। बाद में रुकावट भी पड़ने लगी। जिसका परिणाम यह हुआ कि अब शाम-सुबह छोड़कर मैं प्रायः दोपहर को जाने लगी।
कुंदन से दो मिनट बात करने का मैं अवसर खोजा करती थी, किंतु मेरे पीछे भी लोग जासूस की तरह रहते थे। मैं एकांत कभी न पाती और सबके सामने उससे बात करने का साहस न होता। कभी-कभी मैं उसके नजदीक भी पहुँच जाती तो भी वह मेरी ओर आँख उठाकर न देखता, मैं ही उसे देख लिया करती। अनेक बार जी चाहा कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, जाऊँ, उसकी कुदाल छीनकर फेंक दूँ और उसे अपने साथ लिवा लाऊँ, अब उसकी तपस्या आवश्यकता से अधिक हो चुकी है। उसे अब मेरे निकट रहकर मेरे स्नेह की शीतल छाया में विश्राम करना चाहिए।
उस दिन बड़ी गरमी थी। बंद कमरे में पंखा और खस की टट्टियों के भीतर से मैं उस गरमी का अंदाजा न लगा सकती थी। नींद नहीं आ रही थी, न जाने क्यों एक प्रकार की बेचैनी से मैं अत्यंत अस्थिर-सी थी। उठी, खिड़की खोलकर बाहर निकली । पंखा खींचने वाली दासी ने रोका। “बहू इतनी गरमी में भीतर से बाहर न जाओ लू लग जाएगी।” मैंने उसे हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और बगीचे में पहुँची।
कुंदन की कुदाल रुक गयी। कुदाल को जमीन पर रख एक तरफ फेंककर उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा।
मैंने कहा, “कुंदन! तुम इतनी कड़ी तपस्या क्यों करते हो? तुम्हें इस प्रकार काम करते देखकर मुझे कष्ट नहीं होता? तुम्हारा शरीर इस मेहनत को सह सकेगा! तुम कहीं सुख से रहो तो मुझे भी शांति मिले। आखिर इस प्रकार जीवन को तपाने से क्या लाभ होगा? तुम तो मुझसे अधिक समझदार हो कुंदन!”
सारी करुणा सिमटकर कुंदन की आँखों में उतर आयी। वह कुछ बोला नहीं, बोलता भी कैसे? उसी समय खाँसता हुआ बूढ़ा माली अपनी कोठरी से बाहर आया और फिर उसे कुदाल उठा लेनी पड़ी।
मेरा स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। लोगों को संदेह था, शायद मुझे टी०बी० हो गयी है। पतिदेव मुझे भुवाली भेजने की तैयारी कर रहे थे; किंतु वे क्या जानते थे कि भुवाली से भी अधिक स्वास्थ्य-लाभ मैं कुंदन के समीप, केवल उसके सहवास से कर सकती हूँ। मेरी दवा तो कुंदन है। भुवाली और शिमला मुझे वह स्वास्थ्य नहीं प्रदान कर सकते, जो मुझे कुंदन से केवल स्वतंत्रतापूर्वक मिलने-जुलने से मिल सकता है। मैं उससे केवल स्वतंत्रता से बातचीत करना और मिलना-जुलना चाहती थी, और यह मेरे पतिदेव को स्वीकार न था।
नौकरों को वे मिट्टी के ठीकरों से भी गया-बीता समझते थे। दस रुपए माहवार देने के बाद समझते थे कि उन नौकरों की आत्मा और शरीर दोनों को उन्होंने खरीद लिया है। उनसे इतनी सख्ती से पेश आते कि नौकरों को उनके सामने पहुँचने में बड़े साहस से काम लेना पड़ता।
इधर कुंदन से एक दिन खुलकर बातचीत करने के लिए रात-दिन मेरे मस्तिष्क और हृदय में युद्ध छिड़ा रहता; अब न मुझसे पढ़ा-लिखा जाता और न किसी काम में ही जी लगता। खाने-पीने की तरफ भी कुछ विशेष रुचि न रह गयी थी। खाना देखते ही वे दिन याद आ जाते, जब मैं और कुंदन एक ही थाली में बैठकर खाया करते थे। चाय सामने आते ही कुंदन की याद आ जाती। मुझसे भी अधिक चाय का भक्त तो वही था। आज वह मेरे बगीचे में माली है, और मुझे इतनी भी स्वतंत्रता नहीं कि उससे एक-दो बात भी कर सकूँ। फिर उसके साथ बैठकर चाय पीने, और भोजन करने की बात तो बहुत दूर की रही।
मैं रात-दिन इसी चिंता में घुली जाती थी। किंतु मेरी पीड़ा को कौन पहिचानता? अपने इस घर में तो मुझे सभी हृदयहीन जान पड़ते थे। एक दिन ऑफिस से लौटते ही पतिदेव ने मुझसे प्रश्न किया, “आखिर उस माली से तुम्हें क्या बातें करनी रहती हैं जो दोपहर को भी बगीचे में जाया करती हो। कितनी बार तुमसे कहा कि नौकरों से बातचीत करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, पर तुम्हें मेरी बात याद रहे तब न! इस बात को भूल जाती हो कि तुम एक इंजीनियर की स्त्री हो। तुम्हें मेरी इज्जत का भी खयाल रखना चाहिए।”
मैं कुछ न बोली, बोलती भी क्या? मैंने चुप रहना ही उचित समझा। मुझे उससे क्या बातचीत करनी रहती है, मैं उन्हें क्या बतलाती? वह बतलाने की बात नहीं थी, समझने की बात थी, और उसे वही समझ सकता था जिसके पास हृदय हो। जिसके पास हृदय ही न हो, वह हृदय की बात क्या समझे?
मेरी इस चुप्पी का अर्थ उन्होंने चाहे जो लगाया हो, किंतु उनकी इस बाधा से मुझे बड़ी वेदना हुई। कुंदन से दो-चार मिनट बात करके न तो मैं ‘उनका’ कुछ बिगाड़ देती और न कुंदन को ही कुछ दे देती, फिर भी कुंदन से मिलने में उन्हें इतनी आपत्ति क्यों थी कौन जाने। चाहे जो हो, इस बाधा का परिणाम उलटा ही हुआ। ज्यों-ज्यों मुझे उसके समीप जाने से रोक गाया, त्यों-त्यों उसके पास पहुँचने के लिए मेरी उत्कंठा प्रबल होती गयी।
गर्मी की रात थी। बगीचे में बेलें इस प्रकार खिले थे जैसे आसमान में तारे फैले हों। मैं उन्हीं बेलों के पास संगमरमर की बेंच पर बैठी थी। कई दिन हो गए थे, कुंदन बगीचे में काम करता हुआ न दिखा था। वह कहाँ गया? काम करने क्यों नहीं आता? यद्यपि यह जानने के लिए मैं अत्यंत अस्थिर थी, फिर भी किसी से कुछ पूछने का मुझमें साहस न था।
अत्यंत उद्विग्नता से मैं बगीचे में इधर-उधर टहलने लगी। टहलते-टहलते मैं मालियों के क्वार्टर की तरफ निकल गयी। दूर से कुंदन की कोठरी कई बार देखी थी। आज उस कोठरी के बहुत समीप पहुँच गयी थी। कोठरी में प्रकाश तो न था, किंतु अंदर से कराहने की आवाज साफ‑साफ सुनाई पड़ती थी। मैंने ध्यान से सुना, आवाज कुंदन की थी। अब मैं बिलकुल भूल गयी कि मैं किसी इंजीनियर की स्त्री हूँ और कुंदन मेरा माली। तेजी से कदम बढ़ाकर मैं कोठरी में पहुँच गयी। बिजली का बटन दबाते ही कोठरी में प्रकाश फैल गया, कुंदन ने घबराकर आँखें खोल दीं, मुझे देखते ही इस बीमारी में भी उसकी आँखें चमक उठीं, और वह वही चमक थी, जिसे उसकी आँखों में मैंने एक बार नहीं, अनेक बार देखा थी। मैं उसी की चारपाई पर उसके सिरहाने बैठ गयी।
तेज बुखार से उसका शरीर जल रहा था। मालूम हुआ कि उसे कई दिनों से बुखार आ रहा है, काम वह फिर भी बराबर करता है। इधर कई दिनों से वह बहुत अशक्त हो गया है और दो दिनों से छाती और पसलियों में अधिक दर्द होने के कारण वह कोठरी से बाहर नहीं निकल सका। उसकी अवस्था चिंताजनक थी। कुछ देर तक खाँसकर वह फिर बोला, “हीना रानी, तुम आयी तो हो, कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो नहीं? पर अब तो आयी ही हो, अपने हाथ से एक गिलास पानी पिला दो, बड़ी देर से प्यासा हूँ।”
मैंने मटकी से एक गिलास भर पानी उसे पिलाया और फिर बैठ गयी। मैं उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। रोकने पर भी मेरी आँखों से झड़ी रुकी नहीं, चलती रही। और गला रुँधा जा रहा था। प्रयत्न करने पर भी मैं कुंदन से एक शब्द न कह सकी। कुंदन ने अपने गरम-गरम हाथों को नीचे झुकाकर, मेरे पैरों को छू लिया और क्षीण स्वर में बोला, “हीना रानी, घर जाओ। तुम्हें कोई यहाँ देख लेगा तो नाहक तुम पर कोई विपत्ति न आ जाए? कहीं मेरा यह सुख भी न छिन जाए? तुम्हारे समीप इस हालत में भी रहकर मैं एक प्रकार का सुख पाता हूँ।”
ठीक उसी समय पतिदेव ने कोठरी में प्रवेश किया। उन्होंने आग्नेय नेत्रों से मेरी तरफ देखा, फिर कुछ बोले, क्या बोले मैं कुछ समझी नहीं। मैं उसी प्रकार कुंदन के सिर पर हाथ धरे बैठी रही। मेरी आत्मा ने कहा, ‘मैंने कोई अपराध नहीं किया है। किसी बीमार की सेवा-सुश्रूषा करना मनुष्य मात्र का धर्म है। फिर मृत्यु की घड़ियों को गिनते हुए, उसकी नजरों में अपने एक आश्रित और अपनी आँखों में अपने एक बाल सखा को यदि मैंने एक घूँट पानी पिला दिया, तो क्या यह कोई अपराध कर डाला?’
किंतु मैं उसी क्षण कोठरी छोड़ देने के लिए बाध्य कर दी गयी। मैं ऊपर आयी तो अवश्य, किंतु मेरी अवस्था पागलों की तरह हो गयी थी; रह-रहकर कुंदन की रुग्ण मुखाकृति मेरी आँखों के सामने फिरने लगी। बार-बार ऐसा मालूम होता कि कुंदन एक घूँट पानी के लिए चिल्ला रहा है। पतिदेव सोए थे, मैं भी एक तरफ पड़ी थी। पर मेरी आँखों में नींद कहाँ? उठी और छज्जे पर बेचैनी से टहलने लगी। बंगले के पास ही बिजली के खंभे के नीचे मैंने कुछ सफेद-सफेद-सा देखा। अज्ञात आशंका से मैं सिहर उठी। ध्यान से देखा वह कुंदन था। कदाचित् जीवन की अंतिम साँसें गिन रहा था। उस समय न तो कुल की मान-प्रतिष्ठा का ध्यान रहा, न किसी के भय का; और न यहीं ध्यान रहा कि इतनी रात को लोग मुझे बाहर देखकर क्या कहेंगे।
चौकीदार मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करता? फाटक ख़ुलवाकर मैं बाहर निकल गयी। पास पहुँचकर देखा, कुंदन ही था। आह! वही अपने माता-पिता का दुलारा कुंदन, अपने मित्रों का प्यारा कुंदन, जिसका कुम्हलाया हुआ मुख देखकर कितने ही हृदय सहानुभूति से द्रवीभूत हो उठते थे, जिसके इंगित मात्र पर परिचालक वर्ग सेवा के लिए प्रस्तुत रहता था, आज वही कुंदन जीवन के अंतिम समय में अकेला और असहाय, शून्य दृष्टि से आसमान की ओर देख रहा था। मुझे देखते ही जैसे उसमें कुछ शक्ति आ गयी हो। वह क्षीण स्वर में बोल उठा, “हीना रानी, अच्छा हुआ जो तुम आ गयीं। थोड़ा पानी पिला दो। मैं बहुत प्यासा हूँ।” मैंने पानी के लिए चारों तरफ नजर दौड़ाई। थोड़ी दूर पर नल तो था, पर बरतन कोई न था। जिससे मैं उसे पानी पिलाती। सोचा घर तक जाऊँ, पर घर जाने का समय न था। नल पर से साड़ी का छोर भिगोकर लौटी, परंतु अब वह पानी माँगने वाला इस संसार में था ही कहाँ?
बस मेरी या उसकी कहानी यही है।
समाप्त