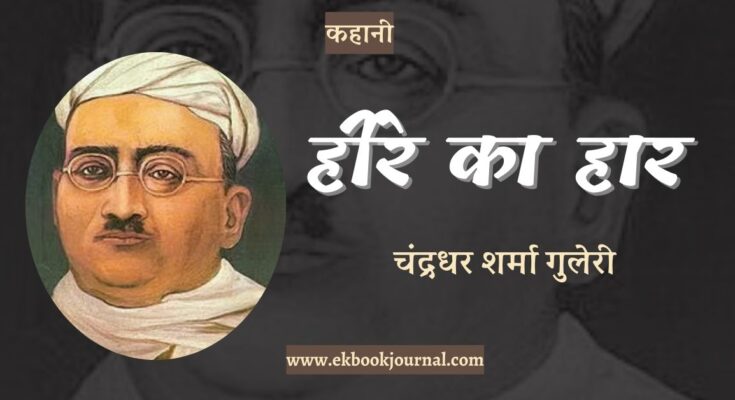1
आज सवेरे ही से गुलाबदेई काम में लगी हुई है। उसने अपने मिट्टी के घर के आँगन को गोबर से लीपा है, उस पर पीसे हुए चावल से मंडन माँडे हैं। घर की देहली पर उसी चावल के आटे से लीकें खैंची हैं और उन पर अक्षत और बिल्वपत्र रक्खे हैं। दूब की नौ डालियाँ चुन कर उनने लाल डोरा बाँध कर उसकी कुलदेवी बनायी है और हर एक पत्ते के दूने में चावल भर कर उसे अंदर के घर में, भींत के सहारे एक लकड़ी के देहरे में रक्खा है। कल पड़ोसी से माँग कर गुलाबी रंग लायी थी उससे रंगी हुई चादर बिचारी को आज नसीब हुई है। लठिया टेकती हुई बुढ़िया माता की आँखें यदि तीन वर्ष की कंगाली और पुत्र वियोग से और डेढ़ वर्ष की बीमारी की दुखिया के कुछ आँखें और उनमें ज्योति बाकी रही हो तो— दरवाज़े पर लगी हुई हैं। तीन वर्ष के पतिवियोग और दारिद्र्य की प्रबल छाया से रात-दिन के रोने से पथराई और सफेद हुई गुलाबदेई की आँखों पर आज फिर यौवन की ज्योति और हर्ष के लाल डोरे आ गये हैं। और सात वर्ष का बालक हीरा, जिसका एकमात्र वस्त्र कुरता खार से धो कर कल ही उजाला कर दिया गया है, कल ही से पड़ोसियों से कहता फिर रहा है कि मेरा चाचा आवेगा।
बाहर खेतों के पास लकड़ी की धमाधम सुनाई पड़ने लगी। जान पड़ता है कि कोई लँगड़ा आदमी चला आ रहा है जिसके एक लकड़ी की टाँग है। दस महीने पहिले एक चिट्ठी आयी थी जिसे पास के गाँव के पटवारी ने पढ़ कर गुलाबदेई और उसकी सास को सुनाया था। उसें लिखा था कि लहनासिंह की टाँग चीन की लड़ाई में घायल हो गयी है और हाँगकांग के अस्पताल में उसकी टाँग काट दी गयी है। माता के वात्सल्यमय और पत्नी के प्रेममय हृदय पर इसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि बेचारियों ने चार दिन रोटी नहीं खायी थी। तो भी — अपने ऊपर सत्य आपत्ति आती हुई और आयी हुई जान कर भी हम लोग कैसे आँखें मीच लेते हैं और आशा की कच्ची जाली में अपने को छिपा कर कवच से ढका हुआ समझते हैं! — वे कभी-कभी आशा किया करती थीं कि दोनों पैर सही सलामत ले कर लहनासिंह घर आ जाय तो कैसा! और माता अपनी बीमारी से उठते ही पीपल के नीचे के नाग के यहाँ पंचपकवान चढ़ाने गयी थी कि “नाग बाबा! मेरा बेटा दोनों पैरों चलता हुआ राजी-खुशी मेरे पास आवे।” उसी दिन लौटते हुए उसे एक सफेद नाग भी दीखा था जिससे उसे आशा हुई थी कि मेरी प्रार्थना सुन ली गयी। पहले पहले तो सुखदेई को ज्वर की बेचैनी में पति की टाँग — कभी दहनी और कभी बाईं — किसी दिन कमर के पास से और किसी दिन पिंडली के पास से और फिर कभी टखने के पास से कटी हुई दिखाई देती परंतु फिर जब उसे साधारण स्वप्न आने लगे तो वह अपने पति को दोनों जाँघों पर खड़ा देखने लगी। उसे यह न जान पड़ा कि मेरे स्वस्थ मस्तिष्क की स्वस्थ स्मृति को अपने पति का वही रूप याद है जो सदा देखा है, परंतु वह समझी की किसी करामात से दोनों पैर चंगे हो गये हैं।
2
किंतु अब उनकी अविचारित रमणीय कल्पनाओं के बादलों को मिटा देने वाला वह भयंकर सत्य लकड़ी का शब्द आने लगा जिसने उनके हृदय को दहला दिया। लकड़ी की टाँग की प्रत्येक खटखट मानो उनकी छाती पर हो रही थी और ज्यों-ज्यों वह आहट पास आती जा रही थी त्यों-त्यों उसी प्रेमपात्र के मिलने के लिए उन्हें अनिच्छा और डर मालूम होते जाते थे कि जिसकी प्रतीक्षा में उसने तीन वर्ष कौए उड़ाते और पल-पल गिनते काटे थे प्रत्युत वे अपने हृदय के किसी अंदरी कोने में यह भी इच्छा करने लगीं कि जितने पल विलम्ब से उससे मिलें उतना ही अच्छा, और मन की भित्ति पर वे दो जाँघों वाले लहनासिंह की आदर्श मूर्ति को चित्रित करने लगी और उस अब फिर कभी न दिख सकने वाले दुर्लभ चित्र में इतनी लीन हो गयी कि एक टाँग वाला सच्चा जीता जागता लहनासिंह आँगन में आ कर खड़ा हो गया और उसके इस हँसते हुए वाक्यों से उनकी वह व्यामोहनिद्रा खुली कि “अम्मा! क्या अम्बाले की छावनी से मैंने जो चिट्ठी लिखवाई थी वह नहीं पहुँची?”
माता ने झटपट दिया जगाया और सुखदेई मुँह पर घूँघट ले कर कलश ले कर अंदर के घर की दहनी द्वारसाख पर खड़ी हो गयी। लहनासिंह ने भीतर जा कर देहरे के सामने सिर नवाया और अपनी पीठ पर की गठरी एक कोने में रख दी। उसने माता के पैर हाथों से छू कर हाथ सिर को लगाया और माता ने उसके सिर को अपनी छाती के पास ले कर उस मुख को आँसुओं की वर्षा से धो दिया जिस पर बाक्तरों की गोलियों की वर्षा के चिह्र कम से कम तीन जगह स्पष्ट दिख रहे थे।
अब माता उसको देख सकी। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उसके बीच-बीच में तीन घावों के खड्डे थे। बालकपन में जहाँ सूर्य, चंद्र, मंगल आदि ग्रहों की कुदृष्टि को बचानेवाला ताम्बे चाँदी की पतड़ियों और मूँगे आदि का कठला था वहाँ अब लाल फीते से चार चाँदी के गोल-गोल तमगे लटक रहे थे। और जिन टाँगों ने बालकपन में माता की रजाई को पचास-पचास दफा उघाड़ दिया उनमें से एक की जगह चमढ़े के तसमों से बँधा हुआ डंडा था। धूप से स्याह पड़े हुए और मेहनत से कुम्हलाए हुए मुख पर और महीनों तक खटिया सेने की थकावट से पिलाई हुई आँखों पर भी एक प्रकार की, एक तरह के स्वावलम्बन की ज्योति थी जो अपने पिता, पितामह के घर और उनके पितामहों के गाँव को फिर देख कर खिलने लगती थी।
माता रुँधे हुए गले से न कुछ कह सकी और न कुछ पूछ सकी। चुपचाप उठ कर कुछ सोच-समझ कर बाहर चली गयी। गुलाबदेई जिसके सारे अंग में बिजली की धाराएँ दौड़ रही थीं और जिसके नेत्र पलकों को धकेल देते थे इस बात की प्रतीक्षा न कर सकी कि पति की खुली हुई बाँहें उसे समेट कर प्राणनाथ के हृदय से लगा लें किंतु उसके पहले ही उसका सिर जो विषाद के अंत और नवसुख के आरम्भ से चकरा गया था पति की छाती पर गिर गया और हिंदुस्तान की स्त्रियों के एकमात्र हाव-भाव — अश्रु — के द्वारा उनकी तीन वर्ष की कैद हुई मनोवेदना बहने लगी।
वह रोती गयी और रोती गयी। क्या यह आश्चर्य की बात है? जहाँ की स्त्रियाँ पत्र लिखना-पढ़ना नहीं जानतीं और शुद्ध भाषा में अपने भाव नहीं प्रकाश कर सकतीं और जहाँ उन्हें पति से बात करने का समय भी चोरी से ही मिलता है वहाँ नित्य अविनाशी प्रेम का प्रवाह क्यों नहीं अश्रुओं की धारा की भाषा में… ( गुलेरी जी इस कहानी को यहीं तक लिख पाए थे। आगे की कहानी कथाकार डॉ। सुशील कुमार फुल्ल ने पूरी की है) …उमड़ेगा। प्रेम का अमर नाम आनंद है। इसकी बेल जन्म‑जन्मांतर तक चलती है। गुलाबदेई को तीन वर्ष के बाद पति-स्पर्श का मिला था। पहले तो वह लाजवंती-सी छुईमुई हुई, फिर वह फूली हुई बनिए की लड़की-सी पति में ही धसती चली गयी। पहाड़ी नदी के बाँध टूटना ही चाहते थे कि लहनासिंह लड़खड़ा गया और गिरते-गिरते बचा। सकुचायी-सी, शर्मायी-सी गुलाबदेई ने लहनासिंह को चिकुटी काटते हुए कहा, “बस..।” और आँखों ही आँखों में बिहारी की नायिका के समान भरे मान में मानो कहा, ‘कबाड़ी के सामने भी कोई लहँगा पसारेगी?’
“हारे को हरिनाम, गुलाबदेई। मेरी प्राणप्यारी। मैं हारा नहीं हूँ। सुनो..। मर्द और कर्द कभी खुन्ने नहीं होते गुलाबो..। और चीन की लड़ाई ने तो मेरी धार और तेज़ कर दी है।” लहनासिंह तन कर खड़ा हो गया था! गुलाबदेई सरसों-सी खिल आयी। मानो लहनासिंह उसे कल ही ब्याह कर लाया हो।
माँ रसोई करने चली गयी थी। तीन साल बाद बेटा आया था। उसके कानों में बैसाखियों की खड़खड़ाहट अब भी सुनाई दे रही थी। भगवती से कितनी मन्नतें मानी थीं। वह शिवजी के मंदिर में भी हो आयी थी! आखिर देवी-देवता चाहें तो वह सही सलामत भी आ सकता था परंतु अब तो वह साक्षात सामने था। फिर भी माँ को किसी चमत्कार की आशा थी, वह सीडूं बाबा से पुच्छ लेने जाएगी। फिर देगची में कड़छी हिलाते हुए सोचने लगी..। देश के लिए एक टाँग गँवा दी तो क्या हुआ। उसकी छाती फूल गयी। बेटे ने माँ के दूध की लाज रखी थी।
“चाचा, तुम आ गये!”
“हाँ बेटा।” लहनासिंह ने उसे अंक में भरते हुए कहा।
“चाचा..। इतने दिन कहाँ थे?”
“बेटा मैं लाम पर था। चीन से युद्ध हो रहा था न…”
“चीन कहाँ है?” मासूमियत से बालक ने पूछा!
“हिमालय के उस पार।”
“मुझे भी ले चलोगे न?”
“अब मैं नहीं जाऊँगा। फौज से मेरी छुट्टी हो गयी!” कुछ सोच कर उसने फिर कहा, “बेटा, तुम बड़े हो जाओगे तो फौज में भर्ती हो जाना।”
“मैं भी चीनियों को मार गिराऊँगा! लेकिन चाचा क्या मेरी भी टाँग कट जाएगी?”
“धत तेरी! ऐसा नहीं बोलते। टाँग कटे दुश्मनों की।” फिर हीरे ने जेब में आम की गुठली से बनाई पीपनी निकाली और बजाने लगा। बरसात में आम की गुठलियाँ उग आती हैं, तो बच्चे उस पौधों को उखाड़ कर गुइली में से गिट्टक निकाल कर बजाने लगते हैं। बड़े-बूढ़े खौफ दिखाते है कि गुठलियों में साँप के बच्चे होते हैं परंतु इन बंदरों को कौन समझाए..। आदमी के पूर्वज जो ठहरे।
“तुम मदरसे जाते हो?”
“हूँ..। लेकिन मौलवी की लम्बी दाढ़ी से डर लगता है…”
“क्यों?”
“दाढ़ी में उसका मुँह ही दिखाई नहीं देता…”
“तुम्हें मुँह से क्या लेना है। अच्छे बच्चे गुरुओं के बारे में ऐसी बात नहीं करते।”
“मेरा नाम तो अभी कच्चा है…”
“नाम कच्चा है या कच्ची में ही…”
“मैं पक्की में हो जाऊँगा लेकिन बड़ी माँ ने अधन्नी नही दी..। फीस लगती है चाचा।” और वह पीपनी बजाता हुआ गयब हो गया।
लहनासिंह सोचने लगा…। उमर कैसे ढल जाती है…। पहाड़ी नदी-नाले मैदान तक पहुँचते-पहुँचते संयत हो जाते हैं…। ढलती हुई उमर में वर्तमान के खिसकने और भविष्य के अनिश्चय घेर लेते हैं। चीन की लड़ाई में जख्मी होने पर जब अस्पताल में था…। तो हर नर्स उसे आठ-नौ साल की सूबेदारनी दिखाई देती…। सिस्टर नैंसी से एक दिन उसने पूछा भी था, “सिस्टर क्या कभी तुम आठ साल की थीं?”
“अरे बिना आठ की उमर पार किए मैं बाईस की कैसे हो सकती हूँ…। तुम्हें कोई याद आ रहा है…”
“हाँ…। वह आठ साल की छोकरी…। दही में नहाई हुई…। बहार के फूलों-सी मुस्कराती हुई मेरी ज़िंदगी में आयी थी…। और फिर एकएक विलुप्त हो गयी…। सूबेदारनी बन गयी…।” कहते-कहते वह खो गया था!
“हवलदार..। तुम परी-कथाओं में विश्वास रखते हो?”
“परियों के पंख होते हैं न…। वे उड़ कर जहाँ चाहें चली जाएँ…। कल्पना ही तो जीवन है।”
“परंतु तुम्हें तो शौर्य-मेडल मिला है।”
“अगर मेरी कल्पना में वह आठ वर्षीय कन्या न होती तो मुझे कभी शौर्य-मेडल न मिलता…। मेरी प्रेरणा वही थी…”
“तुमने विवाह नहीं बनाया।” नैंसी ने पूछा।
“विवाह तो बनाया…। कनेर के फूल-सी लहलहाती मेरी पत्नी है…। एक बेटा है…। और मेरी बूढ़ी माँ है…”
“तो फिर परियों की कल्पना…। आठ वर्ष की कन्या का ध्यान…”
“हाँ, सिस्टर…। मैंने 35 साल पहले उस कन्या को देखा था…। फिर वह ऐसे गायब हुई जैसे कुरली बरसात के बाद कही अदृश्य हो जाती है…। और मैं निपट…। अकेला…।” नैंसी चली गयी थी। वह सोचता रहा था, ‘स्वप्न में सफेद कौओं का दिखाई देना शुभ लक्षण है या अशुभ का प्रतीक..।’ अस्पताल में अर्ध-निमीलित आँखों में अनेक देवता आते…। कभी उसे लगता कि फनियर नाग ने उसे कमर से कस लिया है… शायद यह नपुंसकता का संकेत न हो…। वह दहल जाता…। माँ…। पत्नी…। और हीरा…। कैसे होंगे…। गाँव में वैसे तो ऐसा कुछ नहीं जो भय पैदा करे…। लेकिन तीन साल तो बहुत होते हैं…। वे कैसे रहती होंगी…। युद्ध में तो तनख्वाह भी नहीं पहुँचती होगी…। फिर उसे ध्यान आया कि जब वह चलने लगा था तो माँ ने कहा था, “बेटा…। हमारी चिंता नहीं करना। आँगन में पहाड़िए का बास हमारी रक्षा करेगा…।” फिर उसे ध्यान आया…। कई बार पहाड़िया नाराज़ हो जाए तो घर को उलटा-पुलटा कर देता है। आप चावल की बोरी को रखें…। वह अचानक खुल जाएगी और चावलों का ढेर लग जाएगा। कभी पहाड़िया पशुओं को खोल देगा…। अरे नहीं…। पहाड़िया तो देवता होता है, जो घर-परिवार की रक्षा करता है। वह आश्वस्त हो गया था।
“मुन्नुआ, तू कुथी चला गिया था?”
“माँ फौजी तो हुक्म का गुलाम ओता है।”
“फिरकू तां जर्मन की लड़ाई से वापस आ गया था…। उसका तो कोई अंग-भंग वी नईं हुआ था…और तू पता नहीं कहाँ-कहाँ भटकता रहा…। तिझो घरे दी वी याद नी आयी।”
“अम्मा..। फिरकू तो फिरकी की भाँति घूम गया होगा लेकिन मैं तो वीर माँ का सपूत हूँ…। उस पहाड़ी माँ का जो स्वयं बेटे को युद्धभूमि में तिलक लगा कर भेजती है…। बहाना बना कर लौटना राजपूत को शोभा नही देता…”
“हाँ, सो तो तमगे से देख रेई हूँ लेकिन…”
“लेकिन क्या अम्मा…। तुम चुप क्यों हो गयी।”
“गुलाबदेई तो वीरांगना है..। उसे तो गर्व होना चाहिए…”
“हाँ…बेटा…फौजी की औरत तो तमगों के सहारे ही जीती है लेकिन…”
“लेकिन क्या अम्मा…। कुछ तो बोलो!”
“उसका हाल तो बेहाल रहा…। आदमी के बिना औरत अधूरी है…। और फौजी की औरत पर तो कितणी उँगलियाँ उठती हैं…। तुम क्या जानो।” तुम तो नौल के नौलाई रेअ।
“हूँ।”
“क्या तमगे तुम्हारी दूसरी टाँग वापस ला सकते हैं? और तीन साल से सरकार ने सुध-बुध ही कहाँ ली…”
लहनासिंह के पास कोई जवाब नहीं था। सूबेदारनी ने किस अनुनय-विनय से उसे बींध लिया था…। हजारासिंह बोधा सिंह की रक्षा करके उसने कौन-सा मोर्चा मार लिया था…। वह युद्ध-भूमि में तड़प रहा था और रैड-क्रास वैन बाप-बेटे को ले कर चली गयी थी…। उसने जो कहा था मैंने कर दिया…। सोच कर फूल उठा लेकिन गुलाबदेई के यौवन का अंधड़ कैसे निकला होगा…। लोग कहते होंगे…। बरसाती नाले-सा अंधड़ आया और वह झरबेरी-सी बिछ गयी थी…। तूफान में दबी…।सहमी सी लँगड़े खरगोश-सी…। नहीं…। लँगड़ी वह कहाँ है…। लँगड़ा तो लहनासिंह आया है…। चीन में नैंसी से बतियाता…। खिलखिलाता…
अम्मा फिर रसोई में चली गयी थी! गुलाबदेई उसकी लकड़ी की टाँग को सहला रही थी…। शायद उसमें स्पंदन पैदा हो जाए…। शायद वह फिर दहाड़ने लगे…। तभी लहनासिंह ने कहा था, “गुलाबो…। यह नहीं दूसरी टाँग…”
वह दोनों टाँगों को दबाने लगी थी…। और अश्रुधारा उसके मुख को धो रही थी…। वह फिर बोला, “गुलाबो…। तुम्हें मेरे अपंग होने का दुख है?”
“नहीं तो!”
“फिर रो क्यों रही हो…”
“फौजी की बीबी रोए तो भी लोग हँसते हैं और अगर हँसे तो भी व्यंग्य-वाण छोड़ते हैं…। वह तो जैसे लावरिस औरत हो…। वह फूट पड़ी थी।”
“मैं तो सदा तुम्हारे पास था!”
“अच्छा!” अब ज़रा वह खिलखिलायी।
“हीरे का हीरा पा कर भी तुम बेबस रहीं।”
“और तुम्हारे पास क्या था?”
“तुम!”
“नहीं..। कोई मीम तुम्हें सुलाती होगी..। और तुम मोम-से पिघल जाते होओगे..। मर्द होते ही ऐसे हैं।”
“जरा खुल कर कहो न…”
“गोरी-चिट्टी मीम देखी नहीं कि लट्टू हो गये…”
“तुम्हें शंका है?”
“हूँ…। तभी तो इतने साल सुध नहीं ली…”
“मैं तो तुम्हारे पास था हमेशा…। हमेशा…”
“और वह सूबेदारनी कौन थी?”
“क्या मतलब?”
“तुम अब भी माँ से कह रहे थे…। उसने कहा था…। जो कहा था…। मैंने पूरा कर दिया…”
“हाँ…। मैं जो कर सकता था…। वह कर दिया…”
“किन युद्ध में सूबेदारनी कहाँ से आ गयी?”
“वह कल्पना थी।”
“तो क्या गुलाबो मर गयी थी..। मैं कल्पना में भी याद नहीं आयी।”
“मैं तुम्हें उसे मिलाने ले चलूँगा।”
“हूँ…। मिलोगे खुद और बहाना मेरा..। फौजिया तुद घरे नी औणा था।”
“मैं अब चला जाता हूँ…”
“मेरे लिए तो तुम कब के जा चुके थे…। और आ कर भी कहाँ आ पाए…”
“गुलाबो…। तुम भूल कर रही हो…। मैंने कहा था न…। मर्द और कर्द कभी खुन्ने नहीं होते…। उन्हें चलाना आना चाहिए…”
“अच्छा…। अच्छा…। छोड़ो भी न अब…। हीरा आ जाएगा…”
और दोनों ओबरी में चले गये। सदियों बाद जो मिले थे। छोटे छोटे सुख मनोमालिन्य को धो डालते हैं और एक-दूसरे के प्रति आश्वस्ति जीवन का आधार बनाती है— एक मृगतृष्णा का पालन दाम्पत्य-जीवन को हरा-भरा बना देता है…। गुलाबदेई लहलहाने लगी थी…। और आँगन में अचानक धूप खिल आयी थी।
समाप्त