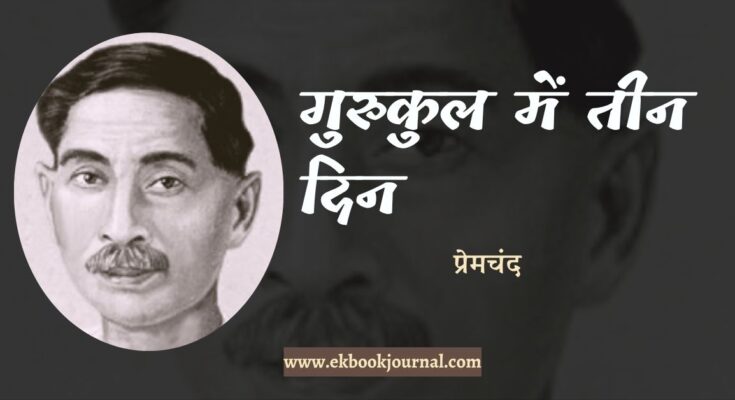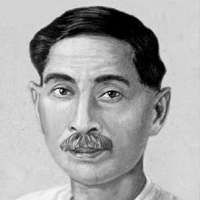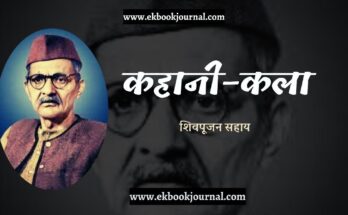1
पिछले आषाढ़ में मुझे गुरुकुल कांगड़ी के दर्शनों का अवसर मिला। इच्छा तो बहुत दिनों से थी, मगर यह सोचकर कि उस वेद वेदांगों के केंद्र में मुझ जैसे धर्मशून्य व्यक्ति का कहाँ गुज़र, कभी जाने को हिम्मत न पड़ी। सौभाग्य से साहित्य-परिषद् ने उन्हीं दिनों अपना वार्षिक उत्सव करने की ठानी और मुझे न्योता मिला। ऐसा अवसर पाकर भला कैसे चूकता। दिली मुराद पूरी हुई। रात को लखनऊ से चलकर प्रातःकाल हरिद्वार जा पहुँचा। वहाँ दो ब्रह्मचारी मेरी राह देख रहे थे। गुरुकुल की सिद्धांतवादिता का कुछ थोड़ा-सा परिचय मुझे स्टेशन पर ही मिला। एक तांगा करने की ठहरी। तांगे वाले ने शायद यह समझकर कि दो नये यात्री हैं, कनखल के आठ आने माँगे। इधर से छह आने कहा गया। तांगे वाले ने शायद कहा, आठ आने से कम न होंगे। ब्रह्मचारियों ने वाजिब किराया कह दिया था। तांगे वाले से ठाँय‑ठाँय करना उनकी शान के खिलाफ था। आध मील जाकर दूसरा तांगा उन्हीं दामों पर लाये। पहला तांगे वाला उन्हीं दामों पर चलने को तैयार था, अपना अपराध क्षमा कराता था, अपनी भूल स्वीकार करता था, पर ब्रह्मचारियों को उस पर दया न आयी। उसने यात्रियों को ठगना चाहा था, इसका दंड उसे देना ज़रूरी था। और नीति की दृष्टि में दया का कोई मूल्य नहीं।
तांगा आध घंटे में कनखल आ पहुँचा। हम लोग उतरकर घाट पर पहुँचे। सामने की पहाड़ियाँ हरे-भरे आभूषण पहने खड़ी थीं। नीचे गंगा पहाड़ियों की गोद से निकलकर उछलती-कूदती चली जाती थी। यहाँ कई धाराएँ हैं, जो वर्षाकाल में मिलकर कांगड़ी के नीचे तक चली जाती हैं। मैंने समझा था किसी किश्ती पर नदी पार करनी पड़ेगी, मगर किश्ती का कहीं पता न था। यहाँ पानी का तोड़ इतना तेज़ है, नीचे का पेटा इतना पथरीला कि थोड़ी दूर के बाद किश्ती आगे जा ही नहीं सकती। तमेड़ों पर बैठकर लोग आते-जाते हैं। यह एक प्रकार की घन्नई है, जिसमें मिट्टी के मटकों की जगह टीन के कनस्तर होते हैं। कई कनस्तरों को लम्बे-लम्बे रखकर रस्सी और बाँसों से बाँध देते हैं। तमेड़ा बीच में चौड़ा और दोनों सिरों पर पतला होता है। जिन्हें इस पर पहली बार बैठना पड़े उन्हें मन में कुछ संशय होने लगता है कि यह डोंगा पार लगेगा या बीच ही में डूबेगा। मगर थोड़ी ही दूर चलकर यह संशय दूर हो जाता है। यह डोंगी डूब नहीं सकती। पानी का बहाव कितना ही तेज हो, भँवर कितना ही भयंकर हों, वायु कितनी ही प्रचंड हो, लहरें उछलकर उसके ऊपर ही क्यों न आ जाती हों, पर उसे परास्त नहीं कर सकतीं। आदमी अगर उस पर ज़रा सँभलकर बैठा रहे, तो चाहे अनंत तक पहुँच जाएँ, डूब नहीं सकता। इस तुच्छ-सी वस्तु को विराट और प्रचंड जल-प्रवाह का इतनी वीरता से सामना करते देखकर ऐसा जान पड़ता था मानों कोई अकेली आत्मा प्राण-सागर की लहरों को ठुकराती, विघ्न बाधाओं को कुचलती परम धाम की ओर चली जा रही हो।
अभी आध घंटा भी न गुजरने पाया था कि घटा छा गयी और वर्षा होने लगी। सारे कपड़े भीग गये, हवा भी चलने लगी। लहरें उछलती ही न थीं, छलाँगें भरती थीं। कई बार तमेड़ा नीचे की चट्टान से टकराया और हम गिरते-गिरते बचे। दस बजते-बजते हम कांगड़ी पहुँच गये।
2
गुरुकुल की इमारतें देखकर बेअख्तियार मुँह से निकल गया – नाम बड़े दर्शन थोड़े। एक ही इमारत है जिसे इमारत कह सकते हैं, पर साधारण हाई स्कूलों की इमारत भी इससे अच्छी होती है। तीन साल पहले यहाँ कई और इमारतें थीं। पर सन् 1924 की बाढ़ में कई इमारतें बह गयीं और हरा-भरा बाग बालू से भर गया। गिरे हुए भवनों के खंडहर अभी तक नज़र आते हैं। हम लोग एक छोटे-से पक्के घर में ठहरे, जिसे यहाँ पक्का धर्मशाला कहते हैं। श्रद्धेय पंडित पद्मसिंह जी शर्मा भी आ गये थे। हम दोनों इसी कमरे में ठहरे। स्नान किया। इतने में भोजन आ गया। खाने बैठ गये। पेड़े बहुत स्वादिष्ट थे। अतिथि-सत्कार यहाँ की विशेषता है। भस्मक रोगी भी यहाँ से तृप्त हुए बिना नहीं जा सकता। सबसे बड़ा आनंद मुझे यहाँ के ब्रह्मचारियों को देखकर हुआ। ऐसे सरल-हृदय, सेवाशील युवक हमारे अंग्रेजी कॉलेजों में बहुत कम हैं। वह पंडिताई वातावरण, जो काशी की किसी संस्कृत पाठशाला में नज़र आता है, यहाँ नाम को भी न था। यहाँ विद्यालय का मेहमान प्रत्येक ब्रह्मचारी का मेहमान है, वह उसकी चारपाई बिछा देगा, उसके लिए पानी भर लाएगा और उसकी धोती भी खुशी से छाँट देगा। यह विद्यालय नहीं, किसी ऋषि का आश्रम मालूम होता है। ऐसे उत्साही युवक मैंने नहीं देखे। जो काम करते हैं, उसमे तन-मन से लिपट जाते हैं। प्रमाद की मात्रा इनमें बहुत ही कम है। कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए यह लोग सदैव उत्सुक रहते हैं।
साहित्य-परिषद् का उत्सव संध्या-समय हुआ। आचार्यजी का व्याख्यान हुआ। ब्रह्मचारियों ने अपनी-अपनी रचनाएँ सुनाई। कुछ साहित्यिक लेख थे, दो-चार गल्पें थीं, एक-दो लेख ऐतिहासिक थे। इन रचनाओं को किसी ऊँचे आदर्श से तोलना अन्याय होगा – ये प्रौढ़ लेखकों की कृतियाँ न थीं, पर किसी विद्यालय के शिष्यों को उन पर गर्व हो सकता है। हाँ, यहाँ जो संगीत सुनने में आया, उससे कुछ निराशा हुई। गुरुकुल में संगीत-शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं। शायद संगीत ब्रह्मचर्य के लिए बाधक समझा जाता हो। मगर मुझे तो ऐसी धार्मिक संकीर्णता यहाँ कहीं न दिखाई दी। सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे ब्रह्मचारियों में विचार-स्वातंत्र्य पर हुआ। उनके राजनैतिक , सामाजिक, धार्मिक विचारों में मुझे संकीर्णता का कोई चिह्न नहीं मिला। दूसरे दिन प्रीतिभोज था। भोजनगृह में सभी ब्रह्मचारी और आचार्य फर्श पर बैठकर थालियों में भोजन कर रहे थे। हमारे अंग्रेजी विद्यालयों में कुर्सियों और मेज़ों का व्यवहार होता है। यहाँ अभी तक अंग्रेज़ियत की वह हवा नहीं आयी। हमारे जातीय रीति-नीति, आचार-विचार की रक्षा अगर हो सकती है तो ऐसों ही संस्थाओं में हो सकती है। मगर शायद अब उसकी रक्षा करने की ज़रूरत ही नहीं समझी जाती। आजकल वही पक्का आर्य है, जो चाहे और सभी बातों में विदेशियों का गुलाम हो, केवल अन्य धर्मावलम्बियों को गाली देता जाए।
आज संध्या-समय एक कवि-सम्मेलन था। पंडित पद्मसिंह जी सभापति थे। ब्रह्मचारियों ने अपनी-अपनी रचनाएँ सुनायीं। अधिकांश कविताएँ हास्यास्पद थीं, मगर मैं ब्रह्मचारियों के साहस की तारीफ करूँगा कि उन्हें अपनी अंड-बंड रचनाएँ सुनाने में लेशमात्र भी संकोच न होता था। किसी हद तक तो यह बालोचित साहस सराहनीय है। हमने ऐसे बालक भी देखे हैं, जो किसी सभा में खड़े कर दिए जाएँ तो उनकी घिग्घी बँध जाएगी। उस झिझक के देखते तो यह धृष्टता फिर भी अच्छी है। पर रसिकजनों के सामने ऐसी रचनाएँ न सुनाना ही अच्छा, जिन्हें सुनकर हँसी आवे। रचनाओं के समाप्त हो जाने के बाद शर्माजी ने विचारपूर्ण वक्तृता कौशल दर्शाया। और ब्रह्मचारियों को खूब हँसाया। शर्माजी जितने विद्वान् हैं, उतने ही सरल और उदार है। और मेहमानवाज़ी तो उनका जौहर है।
तीसरे दिन हमने मुख्याधिष्ठाता जी के घर भोजन किया। उसका स्वाद अभी तक भूला नहीं। रामदेव जी उन सज्जनो में हैं, जिनकी बातों से जी नहीं भरता। ज्यों-ज्यों बातें मालूम होती हैं और मनोरंजन भी होता है, आप अंग्रेज़ी साहित्य के अच्छे ज्ञाता हैं और भारतीय इतिहास के तो आप पूरे माहिर हैं। ब्रह्मचारियों को उन पर असीम श्रद्धा है। गुरुकुल अगर कुछ न करे, तो भी इतने युवकों के सम्मुख सरल जीवन और उच्च विचार का आदर्श रखना ही उसके जीवित रहने के लिए काफी है।अंग्रेज़ी कॉलेजों में तो आवश्यकताओं की गुलामी सिखायी जाती है और अध्यापक लोग ही इस विद्या के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। ज़िंदगी की दौड़ में वे युवक क्या पेश पा सकते हैं, जिनके पैरों में ज़रूरतों की भारी बेड़ियाँ पड़ी हों। सरकारी विभागों में चाहे वे अच्छे पद पा जाएँ, पर सरकारी नौकरियों से तो राष्ट्र नहीं बनते। गुरुकुल ने अपने जीवन के थोड़े से सालों में राष्ट्र के जितने सेवक पैदा किये हैं, उतने और किसी विद्यालय ने न किये होंगे। डिग्रियाँ लेकर पद प्राप्त करना राष्ट्रीय सेवा नहीं। प्रचार और उद्धार के कामों को सँभालना ही राष्ट्रीय सेवा है। अब तक गुरुकुल ने एक सौ इकतालीस स्नातक निकाले हैं। उनमें सार्वजनिक जीवन में भाग लेने वालों की संख्या सत्तासी है। यह कहने में जरा भी अत्युक्ति नहीं है कि हिंदी भाषा को जितना प्रोत्साहन गुरुकुल से मिला है, उतना शायद ही और किसी विद्यालय से मिला हो। गुरुकुल की उपयोगिता के विषय में पहले जनता में बड़ा संदेह फैला हुआ था। पर गुरुकुल से निकले हुए स्नातकों का सांसारिक जीवन देखकर इस विषय की सभी शंकाएँ शांत हो जाती हैं। इस एक सौ इकतालीस स्नातकों में उनतीस तो गुरुकुलों में काम कर रहे हैं, नौ साहित्य-सेवा में लगे हुए हैं, तेईस आर्य-समाज के उपदेशक हैं, पाँच सफल वैद्य हैं, अठारह व्यापार में लगे हुए हैं और सात विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से दो उत्तीर्ण होकर लौट आये हैं। डॉक्टर प्राणनाथ हाल ही में इंग्लैंड से डॉक्टर होकर लौटे हैं, एक और महाशय बैरिस्टर हो आये हैं। पिछले साल चार ब्रह्मचारी सीनियर कैम्ब्रिज (Senior Cambridge) परीक्षा में सम्मिलित हुए और तीन पास हो गये। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मचारियों को अंग्रेज़ी में भी काफी अभ्यास हो जाता है। महाशय सत्यव्रत जी सिद्धांतालंकार ने हाल ही में ब्रह्मचर्य पर अंग्रेज़ी में एक ग्रंथ लिखा है। जिसकी शैली और भाषा दोनों ही परिमार्जित हैं। किसी यूनिवसिर्टी से के विद्यार्थी के लिए ऐसी पुस्तक लिखना गर्व का कारण हो सकता है।
गुरुकुल विद्यालय में एक आयर्वेुद विद्यालय भी है। यहाँ ब्रह्मचारियों को बूटियों तथा रसों का भी ज्ञान हो जाता हैं। शरीर विज्ञान की शिक्षा भी इन वैद्यों को दी जाती है। हमें आशा है कि यहाँ के पढ़े हुए वैद्यों द्वारा आयर्वेुद का उद्धार होगा। वे केवल पुरानी लकीर के फकीर नहीं होते, बल्कि मानव शारीर के तत्त्वों को जानते हैं और शल्य-चिकित्सा में भी दखल रखते हैं। गुरुकुल की प्राकृतिक शोभा का तो कहना ही क्या। बलवान् चरित्र ऐसे ही जलवायु में विकसित होते हैं। सामने गंगा की जल-क्रीड़ा है, पीछे पर्वतों का मौन संगीत। दाहिने-बाएँ मीलों तक शीशम और कत्थे के वृक्ष, ऐसी साफ छनी हुई, विमल वायु में साँस लेना स्वयं आत्मशुद्धि की एक क्रिया है। न शहरों का दूध-घी, न यहीं की स्वच्छ वायु। ब्रह्मचारी गंगा माता की गोद में किलोलें करते हैं, और बड़ी दूर तक तैरते चले जाते हैं, नगरों की दूषित जलवायु में यह गुण कहाँ। मगर पिछले बाढ़ ने विद्यालय को जो क्षति पहुँचायी है, उसको देखते हुए अब विद्यालय का स्थान बदल देने का प्रश्न आवश्यक हो गया है। इसका प्रबंध भी हो रहा है।
(माधुरी पत्रिका में अप्रैल 1928 में प्रकाशित)