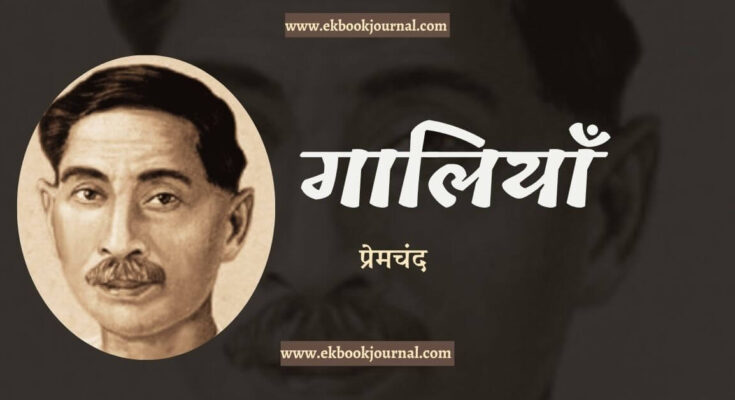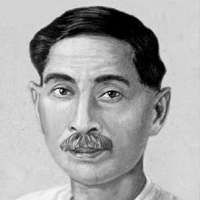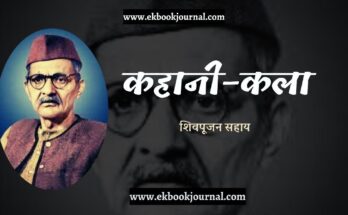हमारे देश में गालियाँ केवल गद्य में ही नहीं पद्य में भी दी जाती हैं। हम गालियाँ गाते हैं और वह भी ख़ुशी के मौक़े पर। अगर शोक के अवसर पर गालियाँ गायी जाएँ तो शायद उसकी यह व्याख्या की जा सके कि हम ज़ालिम आसमान और बेवफ़ा तक़दीर को कोस रहे हैं। लेकिन ख़ुशी के जलसों में गालियाँ गाना अनोखी बात है। हाँ, इन गालियों में वह शैतानियत, वह ख़ूँख़ारी और वह दिल को दुख पहुँचाने की बात नहीं होती जो ग़ुस्से की हालत में गालियों में पायी जाती है। तब भी इन गीतों का एक-एक शब्द दिलों में गंदे ख़याल और गंदी भावनाएँ उभारता है। इसकी व्याख्या इसके सिवा और क्या की जा सकती है कि हमारा कामुक स्वभाव वासना उभारने वाली गालियाँ सुनकर ख़ुश होता है। बारात दरवाज़े पर आयी और गालियों में उसका स्वागत किया गया और फिर लोग उसके आतिथ्य-सत्कार में लग गए लेकिन ज्योंही खाने का वक्त आया, लोग हाथ-पाँव धो-धोकर पत्तलों पर कढ़ी-भात खाने बैठे कि चारों तरफ़ से गालियों की बौछार होने लगी और गालियाँ भी ऐसी-वैसी नहीं, पंचमेल, कि शैतान सुने तो जहन्नुम से निकल भागे। लोग सपड़-सपड़ भात रखा रहे हैं, ढोल-मजीरे बज रहे हैं, वाह-वाह मची है और गालियाँ गायी जा रही हैं गोया पेट भरने के लिए भात के अलावा गालियाँ खाना भी ज़रूरी है। और है भी ऐसा ही। लोग ऐसे शौक़ से गालियाँ सुनते हैं कि शायद रामायण, महाभारत और सत्यनारायण की कथा भी न सुनी होगी। मुस्कराते हैं, मुग्ध होकर गर्दन हिलाते हैं और एक दूसरे का नाम गंदगी में लिथेड़े जाने के लिए पेश करते हैं। जिन महाशयों के नाम इस तरह पेश होते हैं वे इसे अपना सौभाग्य समझते हैं। और दावत ख़त्म होने के बाद कितने ही ऐसे लोग बच रहते हैं जिनके दिल में गालियाँ खाने की हवस बाक़ी रहती है। ख़ुशनसीब है वह आदमी जो इस वक़्त गालियाँ खाता है। सारी बिरादरी की आँखें उसकी तरफ़ उठती हैं। बावजूद इस आदर-सम्मान के वह ग़रीब बड़े विनयपूर्वक गर्दन झुकाए हुए है। कहीं-कहीं घर की औरतें यह फ़र्ज़ अदा करती हैं लेकिन ज़्यादातर जगहों में डोमनियाँ यह पाक रस्म अदा करने के लिए बुलायी जाती हैं। नहीं मालूम ये गीत किसने बनाए हैं। किन्हीं-किन्हीं गीतों में शायरी का रंग पाया जाता है। क्या अजब है, किसी रौशन तबीयत के आदमी ने इसी रंग में अपने फन का कमाल दिखाया हो। इस गाने के लिए गानेवालियों को इनाम देना पड़ता है। दुनिया में हिंदुओं के सिवा और कौन ऐसी जाति है जो गालियाँ खाए और गाँठ से रुपया ख़र्च करके, इस मैदान में कायस्थ लोग सभी फिरकों से बाज़ी ले गए हैं। उनके यहाँ बहुत ज़माना नहीं गुज़रा कि महफ़िलों में गालियाँ बक-बककर इल्मी लियाक़त दिखायी जाती थी। दूसरी जातियाँ शास्त्रार्थ और इल्मी बहसें करती हैं और कायस्थ हज़रात गंदी गालियाँ बकने में अपना पांडित्य दिखाते हैं। क्या उल्टी अक़्ल है। शुक्र है कि यह रिवाज अब कम होता जाता है वर्ना गाँव में किसी लड़के या लड़की की शादी ठहरी और गाँव भर के नौजवान और होनहार लड़के गालियों की ग़ज़लें याद करने लगते थे। हफ़्तों और महीनों तक गालियों को रटने के अलावा उन्हें और कोई काम नहीं था। घर के बड़े-बूढ़े शाम को दफ़्तर और कचहरी से लौटते तो लड़कों से यह गंदी ग़ज़लें सबक की तरह सुनते और लबोलहजा दुरुस्त करते। जब बच्चों को गालियाँ माँ के दूध के साथ पिलायी जाएँ तो नैतिक शक्ति क्योंकर आ सकती है।
ग़ुस्से में हम गाली बकें, दिल्लगी में हम गाली बकें, गालियाँ बककर लियाक़त का ज़ोर हम दिखाएँ, गीत में गाली हम गाएँ–ज़िंदगी का कोई काम इससे ख़ाली नहीं, यहाँ तक कि धार्मिक मामलों में भी हमारे यहाँ गाली बकने की ज़रूरत है। दूसरे सूबों का हमें तज़ुर्बा नहीं मगर संयुक्त प्रांत के कुछ हिस्सों में दीवाली के दो दिन बाद दूज के रोज़ गाली बकने वाली पूजा होती है। सारे गाँव या मुहल्ले की औरतें नहा-धोकर जमा होती हैं, ज़मीन पर गोबर का एक पुतला बनाया जाता है, इस पुतले के इर्द-गिर्द औरतें बेठती हैं और कुछ पान-फूल चढ़ाने के बाद गाली बकना शुरू कर देती हैं। यह त्योहार इसीलिए बनाया गया है। आज के दिन हर औरत का फ़र्ज़ है कि वह अपने प्यारों को गालियाँ दे। जो आज के दिन गालियों से बच जाएगा उसे साल भर के अंदर ज़रूर यमराज घसीट ले जाएँगे। गोया यमराज से बचने के लिए गालियों की यह मोटी दीवार उठायी गयी है । हमने काल से लड़ने के लिए कैसा हथियार निकाला! कहीं-कहीं यह रिवाज है कि दूज के दिन बजाय अपने प्यारों के दुश्मनों को गालियाँ दी जाती हैं और गोबर का पुतला फ़र्ज़ी दुश्मन समझा जाता है। दुश्मन को ख़ूब जी भर कोसने के बाद औरतें इस पुतले की छाती पर ईंट का एक टुकड़ा रख देती हैं और फिर उसे मूसल से कटना शुरू करती हैं। इस तरह दुश्मन का निशान गोया हस्ती के सफ़े से मिटा दिया जाता है। गालियों से केवल धर्म ख़ाली था, वह कसर भी पूरी हो गयी।
हमारी रुचि इतनी विकृत हो गयी है कि हममें से कितने ही शौक़ीन, रंगीन तबियत के लोग ऐसे निकलेंगे जो सुंदरियों के मुँह से गालियाँ सुनना सबसे बड़ा सौभाग्य समझते हैं। बदज़बानी भी गोया हसीनों के नखरे में दाख़िल है। प्रेमीजनों का यह सम्प्रदाय उस सुंदरी को हरगिज़ प्रेमिका न कहेगा जिसकी ज़बान में शोखी और तेजी नहीं। ज़बान का शोख होना माशूकियत का सबसे ज़रूरी जुज़ (अंश) समझा जाता है। मगर अफ़सोस कि ज़बान की शोख़ी का मतलब कुछ और ही ख़याल किया जाता है। अगर माशूक़ दिल्लगीबाज़ हाज़िरजवाब हो तब तो गोया चार चाँद लग गए। मगर हमारे यहाँ ज़बान की शोखी गाली बकने का दूसरा नाम है। मियाँ मजनूँ लैला से हुस्न का जकात तलब करते हैं। लैला तेवर बदलकर गाली दे बैठती है। मियाँ मजनूँ ज़रा और सरगर्म होते हैं तो लैला उनकी मैयत देखने की तमन्ना ज़ाहिर करने लगती है। इस गाली-गलौच का शुमार माशूक़ाना शोख़ी में दाख़िल है। जिस हालत में कि ज़बान से सच्चाई और आत्मीयता में डूबे हुए शब्द निकलने चाहिए उस हालत में हमारे यहाँ गाली-गलौज होने लगता है, और अक्सर निहायत गंदा, फोहश। मगर हमारे स्वर्ग-जैसे देश में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इन गालियों में मुहब्बत की दुगनी तेज़ शराब का मज़ा आता है और जिनकी महफ़िलें इस ज़बानी तेज़ी के बग़ैर सूनी और बेरोनक़ रहती है। हमारी तहज़ीब का ढंग ही निराला है। इसी नैतिक पतन ने हिंदुस्तान को आज ऐसी बेग़ैरत और बेशर्म क़ौम बना रक्खा है।
विलायत में बिलिंग्सगेट नाम का एक बाज़ार है। वहाँ की बदज़बानी सारे इंगलिस्तान में मशहूर है और किताबों में उसकी मिसाल दी जाती है, मगर हमारे हिंदुस्तान की मामूली बोलचाल के आगे बिलिंग्सगेट के मल्लाह भी शर्म से पानी-पानी हो जाएँगे।
गाली हमारा जातीय स्वभाव हो गयी है। किसी इक्के पर बैठ जाइए और सुनिए कि इक्केवान अपने घोड़े को कैसी गालियाँ देता है। ऐसी गंदी कि जी मतलाने लगे। वह ग़रीब घोड़ा और उसकी नेक माँ और बुज़ुर्ग बाप और नालायक दादा, सब इस नेकबख़्त औलाद की बदौलत गालियाँ पाते हैं। हिंदुस्तान ही तो है, यहाँ के जानवरों को भी गालियों से लगाव है। बैलगाड़ी वाला भी अपने बैलों को ऐसी फ़र्माइशी गालियाँ देता है। और तो था ही, सरकार बहादुर ने आजकल गालियाँ बकने के लिए एक महकमा क़ायम कर रक्खा है। इस महकमे में शरीफ़ज़ादे और रईसज़ादे लिए जाते है, उन्हें अच्छी-अच्छी तनख़्वाह दी जाती हैं और रिआया के अमन-चैन की ज़िम्मेदारी उन पर रक्खी जाती है। इस महकमे के लोग गालियों से बात करते हैं। उनके मुँह में जो बात निकलती है, गंदी, घिनौनी। ये लोग गालियाँ बकना हुकूमत की निशानी और अपने ओहदे की शान समझते हैं। यह भी हमारी टेढ़ी अक्ल की एक मिसाल है कि हम गाली बकने को अमीरी की शान समझते हैं। और देशों में ज़बान का सुथरापन और मिठास, चेहरे को गम्भीरता, शराफ़त और अमीरी के अंग समझे जाते हैं और हिंदुस्तान में ज़बान की गंदगी और चेहरे का झल्लापन हुकूमत का जुज़ ख़याल किया जाता है। देखिए मोटे जमींदार साहब अपने असामी को कैसी गालियाँ देते हैं। जनाब तहसीलदार साहब अपने बावर्ची को कैसी खरी-खोटी सुना रहे हैं और सेठ जी अपने कहार पर किन गंदे शब्दों में गरम होते हैं, ग़ुस्से से नहीं सिर्फ़ अपनी हुकूमत की शान जताने के लिए। गाली बकना हमारे यहाँ रईसी और शराफ़त में दाख़िल है। वाह रे हम।
इन फुटकर गालियों से तबियत भरती न देखकर हमारे बुज़ुर्गों ने होली नाम का एक त्योहार निकाला कि एक हफ़्ते तक हर ख़ास व आम ख़ूब दिल खोलकर गालियाँ देते हैं। यह त्योहार हमारी ज़िंदादिली का त्योहार है। होली के दिनों में हमारी तबियतें ख़ूब उभार पर होती हैं और हफ़्ते भर तक ज़बानी गंदगी का एक ग़ुबार-सा हमारे दिल व दिमाग़ पर छाया रहता है। जिसने होली के दिन दो-चार कबीर न गाये और दो-चार दर्ज़न गंदी बातें ज़बान से न निकालीं वह भी कहेगा कि हम आदमी हैं। ज़िंदगी तो ज़िंदादिली का नाम है। लखनऊ में एक ज़िंदादिली अख़बार है। वह भी होली में मस्त हो जाता है और मोटे-मोटे अक्षरों में पुकारता है–
आयी होली आयी होली, हमने अपनी धोती खोली
यह इस ज़िंदादिल अख़बार की ज़िंदादिली है। वह सभ्य और सुसंस्कृत रुचि का समर्थक समझा जाता है। लेकिन जिस देश में गालियों का ऐसा रिवाज हो वहाँ इसी का सुथरे मज़ाक में शुमार है। कुछ हिंदी अख़बारों की ज़िंदादिली उन दिनों अथाह हो जाती है। निरंतर कबीरें छपती हैं और अधिकांश कबीरें शब्दों के अलंकार के पर्दे में गालियों से भरी हुई होती हैं। अगर किसी दूसरी क़ौम का आदमी इन दो हफ़्तों के हिंदी अख़बार उठाकर देखे तो शायद दुबारा उनकी सूरत देखने का नाम न लेगा। हमारे क़ौमी अख़बारों की यह हालत हो जाती है।
तकिया कलाम के तौर पर भी गालियाँ बकने का रिवाज है और इस मर्ज़ में ज़्यादातर नीम-पढ़े लोग गिरफ़्तार पाए जाते हैं। ये लोग कोई एक गाली चुन लेते हैं और बातचीत के दौरान में उसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि वह उनका तकिया कलाम हो जाती है और बहुत बार उनके मुँह से अनायास निकल पड़ती है। यह निहायत शर्मनाक आदत है। इससे नैतिक दुर्बलता का पता चलता है और बातचीत की गम्भीरता बिलकुल धूल में मिल जाती है। जिन लोगों को ऐसी आदत पड़ गयी हो उन्हें तबियत पर ज़ोर डालकर ज़बान में सफ़ाई पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए।
क़िस्सा कोताह, हम चाहे किसी और बात में शेर न हों, बदज़बानी में हम बेजोड़ हैं। कोई क़ौम इस मैदान में हमको नीचा नहीं दिखा सकती। यह हम मानते हैं कि हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी ज़बान की पाकीज़गी पर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता मगर क़ौमी हैसियत से हम इस ज़बर्दस्त कमज़ोरी का शिकार हो रहे हैं। क़ौम की उन्नति या अवनति थोड़े से चुने हुए लोगों के निजी गुणों पर निर्भर नहीं हो सकती।
सच तो यह है कि अभी तक हमारे मार्गदर्शकों ने इस महामारी को जड़ से खोदने की सरगर्म कोशिश नहीं की, शिक्षा की मंदगति पर इसके सुधार को छोड़ दिया और जनसाधारण की शिक्षा जैसी कुछ उन्नति कर रही है वह सूरज की तरह रौशन है। इस बात को दुहराने की ज़रूरत नहीं कि गालियों का असर हमारे आचरण पर बहुत ख़राब पड़ता है। गालियाँ हमारी बुरी भावनाओं को उभारती हैं और स्वाभिमान व लाज-संकोच की चेतना को दिलों से कम करती हैं जो हमको दूसरी क़ौमों की निगाहों में ऊँचा उठाने के लिए ज़रूरी है।
(मूल रूप से उर्दू में लिखा यह निबंध उर्दू मासिक पत्रिका ‘ज़माना’ के दिसंबर 1909 अंक में प्रकाशित हुआ था। )