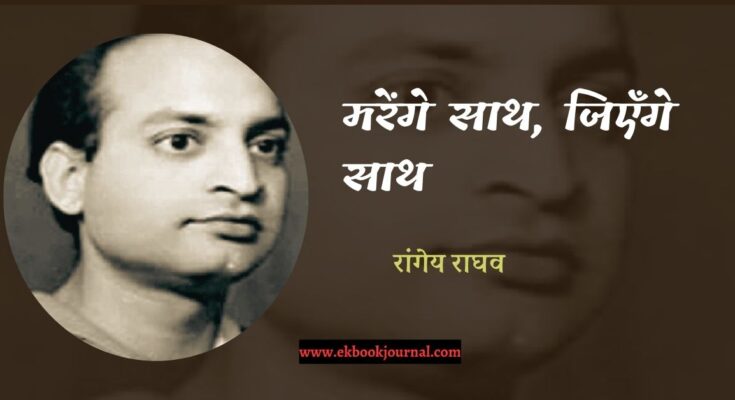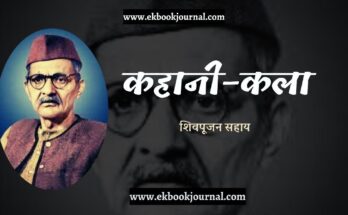पगडंडी, पतली-दुबली लजीली। उस पर हमारे पैरों का बोझ। हरियाली में जाकर वह लजवंती खो गयी। छेवड़िया ऊँघ रहा था। हवा सनसना रही थी। मन भारी था।
किंतु चाँदअली ने टीका लगवाने से इंकार कर दिया। एक बार उसके टीका लग चुका है, फिर क्यों? छोटे-छोटे अलग-अलग बसे घरों को देख विलायत के गाँवों की सुनी-सुनाई बातें याद हो आती हैं। कहते हैं हर घर के चारों तरफ़ जगह रहती है। जिन पर पेड़ों की छाया। मालूम नहीं कहाँ तक सच है। बचपन में एक मास्टर साहब पढ़ाया करते थे। उन्हीं ने कहा था पेरिस की सड़कें रबड़ की होती हैं। तब मान भी लिया था।
साढ़े पाँच सौ घर, उनीदें-से, थके-माँदे से। गाँव पाड़ों में विभाजित है। मन हँसता है, मन रोता है, न रोता है, न हँसता है।
कल शाम को डॉ० मंडल की छत पर एक सभा हुई थी। डॉक्टर विद्यार्थी ने कहा था एक मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए जिसमें स्थानीय डॉक्टर हों। वह अपना ज़िला या सबडिवीज़न सँभाले। किंतु काला कोट पहने एक डॉक्टर के मुँह पर हँसी खेल उठी। यह त्याग कौन करे!
हिंदू-मुसलमानों में झगड़े उठे, बोर्ड भी अंत में बन ही गया, किंतु मैं सोचता हूँ…
सोचता हूँ मनुष्य वर्गों में फँसकर कर्त्तव्य को त्याग कहता है। पड़ोस में आग लग रही है और वह निस्सहाय-सा पूछता है– मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ?
अंत में लोगों ने कहा– हमें अपनी मदद अपने आप करनी होगी। मैंने यह भी सुना था।
टैक्सटाइल वर्कर्स यूनियन के दो मज़दूर, दो स्थानीय विद्यार्थी आज गाँव में टीका लगाने आए थे।
हम चल रहे थे।
एक मरियल किसान हल पर पैर रखकर एक बूढ़े से बातें कर रहा था। वह हमें देखकर मुस्कराया। एक लड़का आम के पत्तों की सींकों से बिंधी टोपी लगाये घूम रहा था।
एक लड़की चीख़ उठी– “दो सौ जो मर गये उनके टीका लगाओगे?”
विक्षुब्ध हो गया है पवन, उन्मन, सनसन! वही संध्या का अविश्वास। मनुष्य की कठोर यातना के सम्मुख हलचल!
एक मज़दूर ने टोपीवाले बच्चे को बुलाया और उसके हाथ पर स्पिरिट लगायी। अचानक ही एक बुढ़िया चिल्ला उठी– “मर जाएँगे तो मर जाएँगे, मगर टीका नहीं लेंगे।”
ज़ियाउद्दीन भौं सिकोड़ता है।
एक जुलाहा झोंपड़ी के आगे बरामदे में बैठा ताना-बाना बुन रहा है। वह थक-थक जाता है। गाँव में अपूर्व हरियाली है। अब इन गड्ढों में फिर पानी भर जायेगा और बरसात में मलेरिया फिर पनपेगा, मनुष्य मरेंगे, दलदलों पर लाशें तैर उठेंगी, मच्छर भनभन करेंगे…
कौन आयेगा इतनी दूर से उनके लिए? वह विस्मित हैं। एक बालक हमें देखकर मुस्करा रहा है। बालक का रूप मुरझाया हुआ है। सूखी बेल पर ओस चमक रही है आज–शायद नये जीवन का प्रभात आरम्भ हो गया है।
बालक सहर्ष टीका लगवा रहा था। माँ विस्मित थी। पिता के जीवित रहने का सवाल ही नहीं उठता। बालक का नाम है गादून। बड़ा होकर वह हमें भूल जायेगा। तब बूढ़ी माँ शायद कहेगी– “बड़ी दूर से आये थे एक बार कुछ डॉक्टर लड़के क्योंकि बंगाल भूखा था और लोग मर रहे थे।”
छह या सात बरस का बालक चाँदअली से कह रहा है– “बाद में तो दाम देकर भी टीका नहीं लगवा सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौजी आएँगे और डाँटेंगे।”
उसकी माँ पूछती है– “बाप रे। यह भी आदमी हैं, जो इतनी दूर से आये हैं?”
टैक्सटाइल यूनियन का मज़दूर कहता है– “माँ हम जो भूखे हैं बीमार।”
सबके स्वर गद्गद हैं। वृद्धा फिर पूछती है–“तुम्हारे माँ है?”
ज़ियाउद्दीन कहता है– “नहीं मैं दुनिया में अकेला हूँ। एक बहिन है छोटी। और कोई नहीं।”
औरों के माँ हैं।
वृद्धा कहती है– “कैसी होंगी वे माँ। देवी? बंगाल की माँओं ने कब भेजा हमारे लिए अपने पूतों को? पर तुम अकेले हो?” उसकी आँखों में पानी आ गया। जैसे औरों के लौटने पर तो उनकी माँओं का दुलार उन्हें मिलेगा ही। यह कौन है ज़ियाउद्दीन जिसे कभी स्नेह नहीं मिला और फिर भी एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों को अपने स्नेह का अक्षय कोष लुटाने आ गया है। क्षण-भर को हम सब विभोर हैं। स्नेह का शुल्क आदि के रूप में लिया जानेवाला धन आदान-प्रदान हो रहा है। वहाँ जहाँ कोई अपने से बाहर नहीं सोचता।
किंतु मैं जानता हूँ, मरघट में प्यार के बादल उमड़ते हैं, उतना कोई कहीं और प्यार नहीं करता। दुश्मन भी दोस्त हो जाता है।
“तुम साथी हो?” एक जुलाहे ने पूछा। अब जैसे हम सब एक हो गये। संस्कृति, भाषा, भाव सबके भेद टूट गये। एक हो गये हम। मनुष्य… केवल मनुष्य। परदेवाली स्त्री ने मुँह खोलकर टीका लगवाया। चाँदअली अपने आप हाथ बढ़ा रहा है।
गादून अब भी मुस्करा रहा है। हम गाँव से चल दिये हैं।
जुलाहे धीरे-धीरे कात रहे हैं, बुन रहे हैं–सुदूर… हलचल से दूर, आग में जलते से। पेड़-पेड़ पर लपट छा रही है। भूखा धुआँ जैसे आकाश में घुमड़ रहा है। बीमारियों से भूमि भट्ठी की तरह धधक रही है। कफ़न के बक्सों-से यह झोंपड़े… आदमी उनमें रेंगते कीड़े…
पाड़ा… पाड़ा… गाँव… गाँव… ऊँचे दाम, ख़रीदने की अशक्ति… नारी की लाश… मृत्यु… गाँव दूर रह गया था। पीछे हरियाली शेष थी। हवा गर्म होने लगी थी।
अब हम फिर बस्ती में पहुँच गये थे।
टाउन के बाहर जहाँ रेल की पटरी के बाहर छोटी-छोटी गंदी-सी दुकानें हैं, उन्हीं के सामने एक लम्बा-सा अहाता है। बायीं तरफ़ बाबुओं के क्वार्टर हैं। अहाते के भीतर कई कमरे बने हैं। उन्हीं में मज़दूरों के रहने की जगह है। पीछे की तरफ़ ईंट पकाने के बड़े-बड़े भट्टे हैं। दूर से उनकी चिमनियों में घुमड़ता हुआ धुआँ आकाश में लहराया करता है। यहाँ काफ़ी हिंदुस्तानी और उड़िया मज़दूर हैं। ज़ियाउद्दीन, आसाम का विद्यार्थी, इंजेक्शन और इनोक्यूलेशन लगाता हुआ दो मज़दूरों के साथ घूम रहा था।
एक जगह हम लोग ठिठक गये। द्वार पर कई साड़ियाँ सूख रही थीं। हम समझे शायद यहाँ सिर्फ़ औरतें हैं। किंतु इसी समय भीतर से एक बालक निकलकर कहने लगा–“आओ न बाबू, भीतर आओ!”
हम लोग भीतर चले गये। सब लोग घरों से बाहर निकल आये थे। उनके चेहरों पर जैसे एक बड़ा प्रश्न-सूचक चिह्न था। वह जो अपने पेट के लिए इतनी दूर पड़े थे, उन्होंने इस बात पर विस्मय किया कि यह डॉक्टर बिना पैसे के इतनी दूर से उनके ही लिए आये थे। वे श्रद्धा, और सन्देह में कुछ निश्चय नहीं कर पाये थे। ज़ियाउद्दीन इन्जेक्शन देने के सिलसिले में लग गया। लोगों में एक अजीब हिचकिचाहट थी। एक मज़दूर ने कहा–“टीका नहीं बाबा। ईश्वर ने हमें बनाया है। वही हमें बचायेगा।”
बहुत दिनों से ऐसी बात नहीं सुनी थी। वास्तविकता की जानकारी ने लाखों को बता दिया था कि परमात्मा का इसमें कोई दोष नहीं, यदि बाज लोगों को चावल मिलना बंद हो गया था। मैं देख रहा था, अभी भी बंगाल में निराशा छा रही थी।
एक मज़दूर साफ़ धोती पहने, बाल काढ़े, अपने कमरे के द्वार पर बैठा था। उसकी बच्ची पास में बैठी गाना गा रही थी। अभी हम उसके द्वार पर पहुँचे भी न थे कि उस स्त्री ने भीतर से अपने छोटे बालक को बाहर दे दिया। मज़दूर ने कहा–“क्या है? इसे बाहर क्यों कर दिया?”
स्त्री ने अंदर से हल्के से कहा–“बच्चा है। इसके टीका लगवा लो।”
पति ने कुछ देर तक सोचा और बच्चा हमारे सामने कर दिया। ज़ियाउद्दीन कभी-कभी उनके मना करने पर हारा-सा कह उठता था–“अरे ये ही जब हम पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर और किसी की चाह है हमें?”
हमारे साथ का मज़दूर साथी कह रहा था–“डॉक्टर! जिसे तुम अविश्वास कहते हो, वह वास्तव में अपनेपन का हठ है। सदियों से जो कभी नहीं पढ़े-लिखे, वे तुम्हें अपना समझकर ही तो सवाल करते हैं, मना करते हैं, फिर मान जाते हैं। पर जब फ़ौज यहाँ आयी थी, तब क्या यह सब हुआ था? हुक्म होता था। उधर, इधर, मज़दूर की पत्नी, बच्चे, सब आस्तीन खोलकर लाइन में खड़े हो जाते थे। किंतु क्या वह ज़बरदस्ती की दवा फ़ायदा कर सकी? आज वह तुमसे पच्चीस सवाल पूछते हैं। फ़ौजियों से तो कुछ नहीं पूछते थे। और देखा न तुमने परिणाम। सब के टीके जानकारी न होने के कारण गंदगी से पक गये हैं।”
मैंने देखा वह असंख्य जनता के दुःख से विक्षुब्ध हो उठा था। इसी समय एक आदमी ने कहा–“मुझे छोड़ तू भय्या। मैं नहीं। मुझे तो परमात्मा की इच्छा होगी तो कुछ भी न होगा।”
एक अधेड़ औरत ने कहा–“महाजनों ने नाज चुराया, अकाल पड़ा, क्या परमात्मा ने यह भी चाहा था?”
वह आदमी एकदम चौंक उठा–“तू दीदी? ऐसा तो नहीं हुआ।”
“तो” औरत कहने लगी, “बिना हाथ उठाये ही क्या भात तेरे मुँह में पहुँच जायेगा? मत लगवा टीका। तू बीमार हो लीजो, तेरे बीबी बच्चे को अपनी सौगात दीजो, मगर जो बस्ती में तूने यह बसंत (चेचक) और हैजा फिर से फैलाया तो?”
एकाएक वह आदमी काँप उठा, मानो अज्ञात आशंकायों ने उसे घेर लिया था।
वही मज़दूरिन बोलती रही–“क्या सदा ही हम पागल और मूर्ख बने रहेंगे? घर पहले ही क्यों न साफ़ कर लिया जाय?”
अबके उस आदमी ने कहा–“दीदी तुम कहती तो हो मगर क्या तुम्हें एकदम भूल गया है कि रामचरण की बेटी, काशीनाथ का भाई, सबके क्या टीके लगे नहीं थे जो फिर से उनके घर में बसंत फैल गया और रामचरण की बेटी तो बेचारी…”
वह कह नहीं सका मानो उसने आवेश में बाज़ी जीत ली थी।
औरत ने आगे बढ़कर कहा–“फिर भी देखो काशीनाथ के भाई के अब चिह्न तो नहीं, वर्ना वह भी होते। पहले यदि सौ को होता तो अब पाँच को। अरे वह तो गंदगी से मरते हैं, बदपरहेज़ी से मरते हैं। याद है रामचरण की बेटी, लाड़ली कभी भी अपनी ज़बान रोकती थी? न, न बाबा, तू भले ही न लगवा, मगर बस्ती की बहुओं, माँओं और बच्चों की आहों की क़सम, तू यहाँ बीमारी फैलाकर नहीं रह सकता।”
वह आदमी क्षण-भर चुप रहा। और हमने विस्मय से देखा उसने हर्ष से अपना हाथ खोलकर बढ़ा दिया।
वह कह रहा था–“दिल तो अब भी हिचकिचाता है, मगर क्या बस्ती में रहकर एक बनकर न रहना चाहिये? क्या मैं अपनी वजह से दूसरों को मरने दूँगा! अरे हम साथ रहते हैं, जिएँगे तो साथ, मरेंगे तो साथ।”
ज़ियाउद्दीन के होठों पर अद्भुत स्फूर्ति मुस्करा रही थी। मैं देख रहा था। आज हम जीवन के एक नये पहलू के सामने खड़े थे। सारा अविश्वास क्षण-भर को भूल गया था। मनुष्य जब अपने आप बढ़ता है तब दूसरे उसके साथ ही चलने को मजबूर होते हैं। धीरेनदास की बातें सच थीं। उसने कहा था कि कुष्टिया के जीवन में तुम लोगों का बड़ा भारी हाथ होगा। जब तुम चले जाओगे तब भी हमारा साहस नहीं टूटेगा। विद्यार्थियों में एक नया जीवन भर उठेगा। देखते नहीं हो मज़दूर तुम्हें कितना प्यार करते हैं।
और मज़दूरों की याद ने मुझे घेर लिया। लम्बी मूँछोंवाले, नीली कमीज़ पहने हुए उस जाग्रत मज़दूर ने गीत सुनाये थे अपने ही स्टाइल में। छोटा-सा टाउन। उसमें ऐसा जागरण।
हिटलर स्टालिन से अपने प्राणों की भीख माँग रहा है–“तुम ही मेरे माँ-बाप हो, मैं ख़ून से भीगा हुआ हूँ – साफ़ नहीं हो सकता…”
अत्याचार मानवता से भीख माँग रहा था….
और रोटी पर रसगुल्ले का रस लगाते हुए गाया था उस मोटी आवाज़ वाले लड़के ने–
कांग्रेस लीगेर मिलन बिना
देशेर संकट दूर होबे ना… .
दूर होबे ना
और विद्यार्थी हिंदू, मुसलमान, मज़दूर, गाँव से आये किसान, आधे भूखे… रात को जो मीटिंग में लड़ चुके थे गा रहे थे, उस समय–दूर होबे ना, दूर होबे ना… क्योंकि समस्त बंगाल से ध्वनि आ रही थी–
देश जले, देश जले, देश जले रे
हम सबसे मिले, हिंदू, मुसलमान। और मंदिर में उस दिन समवेत गीतनृत्य हो रहा था–‘हे काली माता रोको यह अकाल, यह महामारी…’ बंगाल में अब भी महाकाली की प्रचंड शक्ति है… बालक, पुरुष, स्त्री सब जाग रहे हैं…
मेरे सामने अज़हर है, गाँव का नेता। हरिशंकरपुरा का निवासी। वह कह रहा है– “सात सौ की आबादी में से दो सौ पचास मर चुके हैं। किसानों और मज़दूरों को कालाज़ार खा गया है। किसान ज़मीन बेच चुके हैं । इस बार यह आमन की फ़सल पुराने क़र्ज़ चुकाने में निकलती जा रही है।”
अनंत दुःखों की कथा है…
रफ़ाल सरदार के लड़के ने ज्वर से कराहकर करवट ली। माँ देख रही है। चुप है। डॉक्टर के लिए दाम नहीं है। बाप चुप है। आठ रोज़ से खाने को नहीं दिया है। लड़का तड़प रहा है। पाँच और बच्चे, कोई पड़ा है, कोई चुप बैठा है। उनके जीवित रहने की आशा है, तभी मरते के मुँह में दाना डालने का अन्याय कोई नहीं करना चाहता। माँ भी नहीं। बाप देख रहा है… लड़का तड़प रहा है…
माँ का दिल नहीं धड़कता। वह मर गयी है। हार्टफ़ेल हो गया है। रफ़ाल सरदार मुस्कराता उठता है : एक और कम हो गया…
बाहर गाँव के पथ पर एक बुड्ढी पड़ी है। भीख भी नहीं माँगती; कोई दे जाता है, खा लेती है। वह दोनों वक़्त नहीं खा पाती, क्योंकि देनेवाले ही मुश्किल से एक बार खा पाते हैं।
मियाँजान उसके पास जा बैठा है। उसके शरीर पर सूजन है, घाव है।
बुढ़िया उससे घृणा नहीं करती। वह बुढ़िया को प्यार नहीं करता। रोटी के टुकड़ों पर दोनों झगड़ते हैं, भात के कौर धूल में से बीन-बीनकर खाते हैं..
वह दिन बीत गये हैं तब बंगाल में लोग सड़क पर मरते थे। कपड़ा जल चुका है, मगर उसका धुआँ अभी तक कसैला और कड़ुआ जिसकी आँखों में लग जाये, आँसू गिर-गिर जायें। घुमड़न अंतराल में उमड़ती रहे। बुढ़िया बैठी रहे, मियाँजान घावों को खुजलाता रहे–दुनिया आगरे का ताजमहल देखना छोड़ दे। बादशाह और मलका अब मिट्टी है, किंतु यह दोनों अभी जीवित मिट्टी हैं–देखें, सब देखें।
अँधेरी रात में पुल पर खड़े हैं हम। एक मादकता, एक सुरभि-भीनी तेज़ हवा, कहो समीरण, झकझोरती, मन को भर-सी देती। उस पर मज़दूरों का गीत उमड़ता तैरता चला आ रहा है–जाग देश जाग! सर्वहारा में शक्ति है कि वह रात को जगा सके। जब देश सो रहा हो तब उसे जगाने के लिए पुकार उठा सके। आकाश सिहर रहा है। मेरे मन में एक तृप्ति है कि अभी कुछ नहीं हुआ, किंतु होगा वही जो होने को है : कि हम ठीक हैं, कि हमारी विजय होगी।
पटरियों पर सिगनल की लाल रोशनी झलक रही है। एक मज़दूर कह रहा है– “एक दिन पारसाल इन्हीं दिनों हम रात को यहीं खड़े थे। उस दिन हम सब भी भूखे थे। अकाल ज़ोरों पर था। मिल से मिलनेवाला चावल काफ़ी नहीं पड़ता था। बादल आकाश में छाये हुए थे, बिजली चमक रही थी। हम सब चुप खड़े थे। अचानक हमने देखा कि बिजली की कौंध में कोई आकर पटरी पर लेट गया। हम दौड़कर गये। देखा–वह मरने के लिए, रेल से कटकर मरने के लिए लोहे पर सिर रखे था। उसके दाँत भिंचे हुए थे। नसें उभरी हुई थीं। दौड़कर आती हुई रेल रुकवायी गयी। उससे पूछा। उसने कुछ भी नहीं कहा। वह मौन था, जैसे गूँगा हो। बहुत देर बाद उसने बताया–ज़िला फ़रीदपुर के मदारीपुर से चलकर आया था वह। घर में दस आदमी थे और खेत थे। खेत बिक गये, सब कुछ बिक गया और कुछ लुट गया–घर के बाहर का बाज़ार में, घर के भीतर का मौत के हाथ। कुष्टिया के लंगरखाने भी जब उसको कुछ न दे सके तब वह बहादुरी से मरने आया था।”
उसके बाद की कहानी कोई ख़ास नहीं। उसी ने बताया था कि एक दिन उसकी बेटी और जमाई एक साथ सो रहे थे। बग़ल-बग़ल में। सुबह दोनों की मुट्ठियाँ बँधी थीं। आँखें चढ़ी हुई और साँस, कहीं दूर चली गयी थी।
मज़दूर चुप हो गया। हो गया कुष्टिया पूरा। क्या बचा है अब देखना!
पहली कहानी–हम सुखी थे।
दूसरी गाथा–अकाल आया।
नाटक–दाम बढ़े, चावल नहीं मिला।
प्रहसन: लोग मरने लगे।
विष्कम्भक: मलेरिया शुरू हुआ।
महाकाव्य: मौत… मौत… मौत…
मेरी पुकार–जिएँगे साथ, जिएँगे साथ, नहीं मरेंगे, क्योंकि जीना है–जीना है–जीना है…