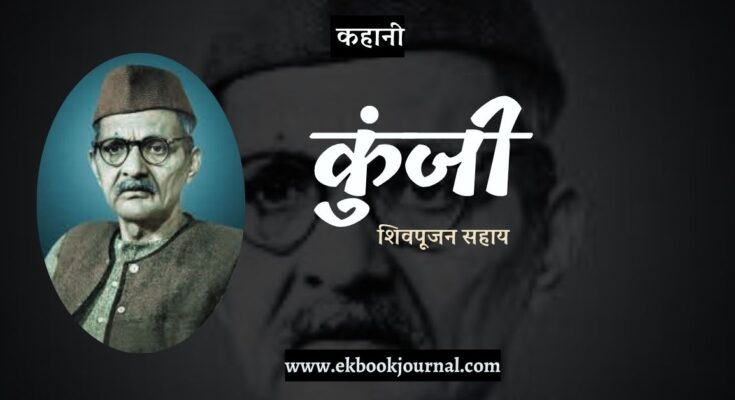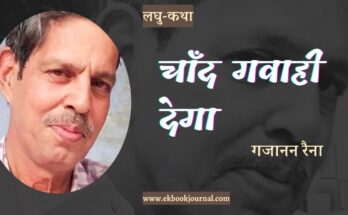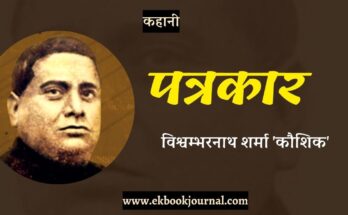अगर मौके से टैक्सी-मोटर न मिल जाती तो समझ लीजिए कि गाड़ी छूट ही चुकी थी। मोटर ने तो एक का डेढ़ लेकर ठीक समय पर हावड़ा पहुँचा दिया, मगर वहाँ स्टेशन के कुली असबाब उठाने में हुज्जत करने लगे। पहले तो वे कंक की तरह असबाब पर टूट पड़े। फिर बारी-बारी करके एक रुपया, डेढ़ रुपया तक नीलामी डाक बोल गये! कुली क्या हैं, तीर्थ के पंडे हैं!
एक संन्यासी ने झट आकर मेरी पेटी उठा ली और कहा, “तुम बिस्तर ले लो, जल्दी करो, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी।”
यह कहकर संन्यासी बाबा आगे बढ़े। मैं बिस्तर लेकर ताबड़तोड़ उनके पीछे दौड़ा। कुली बेचारे मुँह ताकते रह गये।
ज्योंही संन्यासी बाबा के साथ मैं दूसरे दरजे में सवार हुआ त्योंही गाड़ी खुल गयी। संन्यासी ने कहा, “तुम जैसे नवयुवक को तो स्वावलम्बी होना चाहिए। तुम कुलियों का मुँह क्यों ताकते थे? क्या दूसरे पर आश्रित रहकर तुम सुखी होना चाहते हो? क्या अमीरी का यह कोई खास लक्षण है? तुम्हें तो स्वयंसेवक की तरह दूसरों की सहायता के लिए खुद मुस्तैद रहना चाहिए। जब तुम्हें स्वयं दूसरे की सहायता की दरकार है तब तुम औरों की सहायता क्या करोगे?”
“गठरी भारी थी। गाड़ी खुलने का वक्त हो चुका था। इसीलिए मैं कुलियों के फंदे में मुसाफिरखाने में ही पड़ा झखता रहता।”
“तुम जाते कहाँ हो?”
“काशी जाता हूँ। मेरे एक सम्बंधी बीमार हैं। मरने के लिए काशी आये हुए हैं। आज ही उनका तार मिला है। यह गाड़ी छूट जाती तो मेरा सर्वनाश हो जाता।”
“ऐसी कौन-सी बात है?”
“मरने वाले सज्जन बम्बई के बड़े भारी सेठ हैं। मैं उनका मुनीम हूँ। मरने से पहले पहुँच जाऊँगा तो कुछ हाथ लग जायगा।”
“क्या हाथ लगेगा?”
“किस्मत भी फूट गयी तो दो लाख से कम नहीं।”
“तब तो तुम दो लाख के लिए जा रहे हो, अपने मालिक के लिए नहीं।”
“दोनों के लिए समझ लीजिए।”
“किंतु प्रधान दो लाख ही समझे। क्यों?”
“आप संन्यासी हैं। हम लोग संसारी हैं। हम लोगों के लिए तो नगद-नारायण ही सब कुछ है।”
मेरी बात सुनकर संन्यासी बाबा शांत और गम्भीर हो गये। उन्होंने दीर्घ निःश्वास खींचकर कहा, “भज गोविंदं भज गोविंदं भज मूढ़मते।”
यह कहकर उन्होंने आकाश की ओर देखा, और हाथ जोड़कर आँखें बंद किये हुए सिर झुकाया; फिर मेरी ओर देखने लगे।
मैंने पूछा, “महाराज! अभी आपने यह क्या किया है?”
“उस परमात्मा की वंदना की है, जिसकी यह लीला है।”
“लीला कौन-सी?”
“स्वार्थ की विकट लीला के सिवा इस संसार में दूसरी लीला कौन-सी है?”
“क्या स्वार्थ के सिवा इस संसार में कुछ है ही नहीं?”
“है क्यों नहीं? किंतु प्रत्यक्ष तो स्वार्थ ही है। और जो कुछ है, वह अंतरिक्ष है। उस अदृश्य लीला को यह आँखें नहीं देख सकती।”
“तो फिर उन्हें देखने के लिए क्या ईश्वर ने इन दो के सिवा कोई तीसरी आँख भी बनायी है?”
“हाँ, वही ज्ञानचक्षु है। उसके खुल जाने पर ये दोनों आँखें बंद हो जाती हैं।”
“तो क्या मनुष्य अंधा हो जाता है?”
“नहीं, सूर्योदय के बाद दीपक की आवश्यकता नहीं रहती।”
“अच्छा, तो वह ज्ञान की आँख खुलती कब है?”
“जब ईश्वर की दया होती है।”
“आप पर पहले-पहल कब ईश्वर की दया हुई थी?”
इतना पूछते ही संन्यासी बाब फिर शांत और गम्भीर हो गये। देर पूर्ववत् ध्यानस्थ हो, मेरी तरफ मुखातिब होकर कहने लगे, “जिस विधाता ने हंस को श्वेत वर्ण, शुक को हरित वर्ण, कोकिल को कृष वर्ण, कोकनद को अरुणवर्ण, चम्पा को पीत वर्ण और इंद्रधनुष को विविध वर्णों से रंजित किया तथा मयूरपुच्छ को सुचारु चमकीले रंगों से चित्रित किया, उसी विधाता ने इस संसार पर स्वार्थ का गाढ़ा रंग चढ़ा दिया। जिस प्रकार, अग्नि से ताप, सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा से चंद्रिका, पृथ्वी से गंध, जल से शीतलता, बिजली से चंचलता, मेघ से श्यामता और पुष्प से सुकुमारता दूर नहीं की जा सकती; उसी प्रकार संसार से स्वार्थपरता भी अलग नहीं की जा सकती।
“दरिद्रता और दुःख का जैसा घनिष्ठ सम्बंध है, इस संसार से स्वार्थ का भी वैसा ही गहरा सम्बंध है। जिस प्रकार आलस्य सब रोगों का घर है, उसी प्रकार यह संसार भी समस्त स्वार्थों का अखाड़ा है। यहाँ यदि स्वार्थों के संघर्ष से दारुण दावानल न धधकता होता, तो यह नंदन-कानन से भी अधिक रमणीय और शीतल समझा जाता। इस विलक्षण संसार के प्रत्येक कण में स्वार्थ की सत्ता भरी है। यदि स्वार्थ निकल जाय, तो इस संसार की विचित्रताएँ रहस्य-शून्य हो जाएँ।
“जो स्वार्थ का फंदा तोड़ देता है, वह इस संसार-कारागार से मुक्त हो जाता है। वह संसार को परास्त कर देता है। संसार उसके चरणों में झुक जाता है और वह संसार के सिर पर अभयवरद हाथ रख देता है। किंतु स्वार्थ आकाशवल्लरी की तरह इस विश्व-विटप पर छा रहा है। उस उलझनदार जाल को तोड़ना सहज नहीं है।”
मैंने पूछा, “महाराज! आपने उस जाल को कैसे तोड़ा था?”
“अभी तक मैं नहीं तोड़ सका! हाँ, तोड़ सकूँगा, ऐसी आशा है। उस आशा की ज्योति मेरे पिता की धधकती हुई चिता की ज्वाला ने जलायी थी।”
“आपकी रामकहानी सुनने के लिए उत्सुकता हो रही है। क्या आप कृपा करके सुनाएँगे?”
“यदि उसके सुनने से तुम्हारा कुछ उपकार हो सकता है, तो मैं संक्षेप में सुना सकता हूँ।”
“आपके आदर्श जीवन-वृत्तांत से मेरा अवश्य ही उपकार होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। सत्संग की महिमा सबसे बढ़कर है। आपकी बातों से मेरा कौतूहल भी शांत होगा और मैं बहुत-कुछ उपदेश भी प्राप्त करूँगा।”
“एवमस्तु! मैं मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े जमींदार का पुत्र था। मेरे पिता चार भाई थे। जब मेरे पिता मृत्युशय्या पर पड़े-पड़े अपनी अंतिम घड़ियाँ गिन रहे थे, तब मैं बिलकुल मदांध नवयुवक था। मेरे पास सांसारिक चिंताएँ फटकने नहीं पाती थीं।
“कभी -कभी मैं अपने पिता की रोग-शय्या के पास बैठकर उनके सजल नेत्रों के आँसू पोंछा करता था। वे रह-रहकर बड़े स्नेह से मेरे हाथों को चूम लिया करते थे। उनके स्नेह का अंतिम उच्छ्वास देखकर मेरा हृदय उमड़ आता था। उनके पवित्र वात्सल्य की मंदाकिनी आज भी मेरे हृदय में उमड़कर आँखों की राह प्रवाहित होती हैं।”
इतना कहते-कहते उनकी आँखें भर आयीं। मेरी आँखों में भी आँसू छलछला उठे। मैंने अधीर होकर पूछा, “आप संन्यासी क्यों हुए?”
बोले, “वही तो कह रहा हूँ। मेरे पिता जिस दिन मरने लगे, उस दिन वे पूर्ण चैतन्य थे। वे अपने सामने की दीवार में टँगे हुए श्रीराधाकृष्ण के चितचोर चित्र को देख रहे थे। इतने में, देखते ही देखते, उनकी आँखें उलट गयीं। घर में हाहाकार मच गया। मेरा बना-बनाया संसार बिगड़ गया।
“माता ने मेरा मुख देखकर धैर्य धारण किया। वह मुझे अपनी गोद में लेकर अपने दुःखों को भूल गयी!
“मेरी पत्नी ने दिखावे के आँसू ढालकर कहा, ‘आप शोक करके अपने शरीर को मत गलाइए।’
“बस, वहीं से मेरा माथा ठनका।
“माता ने अपने स्नेहांचल से जब मेरे आँसुओं को पोंछा और मेरी ठुड्डी पकड़कर कहा ‘मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ, नहीं तो मुझे जीना नहीं चाहिए’ तब भी अंदर से मेरे हृदय में कोई ठोकरें मार गया। किंतु उस ठोकर से मोह का घड़ा न फूट सका।
“पहले भी जब चाचाजी मेरे पिता की रोगशय्या के पास बैठकर धीरे-धीरे उनसे रुपये-पैसे और लेन-देन की बातें पूछते थे, तब मैं पिताजी को बड़े कष्ट से उत्तर दे सकने में भी असमर्थ देखकर अशांत हो उठता था। किंतु हृदय की वह घोर अशांति भी मोह-निद्रा को भंग न कर सकी।”
मैंने कहा, “तो क्या आप अपने चाचा के दुर्व्यवहारों से ऊबकर घर से भाग निकले?”
बोले, “बीच ही में मत छेड़ा करों। मैं जो कुछ कहता जाता हूँ, उसे शांत भाव से सुनते चलो। जब मेरे पिता की अर्थी श्मशान में पहुँची, तब उनका शव चिता पर रखकर मुझे अग्नि-संस्कार करना पड़ा। हृदय को वज्र बनाकर मैंने वह भी कर डाला। देखते ही देखते चिताग्नि धधक उठी।
“तब तक मेरे ताऊ ने चिल्लाकर कहा ‘उफ! कमर का धागा तो तोड़ा ही नहीं गया। उसी में तिजोरी की कुंजी भी रह गई है। हाय! सर्वनाश हो गया!”
“बड़े चाचा का चिल्लाना था कि छोटे चाचा ने अर्थी के बाँस से सजायी हुई चिता बिखेर दी। मेरे पिता का अर्द्धनग्न शरीर चिता से कुछ खिसक पड़ा। कमर का धागा जल गया था। कुंजी आग में गिरकर लाल हो गयी थी। उसे झट बाहर निकालकर छोटे चाचा ने धूल में ढँक दिया।
“वही कुंजी! वही कुंजी!! वहीं कुंजी मेरे अज्ञान का ताला खोलने में समर्थ हुई। वहीं मैंने इस संसार का असली रूप देखा। वहीं मेरे तीसरी आँख खुली। वहीं मेरे जीवन की ज्योति का विकास हुआ।”
इतना कहते-कहते संन्यासी बाबा ध्यानस्थ हो गये; और मैं एक अपूर्व किंतु तीव्र चिंता-स्रोत में डूब गया।
(यह रचना 1919 में लिखी गयी। 1923 में ‘मारवाड़ी अग्रवाल’ में प्रकाशित हुई।)