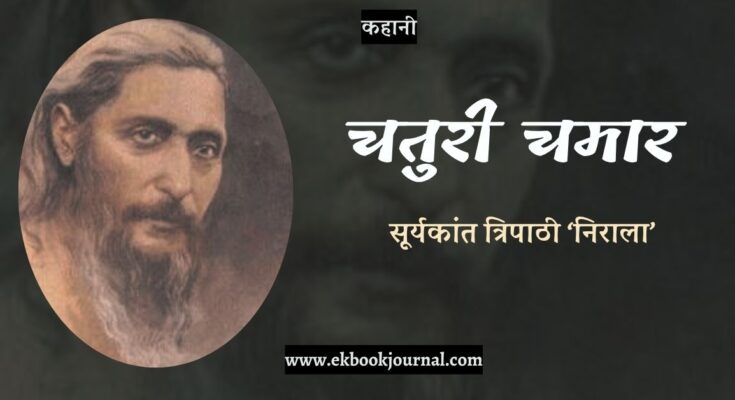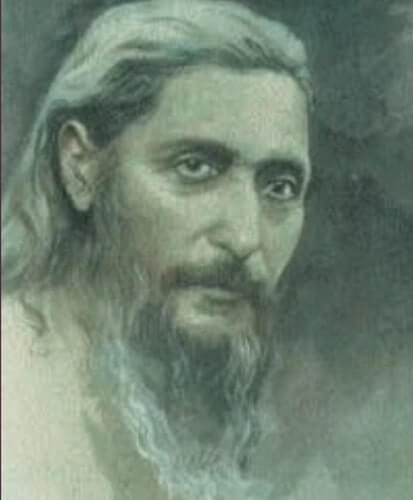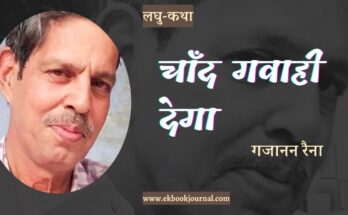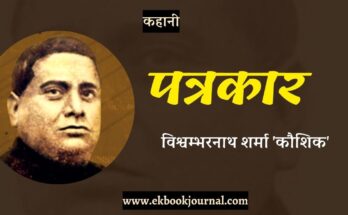चतुरी चमार डाकखाना चमियानी मौजा गढ़कला, उन्नाव का एक कदीमी बाशिंदा है। मेरे नहीं, मेरे पिताजी के बल्कि उनके पूर्वजों के भी मकान के पिछवाड़े कुछ फासले पर, जहाँ से होकर कई और मकानों के नीचे और ऊपरवाले पनालों का, बरसात और दिन-रात का शुद्धाशुद्ध जल बहता है। ढाल से कुछ ऊँचे एक बगल चतुरी चमार का पुश्तैनी मकान है। मेरी इच्छा होती है, चतुरी के लिए गौरवे बहुवचनम् लिखूँ, क्योंकि साधारण लोगों के जीवनचरित या ऐसे ही कुछ लिखने के लिए सुप्रसिद्ध सम्पादक पं. बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा दिया हुआ आचार्य द्विवेदीजी का प्रोत्साहन पढ़कर मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ गयी है, पर एक अड़चन है, गाँव के रिश्ते में चतुरी मेरा भतीजा लगता है। दूसरों के लिए वह श्रद्धेय अवश्य है, क्योंकि अपने उपानह-साहित्य में आजकल के अधिकांश साहित्यिकों की तरह अपरिवर्तनवादी है। वैसे ही देहात में दूर-दूर तक उसके मजबूत जूतों की तारीफ है। पासी हफ्ते में तीन दिन हिरन, चौगड़े और बनैले सुअर खदेड़कर फाँसते हैं। किसान अरहर की ठूँठियों पर ढोर भगाते हुए दौड़ाते हैं—कँटीली झाड़ियों को दबाकर चले जाते हैं। छोकड़े बेल, बबूल, करील और बेर के काँटों से भरे रुँधवाये बागों से सरपट भागते हैं, लोग जेंगरे पर मड़नी करते हैं, द्वारिका नाई न्योता बाँटता हुआ दो साल में दो हजार कोस से ज्यादा चलता है। चतुरी के जूते अपरिवर्तनवाद के चुस्त रूपक जैसे टस-से-मस नहीं होते। यह जरूर है कि चतुरी के जूते जिला बाँदा के जूतों से वजन में हल्के बैठते हैं; सम्भव है, चित्रकूट के इर्द-गिर्द होने के कारण वहाँ के चर्मकार भाइयों पर रामजी की तपस्या का प्रभाव पड़ा हो, इसलिए उनका साहित्य ज्यादा ठास हुआ; चतुरी वगैरह लखनऊ के नजदीक होने के कारण नवाबों के साये में आए हों।
उन दिनों मैं गाँव में रहता था। घर बगल में होने के कारण बैठे हुए ही मालूम कर लिया कि चतुरी चतुर्वेदी आदिकों से संत-साहित्य का अधिक मर्मज्ञ है। केवल चिट्ठी लिखने का ज्ञान न होने के कारण एक क्रिय होकर भी भिन्न फल है—वे पत्र और पुस्तकों के सम्पादक हैं, यह जूतों का। एक रोज मैंने चतुरी आदि के लिए चरस मँगवाकर अपने ही दरवाजे बैठक लगवायी। चतुरी उम्र में मेरे चाचाजी से कुछ छोटा होगा, कई घरों के लड़के-बच्चे समेत ‘चरस-रसिक रघुपति-पद-नेहू’ लोध आदि के सहयोग से मजीरेदार डफलियाँ लेकर वह रात आठ बजे आकर डट गया। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, पल्टूदास आदि ज्ञात-अज्ञात अनेकानेक संतों के भजन होने लगे। पहले मैं निर्गुण शब्द का केवल अर्थ लिया करता था; लोगों को ‘निर्गुण पद है’ कहकर संगीत की प्रशंसा करते हुए सुनकर हँसता था; अब गम्भीर हो जाया करता हूँ—जैसे उम्र की बाढ़ के साथ अक्ल बढ़ती है! मैं मचिया पर बैठकर भजन सुनने लगा।
चतुरी आचार्य-कंठ से लोगों को भूले पदों की याद दिला दिया करता। मुझे मालूम हुआ, चतुरी कबीर-पदावली का विशेषज्ञ है। मुझसे उसने कहा, “काका, ये निर्गुण-पद बड़े-बड़े विद्वान् नहीं समझते।” फिर शायद मुझे भी उन्हीं विद्वानों की कोटि में शुमार कर बोला, “इस पद का मतलब?”
मैंने उतरे गले से बात काटकर उभड़ते हुए कहा, “चतुरी, आज गा लो, कल सुबह आकर मतलब समझाना। मतलब से गाने की तलब चली जाएगी।”
चतुरी खखारकर गम्भीर हो गया। फिर उसी तरह डिक्टेट करता रहा। बीच-बीच में ओजस्विता लाने के लिए चरस की पुट चलती रही। गाने में मुझे बड़ा आनंद आया। ताल पर तालियाँ देकर मैंने भी सहयोग किया। वे लोग ऊँचे दरजे के उन गीतों का मतलब समझते थे, उनकी नीचता पर यह एक आश्चर्य मेरे साथ रहा। बहुत से गाने आलंकारिक थे। वे उनका भी मतलब समझते थे।
रात तक मैं बैठा रहा। मुझे मालूम न था कि ‘भगत’ कराने के अर्थ रातभर गँवाने से हैं। तब तक आधी चरस भी खत्म न हुई थी। नींद ने जोर मारा। मैंने चतुरी से चलने की आज्ञा माँगी। चरस की ओर देखते हुए उसने कहा, “काका, फिर कैसे काम बनेगा?”
मैंने कहा, “चतुरी, तुम्हारी काकी तो भगवान् के यहाँ चली गयी, जानते ही हो, भोजन अपने हाथ पकाना पड़ता है, कोई दूसरा मदद के लिए है नहीं, जरा आराम न करेंगे तो कल उठ न पाएँगे।”
चतुरी नाराज होकर बोला, “तुम ब्याह करते ही नहीं, नहीं तो तेरह काकी आ जाएँ, हाँ वैसी तो…”
मैंने कहा, “चतुरी, भगवान् की इच्छा।”
दुःखी हृदय से सहानुभूति दिखलाते हुए चतुरी ने कहा, “काकी बहुत पढ़ी-लिखी थीं। मैंने हसार को कई चिट्ठियाँ उनसे लिखवायी हैं।” फिर चलती हुई चिलम में दम लगाकर धुआँ पीकर, सिर नीचे की ओर जोर से दबाकर नाक से धुवाँ निकालकर बैठे गले से बोला, “काकी रोटी भी करती थीं, बरतन भी मलती थीं और रामायण भी पढ़ती थीं। बड़ा अच्छा गाती थीं काका, तुम वैसा नहीं गाते। बुढ़ऊ बाबा, (मेरे चाचा) दरवाजे बैठते थे—भीतर काकी रामायण पढ़ती थीं। गजलें और न जाने क्या-क्या टिल्लाना गाती थीं—क्यों काका?”
मैंने कहा, “हूँ! तुम लोग चतुरी गाओ, मैं दरवाजा बंद करके सुनता हूँ।”
जगने तक भगत होती रही। फिर कब बंद हुई, मालूम नहीं। जब आँख खुली तब काफी दिन चढ़ आया था। मुँह धोकर दरवाजा खोला, चतुरी बैठा एकटक दरवाजे की ओर देख रहा था। कबीर पदावली का अर्थ उससे किसी ने नहीं सुना। मैंने सुबह सुनने के लिए कहा था, वह आया हुआ है। मैंने कहा, “क्यों चतुरी, रात सोये नहीं?”
चतुरी सहज-गम्भीर मुद्रा से बोला, “सोकर जगे तो बड़ी देर हुई, बुलाने की वजह से आया हुआ हूँ।” जिनमें शक्ति होती है, अवैतनिक शिक्षक वही हो सकते हैं। मैंने कहा, “मैं तैयार हूँ, पहले तुम कबीर साहब की कोई उल्टबासी को सीधी करो।”
“कौन सुनाऊँ?” चतुरी ने कहा, “एक-से-एक बढ़कर हैं। मैं कबीरपंथी हूँ न काका, जहाँ गिरह लगती है, साहब आप खोल देते हैं।”
मैंने कहा, “तुम पहुँचे हुए हो, यह मुझे कल ही मालूम हो गया था।”
चतुरी आँख मूँदकर शायद साहब का ध्यान करने लगा, फिर सस्वर एक पद गुनगुनाकर गाने लगा, फिर एक-एक कड़ी गाकर अर्थ समझाने लगा। उसके अर्थ में अनर्थ पैदा करना आनंद खोना था। जब वह भाष्य पूरा कर चुका, जिस तरह के भाष्य से हिंदीवालों पर ‘कल्याण’ के निरामिष लेखों का प्रभाव पड़ सकता है, मैंने कहा, “चतुरी, तुम पढ़े-लिखे होते तो पाँच सौ की जगह पाते।”
खुश होकर चतुरी बोला, “काका, कहो तो अर्जुनवा (चतुरी का एक सत्रह साल का लड़का) को पढ़ाने के लिए भेज दिया करूँ तुम्हारे पास, पढ़ जाएगा, तुम्हारी विद्या ले लेगा, मैं भी अपनी दे दूँगा; तो कहो, भगवान् की इच्छा हो जाए तो कुछ हो जाए।”
मैंने कहा, “भेज दिया करो। दीया घर से लेकर आया करे। हमारे पास एक ही लालटेन है। बहुत नजदीक घिचेगा तो गाँववाले चौंकेंगे। आगे देखा जाएगा। लेकिन गुरु-दक्षिणा हम रोज लेंगे। घबराओ मत। सिर्फ बाजार से हमारे लिए गोश्त ले आना होगा और महीने में दो दिन चक्की से आटा पिसवा लाना होगा। इसकी मेहनत हम देंगे। बाजार तुम जाते ही हो।” चतुरी को इस सहयोग से बड़ी खुशी हुई। एक प्रसंग पर आने के विचार से मैंने कहा, “चतुरी, तुम्हारे जूते की बड़ी तारीफ है।”
खुश होकर चतुरी बोला, “हाँ काका, दो साल चलता है।” उसमें एक दर्द भी दबा था। दुखी होकर कहा, “काका, जिमीदार के सिपाही को एक जोड़ा हर साल देना पड़ता है। एक जोड़ा भगवता देता है। एक जोड़ा पंचमा। जब मेरा ही जोड़ा मजे में दो साल चलता है तब ज्यादा लेकर कोई चमड़े की बरबादी क्यों करे?” कहकर डबडबाई आँखों से देखता हुआ जुड़े हाथों सेवई सी बटने लगा।
मुझे सहानुभूति के साथ हँसी आ गयी। मगर हँसी को होंठों से बाहर न आने दिया। सँभलकर स्नेह से कहा, “चतुरी, इसका वाजिबउल-अर्ज में पता लगाना होगा। अगर तुम्हारा जूता देना अर्ज होगा तो इसी तरह पुश्त-दर-पुश्त तुम्हें जूते देते रहने पड़ेंगे।”
चतुरी सोचकर मुसकराया। बोला, “अब्दुल अर्ज में दर्ज होगा, क्यों काका?”
मैंने कहा, “देख लो, सिर्फ एक रुपया हक लगेगा।”
वक्त बहुत हो गया था। मुझे काम था। चतुरी को मैंने विदा किया। वह गम्भीर होकर सिर हिलाता हुआ चला गया। मैं उसके मनोविकार पढ़ने लगा, “वह एक ऐसे जाल में फँसा है, जिसे वह काटना चाहता है। भीतर से उसका पूरा जोर उभर रहा है। जिसमें बार-बार उलझकर रह जाता है।”
अर्जुन का आना जारी हो गया। उन दिनों बाहर मुझे कोई काम न था, देहात में रहना पड़ा। गोश्त आने लगा। समय-समय पर लोध, पासी, धोबी और चमारों का ब्रह्मभोज भी चलता रहा। घृतपक्व मसालेदार मांस की खुशबू से जिसकी भी लार टपकी, आप ही निमंत्रित होने को पूछा। इस तरह मेरा मकान साधारण जनों का अड्डा, बल्कि हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया। अर्जुन की पढ़ाई उत्तरोत्तर बढ़ चली। पहले-पहले जब दादा, मामा, काका, दीदी, नानी उसने सीखा तो हर्ष में उसके माँ-बाप सम्राट् पद पाये हुए को छापकर छलके। सब लोग आपस में कहने लगे, अब अर्जुनवा ‘दादा-दादी’ पढ़ गया। अर्जुन अपने बाप चतुरी को दादा और माँ को दीदी कहता था। दूसरे दिन उसके बड़े भाई ने मुझसे शिकायत की, कहा, ‘बाबा, अर्जुनवा और तो सब लिख-पढ़ लेता है, पर भैया नहीं लिखता।’ मैंने समझाया कि किताब में दादी-दादा से भैया की इज़्ज़त बहुत ज्यादा है; भैया तक पहुँचने में उसे दो महीने की देर होगी।
धीरे-धीरे आम पकने के दिन आए। अर्जुन अब दूसरी किताब समाप्त कर अपने खानदान में विशेष प्रतिष्ठित हो चला। कुछ नाजुक मिज़ाज भी हो गया। मोटा काम न होता था। आम खिलाने के विचार से मैं अपने चिरंजीव को लिवा लाने के लिए ससुराल चला गया। तब उसकी उम्र 9-10 साल की होगी। सोयम (तीसरी) या चहर्रुम (चौथी) में पढ़ता था। मेरे यहाँ उसके मनोरंजन की चीज न थी। कोई स्त्री भी न थी, जिसके प्यार से वह बहला रहता। पर दो-चार दिन के बाद मैंने देखा कि वह ऊबा नहीं, अर्जुन से उसकी गहरी दोस्ती हो गयी है। मैं अर्जुन के बाप के जैसा, वह भी अर्जुन का काका लगता था। यद्यपि उम्र में उससे पौने दो पट था, फिर भी पद और पढ़ाई में मेरे चिरंजीव बड़े थे, फिर यह ब्राह्मण के लड़के भी थे। अर्जुन को नयी और इतनी बड़ी उम्र में उतने छोटे से काका को श्रद्धा देते हुए प्रकृति के विरुद्ध दबना पड़ता था। इसका असर अर्जुन के स्वास्थ्य पर तीन-चार दिन में ही प्रत्यक्ष हो चला। तब मुझे कुछ मालूम न था। अर्जुन शिकायत न करता था। मैं देखता था। जब मैं डाकखाना या बाहर गाँव से लौटता हूँ, मेरे चिरंजीव अर्जुन के यहाँ होते हैं या घर ही पर उसे घेरकर पढ़ाते रहते हैं। चमारों के टोले में गोस्वामीजी के इस कथन को—‘मनहु मत्त गजगन निरखि-सिंह किसोरहिं चोप’, वह कई बार सार्थक करते देख पड़े। मैं ब्राह्मण-संस्कारों की सब बातों को समझ गया। पर उसे उपदेश क्या देता? चमार दबेंगे, ब्राह्मण दबाएँगे। दवा है, दोनों की जड़ें मार दी जाएँ, पर सहज-साध्य नहीं। सोचकर चुप हो गया।
मैं अर्जुन को पढ़ाता था तो स्नेह देकर उसे अपनी ही तरह का एक आदमी समझकर, उसके उच्चारण की त्रुटियों को पार करता हुआ। उसकी कमज़ोरियों की दरारें भविष्य में भर जाएँगी, ऐसा विचार रखता था। इसलिए उसमें कहाँ-कहाँ प्रमाद है, यह मुझे याद भी न था। पर मेरे चिरंजीव ने चार ही दिन में अर्जुन की सारी कमज़ोरियों का पता लगा लिया, और समय-असमय उसे घर बुलाकर (मेरी गैर-हाज़िरी में) उन्हीं कमज़ोरियों के रास्ते उसकी जीभ को दौड़ाते हुए अपना मनोरंजन करने लगे, मुझे बाद में मालूम हुआ।
सोमवार मियाँगंज के बाज़ार का दिन था। गोश्त के पैसे मैंने चतुरी को दे दिए थे। डाकखाना तब मगरायर था। वहाँ से बाज़ार नजदीक है। मैं डाकखाने से निबंध भेजने के लिए टिकट लेकर टहलता हुआ बाजार गया। चतुरी जूते की दुकान लिये बैठा था। मैंने कहा, “कालिका (धोबी) भैया आए हुए हैं। चतुरी हमारा गोश्त उनके हाथ भेज देना। तुम बाज़ार उठने पर जाओगे, देर होगी।”
चतुरी ने कहा, “काका, एक बात है, अर्जुनवा तुमसे कहता डरता है, मैं घर आकर कहूँगा। बुरा न मानना लड़कों की बात का।”
“अच्छा,” कहकर मैंने बहुत कुछ सोच लिया। बकर-कसाई के सलाम का उत्तर देकर बादाम और ठंडई लेने के लिए बनियों की तरफ गया। बाजार में मुझे पहचाननेवाले न पहचाननेवालों को मेरी विशेषता से परिचित करा रहे थे—चारों ओर से आँखें उठी हुई थीं, ताज्जुब यह था कि अगर ऐसा आदमी है तो मांस खाना जैसा घृणित पाप क्यों करता है। मुझे क्षणमात्र में यह सब समझ लेने का काफी अभ्यास हो गया था। गुरुमुख ब्राह्मण आदि मेरे घड़े का पानी छोड़ चुके थे। गाँव तथा पड़ोस के लड़के अपने-अपने भक्तिमान पिता-पितामहों को समझा चुके थे कि बाबा मैं कहते हैं, मैं पानी-पाँड़े थोड़े ही हूँ, जो ऐरे-गैरे, नत्थू-खैरे सबको पानी पिलाता फिरूँ। इससे लोग नाराज हो गए थे। साहित्य की तरह समाज में भी दूर-दूर तक मेरी तारीफ फैल चुकी थी—विशेष रूप से जब एक दिन वलायत की रोटी-पार्टी की तारीफ करनेवाले एक देहाती स्वामीजी को मैंने कबाब खाकर काबुल में प्रचार करनेवाले रामचंद्रजी के वक्त के एक ऋषि की कथा सुनाई, और मुझसे सुनकर वहीं गाँव के बाह्मणों के सामने बीड़ी पीने के लिए प्रचार करके भी मुझे नीचा नहीं दिखा सके—उन दिनों भाग्यवश मिले हुए अपने आवारागर्द नौकर से बीड़ी लेकर, सबके सामने दीयासलाई लगाकर मैंने समझा दिया कि तुम्हारा इस जूठे धुएँ से बढ़कर मेरे पास दूसरा महत्त्व नहीं।
मैं इन आश्चर्य की आँखों के भीतर बादाम और ठंडई लेकर जरा रीढ़ सीधी करने को हुआ कि एक बुड्ढे पंडितजी एक देहाती भाई के साथ मेरी ओर बढ़ते नजर आए। मैंने सोचा, शायद कुछ उपदेश होगा। पंडितजी सारी शिकायत पीकर मधु-मुख हो, अपने प्रदर्शक से बोले, “आप ही हैं?”
उसने कहा, “हाँ, यही हैं।”
पंडितजी देखकर गद्गद हो गए। बोढ़ी उठाकर बोले, “ओहो हो! आप धन्य हैं।”
मैंने मन में कहा, ‘नहीं, मैं धन्य हूँ, मजाक करता है खूसट।’ पर गौर से उनका पग्गड़ और खौर देखकर कहा, “प्रणाम करता हूँ पंडितजी।”
पंडितजी मारे प्रेम के संज्ञा खो बैठे। मेरा प्रणाम मामूली प्रणाम नहीं, बड़े भाग्य से मिलता है। मैं खड़ा पंडितजी को देखता रहा। पंडितजी ने अपने देहाती साथी से पूछा, “आप बे-में सब पास हैं?”
उनका साथी अत्यंत गम्भीर होकर बोला, “हाँ, जिला में दूसरा नहीं है।”
होंठ काटकर मैंने कहा, “पंडितजी, रास्ते में दो नाले और एक नदी पड़ती है। भेड़िए लागन हैं। डंडा नहीं लाया। आज्ञा हो तो चलूँ—शाम हो रही है।”
पंडितजी स्नेह से देखने लगे। जो शिकायत उन्होंने सुनी थी। आँखों में उस पर संदेह था; दृष्टि कह रही थी, ‘यह वैसा नहीं, जरूर गोश्त न खाता होगा। बीड़ी न पी होगी। लोग पाजी हैं।’
प्रणाम करके, आशीर्वाद लेकर मैंने घर का रास्ता पकड़ा।
दरवाजे पर आकर रुक गया। भीतर बातचीत चल रही थी। प्रकाश कुछ-कुछ था। सूर्य डूब रहा था। मेरे पुत्र की आवाज आयी, “बोल रे बोल!” इस वीर रस का अर्थ मैं समझ गया। अर्जुन बोलता हुआ हार चुका था। पर चिरंजीव को रस मिलने के कारण बुलाते हुए हार न हुई थी। चूँकि बार-बार बोलना पड़ता था, इसलिए अर्जुन बोलने से ऊबकर चुप था। डाँटकर पूछा गया तो सिर्फ कहा, “क्या?”
“वही गुण बोल।”
अर्जुन ने कहा, “गुड़।”
बच्चे के अट्टहास से घर गूँज उठा। भरपेट हँसकर, स्थिर होकर फिर उसने आज्ञा की, “बोल गणेश।”
रोनी आवाज में अर्जुन ने कहा, “गड़ेश।”
खिलखिलाकर, हँसकर, चिरंजीव ने डाँटकर कहा, “गड़ास-गड़ास करता है, साफ नहीं कहना आता—क्यों रे, रोज दातौन करता है?”
अर्जुन अप्रतिभ होकर दबी आवाज में एक छोटी सी ‘हूँ’ करके, सिर झुकाकर रह गया। मैं दरवाजा धीरे से ढकेलकर भीतर खम्भे की आड़ से देख रहा था। मेरे चिरंजीव उसे उसी तरह देख रहे थे जैसे गोरे कालों को देखते हैं। जरा देर चुप रहकर फिर आज्ञा की, “बोल वर्ण।”
अर्जुन की जान आ पड़ी। मुझे हँसी भी आयी, गुस्सा भी लगा। निश्चय हुआ, अब अर्जुन से विद्या का धनुष नहीं उठने का। अर्जुन वर्ण के उच्चारण में विवर्ण हो रहा था। तरह-तरह से मुँह बनाने का आनंद लेकर चिरंजीव ने फिर डाँटा, “बोलता है या लगाऊँ झापड़। नहा लूँगा, गरमी तो है।”
मैंने सोचा, अब प्रकट होना चाहिए। मुझे देखकर अर्जुन खड़ा हो गया और आँखें मल-मलकर रोने लगा। मैंने पुत्र-रत्न से कहा, “कान पकड़कर उठो-बैठो दस दफे।”
उसने नजर बदलकर कहा, “मेरा कुसूर कुछ नहीं और मैं यों ही कान पकड़कर उठूँ-बैठूँ?”
मैंने कहा, “तुम इससे गुस्ताखी कर रहे थे।”
उसने कहा, “तो आपने भी की होगी। इससे ‘गुण’ कहला दीजिए। आपने पढ़ाया तो है, इसकी किताब में लिखा है।”
मैंने कहा, “तुम हँसते क्यों थे?”
उसने कहा, “क्या मैं जान-बूझकर हँसता था?”
मैंने कहा, “अब आज से तुम इससे बोल न सकोगे।”
लड़के ने जबाव दिया, “मुझे मामा के यहाँ छोड़ आइए। यहाँ डाल के आम खट्टे होते हैं, थोपी होती है, मुँह फदक जाता है, वहाँ पाल के आम आते हैं।”
चिरंजीव को नाई के साथ भेजकर मैंने अर्जुन और चतुरी को सांत्वना दी।
कुछ महीने और मुझे गाँव में रहना पड़ा। अर्जुन कुछ पढ़ गया। शहरों की हवा मैंने बहुत दिनों से न खायी थी—कलकत्ता, बनारस, प्रयाग आदि का सफर करते हुए लखनऊ में डेरा डाला—स्वीकृत किताबें छपवाने के विचार से। कुछ काम लखनऊ में और मिल गया। अमीनाबाद होटल में एक कमरा लेकर निश्चिंत चित्त से साहित्य साधना करने लगा।
इन्हीं दिनों देश में आंदोलन जोरों का चला—यही, जो चतुरी आदिकों के कारण फिस्स हो गया है। होटल में रहकर, देहात से आनेवाले शहरी युवक मित्रों से सुना करता था, गढ़ाकोला में भी आंदोलन जोरों पर है, छह-सात सौ तक का जो किसान लोग इस्तीफा देकर छोड़ चुके हैं, वह जमीन अभी तक नहीं उठी। किसान रोज इकट्ठा होकर झंडा गीत गाया करते हैं। सालभर बाद जब आंदोलन में प्रतिक्रिया हुई; जमींदारों ने दावा करना और रियाया को बिना किसी रियायत के दबाना शुरू किया, तब गाँव के नेता मेरे पास मदद के लिए आए, बोले, “गाँव में चलकर लिखो। तुम रहोगे तो मार न पड़ेगी, लोगों को हिम्मत रहेगी। अब सख्ती हो रही है।”
मैंने कहा, “मैं कुछ पुलिस तो हूँ नहीं, जो तुम्हारी रक्षा करूँगा, फिर मार खाकर चुपचाप रहनेवाला धैर्य मुझमें बहुत थोड़ा है। कहीं ऐसा न हो कि शक्ति का दुरुपयोग हो।”
गाँव के नेता ने कहा, “तुम्हें कुछ करना तो है नहीं, बस बैठे रहना है।”
मैं गया।
मेरे गाँव की कांग्रेस ऐसी थी कि जिले के साथ उसका कोई तअल्लुक न था—किसी खाते में वहाँ के लोगों के नाम दर्ज न थे। पर काम में पुरवा डिवीजन में उससे आगे दूसरा गाँव न था। मेरे जाने के बाद पता नहीं कितनी दरख्वास्तें तो जमींदार साहब ने इधर-उधर लिखीं।
कच्चे रंगों से रंगा तिरंगा झंडा महावीर स्वामी के सामने एक बड़े बाँस में गड़ा, बारिश से घुलकर धवल हो रहा था। इन दिनों मुकदमेबाजी और तहकीकात जोरों से चल रही थी। कुछ किसानों पर एक साल के हरी-भूसे को तीन साल का बाकी बनाकर, जमींदार साहब ने दावे दायर किए थे, जो अपनी क्षुद्रता के कारण जमींदार ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट के पास आकर किसानों की दृष्टि में और भयानक हो रहे थे। एक दिन दरख्वास्तों के फलस्वरूप शायद दरोगाजी तहकीकात करने आए। मैं मगरायर डाक देखने जा रहा था। बाहर निकला तो लोगों ने कहा, “दारोगाजी आए हैं, अभी रहो।”
आगे दरोगाजी भी मिल गए। जमींदार साहब ने मेरी तरफ दिखाकर अंग्रेजी में धीरे से कुछ कहा। तब मैं कुछ दूर था, सुना नहीं। गाँववाले समझे नहीं, दरोगाजी झंडे की तरफ जा रहे थे। जमींदार शायद उखड़वा देने के इरादे से लिये जा रहे थे।
महावीरजी के अहाते में झंडा देखकर दरोगाजी कुछ सोचने लगे, बोले, “यह तो मंदिर का झंडा है।” देखा, उसमें कोई रंग न दीख पड़ा। जमींदार साहब को गौर से देखते हुए लौटकर डेरे की तरफ चले। जमींदार साहब ने बहुत समझाया कि यह बारिश से धुलकर सफेद हो गया है। लेकिन है यह कांग्रेस का झंडा। पर दरोगाजी बुद्धिमान थे। महावीरजी के अहाते में सफेद झंडे को उखड़वाकर वीरता प्रदर्शित करने की आज्ञा न दी। गाँव में कांग्रेस है, इसका पता न सब-डिवीजन में लगा, न जिले में; थानेदार साहब करें क्या?
उन दिनों मुझे उन्निद्र रोग था। इसलिए सिर के बाल साफ थे। मैंने सोचा कि वेश का अभाव है तो भाषा को प्रभावशाली करना चाहिए; नहीं तो थानेदार साहब पर अच्छी छाप न पड़ेगी। वहाँ तो महावीर स्वामी की कृपा रही, यहाँ अपनी ही सरस्वती का सहारा है। मैं ठेठ देहाती हो रहा था। थानेदार साहब ने मुझसे पूछा, “आप कांग्रेस में हैं?”
मैंने सोचा, ‘इस समय राष्ट्रभाषा से राजभाषा का बढ़कर महत्त्व होगा।’ कहा, “मैं तो विश्व सभा का सदस्य हूँ।”
इस सभा का नाम भी थानेदार साहब ने न सुना था। पूछा, “यह कौन सी सभा है?”
उनके जिज्ञासा भाव पर गम्भीर होकर, नोबल पुरस्कार पाए हुए कुछ लोगों के नाम गिनाकर मैंने कहा, “ये सब उसी सभा के सदस्य हैं।”
थानेदार साहब क्या समझे; वह जानें। मुझसे पूछा, “इस गाँव में कांग्रेस है?”
मैंने सोचा, ‘युधिष्ठिर की तरह सत्य की रक्षा करूँ तो असत्य-भाषण का पाप न लगेगा।’ कहा, “कहाँ इस गाँव के लोग तो कांग्रेस का मतलब भी नहीं जानते।” इतना कहके मैंने सोचा, ‘अब ज्यादा बातचीत ठीक न होगी।’ उठकर खड़ा हो गया और थानेदार साहब से कहा, “अच्छा, मैं चलता हूँ, जरा डाकखाने में काम है। चिट्ठीरसा हफ्ते में दो ही दिन गश्त पर आता है। मेरी जरूरी चिट्ठियाँ होती हैं और रजिस्ट्री, अखबार, मासिक पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं, फिर उस गाँव में हम लोगों की लाइब्रेरी भी है, जाना पड़ता है।”
थानेदार साहब ने पूछा, “कांग्रेस की चिट्ठियाँ आती हैं।”
मैंने कहा, “नहीं मेरी अपनी।” मैं चला आया।
थानेदार साहब जमींदार साहब से शायद नाराज होकर गए।
इससे तो बचाव हुआ, पर मुकदमा चलता रहा। जमींदार ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट ने, जिनके एक रिश्तेदार जमींदार की तरफ से वकील थे, किसानों पर जमींदार को डिग्री दे दी। बाद में चतुरी वगैरह की बारी आयी। दावे दायर हो गए, अब तक जो सम्मिलित धन मुकदमों में लग रहा था, सब खर्च हो गया। पहले की डिग्री में कुछ लोगों के बैल वगैरह नीलाम कर लिये गए। लोग घबरा गए। चतुरी को मदद की आशा न रही। गाँववालों ने चतुरी आदि के लिए दोबारा चंदा न लगाया।
चतुरी सूखकर मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। मैंने कहा, “चतुरी, मैं शक्ति भर तुम्हारी मदद करूँगा।”
“तुम कहाँ तक मदद करोगे, काका?” चतुरी जैसे कुएँ में डूबता हुआ उभरा।
“तो तुम्हारा क्या इरादा है?” उसे देखते हुए मैंने पूछा।
“मुकदमा लड़ूँगा। पर गाँववाले डर गए हैं, गवाही न देंगे।” दिल से बैठा हुआ चतुरी बोला। उस परिस्थिति पर मुझे भी निराशा हुई। उसी स्वर से मैंने पूछा, “फिर चतुरी?”
चतुरी बोला, “फिर छिदनी-पिरकिया आदि मालिक ही ले लें।”
मैंने गाँव में कुछ पक्के गवाह ठीक कर दिए। सत्तू बाँधकर, रेल छोड़कर पैदल दस कोस उन्नाव चलकर, दूसरी पेशी के बाद पैदल ही लौटकर हँसता हुआ चतुरी बोला, “काका, जूता और पुर वाली बात अब्दुल-अर्ज मे दर्ज नहीं है।”
समाप्त