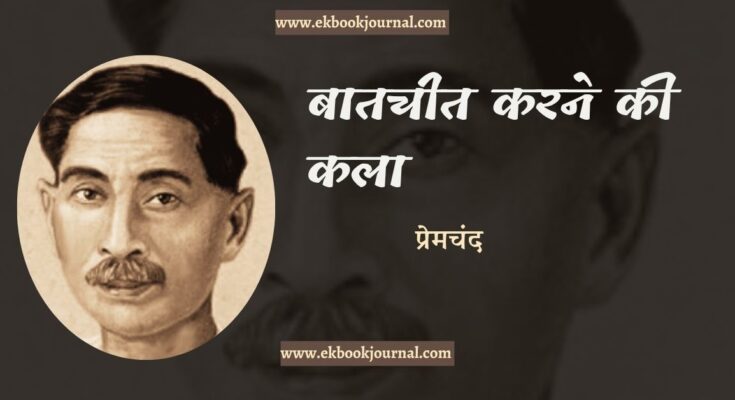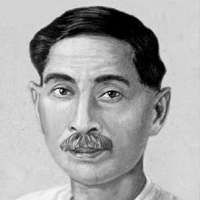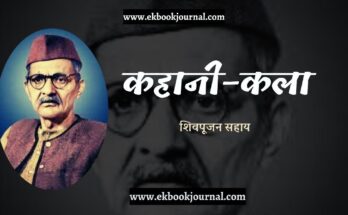बातचीत करना उतना आसान नहीं है, जितना हम समझते हैं। यों मामूली सवाल जवाब तो सभी कर लेते हैं, अपना दु:ख सभी रो लेते हैं, उसी तरह, जैसे सभी थोड़ा-बहुत गाकर अपना मन प्रसन्न कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह गाने की कला कुछ और है और उसे सीखने की जरूरत है, उसी तरह बातचीत करने की भी एक कला है, जो कुछ लोगों में तो ईश्वरदत्त होती है और कुछ लोगों को अभ्यास से आती है और जो आज अज्ञात कारणों से लुप्त होती जा रही है। आज दो चार हजार सुशिक्षित आदमियों में एक दो ही ऐसे निकलेंगे, जो अपने संभाषण से किसी समाज या मंडली का मनोरंजन कर सकते हों, अपनी लियाकत का सिक्का जमा सकते हों या अपने पक्ष का समर्थन कर सकते हों। और विचित्र बात यह है कि पढ़े-लिखे और विद्वान् लोग इस कला से जितने शून्य देखे जाते हैं, उतने अशिक्षित और ग्रामीण लोग नहीं।
किसी गाड़ी में दो पढ़े-लिखे सज्जन हजार-दो हजार मील की यात्रा साथ करेंगे, पर एक-दूसरे से सलाम-कलाम भी न करेंगे। एक अपना अखबार पढ़ता रहेगा, दूसरा अपने उपन्यास में डूबा रहेगा। इससे उल्टे दो ग्रामीण ज्योंही गाड़ी में बैठे कि उनमें चिलमबाजी शुरू हो जाती है, फिर खेतीबाड़ी का जिक्र छिड़ जाता है, फिर मामले-मुकदमे की चर्चा होने लगती है, जमींदार ने कैसे उसे बेदखल किया या साहुकार ने कैसे सूद दर सूद लगाकर पचास के दो सौ पचास रुपये कर लिये और उसकी सारी जायदाद नीलाम करा ली। जब तक यात्रा समाप्त न होगी, उनकी जबान बंद न होगी। सम्भव है, वे गाना शुरू कर दें। चलते-चलते उनमें एक सद्भाव पैदा हो जाता है। यहाँ हमारे बाबू साहब अपनी जगह पर बैठे अपने मुसाफिर भाई को गहरी आलोचना की आँखों से देखकर रह जाते हैं। आप एक ग्रामीण के साथ लम्बी-से लम्बी यात्रा हँसते हुए कर सकते हैं, लेकिन बाबू साहब के साथ आप छोटी यात्रा करके ऊब भी जाते हैं। उस ग्रामीण के जीवन में कुछ रस है, कुछ उत्साह है। कुछ आशावादिता है, कुछ बालकों का-सा कुतूहल है, कुछ अपनी विपत्ति पर हँसने की सामर्थ्य है, लेकिन मिस्टर या बाबू साहब अपने आप में सिमटकर मानों सारी दुनिया से रूठ गए हैं। ऐसा क्यों होता हैं, समझ में नहीं आता।
लेकिन ग्रामीणों में भी यह कला तनज्जुल (अवनति, ह्रास) पर है। पुराने जमाने में नाई संभाषण-कला में जन्म ही से निपुण होता था, उसी तरह जैसे धोबी जन्म ही से कविता की कला में सिद्ध होता है। अलिफलैला में नाइयों द्वारा कहीं गयी कई कहानियाँ हैं और यह विशेषता कुछ ईरानी या अरबी हज्जामों ही में न थी, हमारे यहाँ भी नाई पक्का बातूनी होता था, बड़ा हाजिरजवाब, जिसका दिमाग लोकोक्तियों और चुटकुलों की खान होता था। गाँवों में नाऊ ठाकुरों को हजारों कथाएँ आज भी प्रचलित हैं, लेकिन नाइयों में भी अब उस कला का लोप होता जा रहा है। अब तो वह मुहर्रमी सूरत लिए आता है, चुपचाप बाल बनाता है, और पैसे लेकर चला जाता है। नाइयों में तो इस कला के मिटने का कारण देहातों को बदहाली और साधारण जनता की गरीबी हो सकती है। जिनके पास पैसे हैं, वे अब अपने हाथों अपनी दाढ़ी साफ कर लेते हैं, कहीं छठे महीने उन्हें बाल कटवाने के लिए नाई को जरूरत पड़ती है। और देहातों में किसान आप ही दाने को मुहताज है, नाई का पेट कहाँ से भरें। जब किसान के बखारों में अनाज और गायें-भैंसों के थनों में दूध भरा होता था , तब नाई ठाकुर मूँछों पर ताव देते थे और भरा हुआ पेट उबलते हुए झरने को तरह किलोलें करता था, आनंद बढ़ाने बाली भावनाएँ मन में उठती थीं और चुटकला के रूप में निकलती थीं। जहाँ किसान बाकी और ब्याज के भँवर में डूबता उतरता हो और उसके बच्चे भूख से बिलबिलाते हों, वहाँ हँसने हँसाने की किसे सूझती है। शिक्षित लोगों में जो रूखापन और उदासीनता आ गयी है, उसका कारण शायद आजकल की शिक्षा प्रणाली है। पहले साहित्य ही मुख्य पाठ्य विषय था। हम बड़े-बड़े कवियों की सूक्तियाँ याद कर लिया करते थे। सुभाषितों का एक खजाना हमारे दिमाग में जमा हो जाता था और कंठस्थ होने के कारण अवसर पड़ने पर हम संभाषण में उसका व्यवहार करते थे। अब बाल्यावस्था में जो किस्से-कहानियाँ या अन्य पाठ पढ़ाये जाते हैं, उनमें सुभाषितों का नाम भी नहीं होता। और जब ऊँची कक्षाओं में क्लासिक पढ़ने का समय आता है, तो उसके लिए पाठ्यक्रम में इतना कम समय होता है कि केवल उसका अर्थ समझ लेना ही काफी समझा जाता है। रटंत की किसे फुरसत है। अच्छे संभाषण के लिए अच्छी स्मरण-शक्ति का होना आवश्यक है, और यह शक्ति आजकल उपेक्षा की दृष्टि से देखी जाती है। बड़े-बड़े विद्वानों से कहिए कि शेक्सपियर की दो-चार सूक्तियाँ सुनाइए ना, वे केवल मुस्कराकर रह जाएँगे। गरीब को कुछ याद हो तब तो सुनाये। एक कारण यह भी है कि हमने जनता में मिलना-जुलना तर्क कर दिया है, जहाँ भावनाएँ अपने मौलिक और प्राकृतिक रूप में निवास करती हैं। जब तक आपको हजार पाँच सौ शेर और कवित्त या दोहे, सौ दो सौ चुटकुले, दो चार सौ सुभाषित और सूक्तियाँ याद न हों, आप मनोरंजक संभाषण नहीं कर सकते। किसी को स्पीच सुनने जाइए, अगर वह केवल फिलॉसफी बघार रहा है, या बड़ी ओजस्विनी भाषा में परिस्थितियों पर अपना मत प्रकट कर रहा है तो आप बहुत जल्द ऊब जाएँगे। लेकिन अगर वह बीच-बीच में अपने कथनों को विनोद-भरे चुटकुलों और मुहावरों से अलंकृत करता जाता है, तो आप अंत तक मुग्ध बैठे रहेंगे। एक लतीफे से सारे संभाषण में जान-सी पट जाती है। सैकड़ों दलीलें एक तरफ और एक चुस्त सुभाषित एक तरफ। वह प्रतिद्वंद्वी को निरुत्तर कर देता है, उसके जबाब में उसकी जबान नहीं खुलती। उसका पक्ष कितना ही प्रबल हो, पर सुभाषितों में कुछ ऐसा जादू होता है कि मानों वह एक फूँक से दलीलों को उड़ा देता है। मौलाना मुहम्मदअली मरहूम जिन दिनों अंग्रेजी ‘कामरेड’ नाम का साप्ताहिक-पत्र लिखा करते थे तो उनके लेखों का हरेक पैराग्राफ ग़ालिब के शेरों से अलंकृत होता था और इससे राजनीति के रूखे विषय में भी रस आ जाता था। उनके इस तरह के लेख लाजवाब होते थे और बड़ी रुचि से पढ़े जाते थे। मौलाना मुहम्मदअली को ग़ालिब का पूरा दीवान कंठ था और शेर को वह कुछ इस तरह चिपका दिया करते थे कि मालूम होता था ग़ालिब ने वह शेर इसी अवसर के लिए कहा हो। स्व. अकबर की व्यंगोक्तियाँ भी दंदाशिकन हैं, इतनी संजीव और चुलबुली कि अगर हम अपनी बातचीत में मौके पर उनका व्यवहार कर सकें, तो सुनने वालों को फड़का दे। कबीर और तुलसी, रहीम, गिरधर आदि की रचनाएँ सुभाषितों से भरी पड़ी है। मगर अंग्रेजी स्कूलों में हिंदी साहित्य एक गौण विषय है, और जिन लोगों ने इन महाकवियों को केवल स्कूलों में पढ़ा है, वे शायद ही उनकी सूक्तियाँ को याद रख सकते हो। लतीफों की कोई अच्छी पुस्तक हिंदी में हमारी नजर से नहीं गुजरी। बीरबल, अकबर और खुसरो के नाम से जो लतीफे प्रचलित हैं उनमें अधिकांश गंदे और कुरुचिपूर्ण हैं! अगर कोई सज्जन लतीफों को संग्रह कर सकें, तो साहित्य का उपकार करें। समाज में वार्ता-कुशल व्यक्ति का कितना सम्मान और प्रभाव होता है, यह लिखने की जरूरत नहीं। ऐसा आदमी किसी मंडली में पहुँच जाता है, तो तुंरत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और मंडली पर मानों उसका आधिपत्य हो जाता है। हाँ, मौका देखकर ही जबान खोलनी चाहिए और उसी विषय में बोलने का साहस करना चाहिए जिसका हमें कुछ अनुभव या ज्ञान है। मौन की बड़ी प्रशंसा की गयी है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम मौका आने पर भी मुँह बंद किए बैठे रहें। हाँ, अगर हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, तो मौन रहना ही उचित है। मौन से कम-से-कम हमारी मूर्खता का परदा तो ढका रहता है। हम तो कहते हैं, हमारे थोथेपन के लिए बड़ी हद तक हमारी अयोग्यता ही जिम्मेदार है। अगर हमारे स्टॉक में लोकोक्तियों और लतीफों का अभाव न हो, तो हम थोथे बैठे ही नहीं रह सकते। जिसे नाचना आता है, वह अवसर पड़ने पर बिना नाचे रह ही नहीं सकता। अगर उसे नाचने का अवसर मिले, तो वह मन में बहुत दु:खी होगा और भाव-भंगिमा से अपना असंतोष प्रकट करेगा। जो अच्छे वक्ता हैं, वे किसी सम्मेलन में चुप नहीं बैठ सकते। उनकी जीभ खुजलाने लगती है। और वे बार-बार स्लिप लिख-लिखकर सभापति से बोलने की अनुमति लेकर ही रहते हैं। जिन गरीबों को बोलने की शक्ति या अभ्यास नहीं है, वे तो बार-बार कहने पर भी मंच पर नहीं आते, मनाते रहते हैं कि यह बला मेरे सिर न आ जाएँ।
लगभग एक महीना हुआ हमारी मुलाकात एक ऐसे सज्जन से हुई, जिनकी वाचालता देखकर हम दंग रह गए। लतीफों और सुभाषितों का एक सोता था, जो उबलता चला आता था। ऐसा कोई विषय न था जिस पर उनकी अपनी एक स्वतंत्र राय न हो और जिसका समर्थन वह कायल कर देने वाले ढंग से न कर सकें । कई बार यह जानते हुए भी कि उनका कथन भ्रममूलक है, उनकी वाचालता से लाजवाब हो गये। अपने पक्ष में एक मार्मिक लतीफा कहकर वह कहकहा मारते थे और इसके साथ मैदान मार लेते थे। वह जानते थे, इस फैसले के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कितने लतीफे कहे, इस वक्त सब तो याद नहीं आते, लेकिन दो-चार याद हैं, उन्हें मैं पाठकों के मनोरंजन के लिए यहाँ देता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह अपने दिमाग को ऐसे लतीफों से जितना सशस्त्र कर सकें, कर लें। इससे वे अपने ही दु:खों पर नहीं, दूसरे के दु:खों पर भी प्रहार कर सकेंगे और अपने श्रद्धालुओं का दायरा फैला सकेंगे–
(1) दक्षिणी अफ्रीका में एक बार सरकारी कर्मचारी जन-गणना के सिलसिले में एक झोंपड़ी के सामने पहुँचा, जहाँ कई बच्चे खेल रहे थे। उसने आवाज दी, तो उसके जवाब में एक हबशिन बाहर निकल आयी। कागजों की खानापूरी करने के लिए कर्मचारी ने पूछा, “तुम्हारा शौहर क्या काम करता है?”
हबशिन ने जवाब दिया, “वह क्या करेगा। उसे मरे तो बीस साल हो चुके हैं।”
“तो यह बच्चे किसके हैं?”
“मेरे हैं।”
“लेकिन तुम तो कहती हो कि तुम्हारे शौहर को मरे बीस साल हो गए?”
“हाँ, वह मर गया है, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ।”
(2) एक तेली ने अपने बैल के गले में घंटी बाँध रक्खी थी। एक सज्जन ने पूछा, “क्यों साहजी, बैल की गर्दन में घंटी क्यों बाँध रक्खी है?”
तेली ने जवाब दिया, “इसलिए कि बैल चलता रहता है, तो घंटी बजती रहती है। मैं कोई दूसरा काम भी करता रहता हूँ, तो मुझे मालूम रहता है कि बैल चल रहा है, खड़ा नहीं हो गया।”
“लेकिन अगर बैल खड़ा होकर सिर हिलाता रहे?”
“महाशय, मेरा बैल इतना समझदार नहीं है?”
(3) एक हिसाबदाँ ने दरिया को गहराई का अनुपात निकालकर घर वालों से कहा, “पानी थोड़ा है, कोई डर नहीं, हम इसे पार कर लेंगे, लेकिन जब घर के सब लोग मध्य धारा में पहुँचते ही उसकी आँखों के सामने डूब गये, तो वह फिर किनारे पर पहुँचे और फिर अनुपात निकाला। वही जबाब निकाला जो पहले था, तो बोले, “अभी ज्यो का त्यों, कुवां डूबा क्यों?”
(4) एक अफीमची पिनक में राह में पड़ा हुआ था। एक फक्कड़ ने उसके सिर की पगड़ी उतार ली और उसकी जगह थोड़ी सी रुई रख दी।
अफीमची तब पिनक से जागा, तो पगड़ी सँभालने के लिए सिर की तरफ हाथ बढ़ाया। पगड़ी की जगह रुई उसके हाथ आयी तो बोला, “कमबख़्त, धुनकी गयी, काती गथी, बुनी गयी, पगड़ी बनी। इतना सब कुछ हो चुकने के बाद फिर रुई की रुई।”
(5) एक बार मि. हर्बर्ट स्पेंसर कहीं सैर करने जा रहे थे। आप इंगलैंड के बहुत बड़े फिलॉसफर हो गुजरे हैं। रास्ते में आपको एक सौ साल की बुढ़िया बैठी पड़ी। हर्बर्ट स्पेंसर को मजाक की सूझी, बोले, “मैडम, दुनिया में तुम्हारा कोई प्रेमी भी है?” बुढ़ियाया ने छूटते ही जवाब दिया, “बेटा, मेरे प्रेमी तो सब स्वर्ग सिधार गए, बस एक तुम जीते बचे हो।” फिलॉसफर साहब ऐसे झेंपे कि भागते ही बना।
(6) तुर्कों के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री असमत पाशा जब लोजान की कान्फ्रेंस में सेवरी की संधि को बदलवाने के लिए आये, तो आपका सामना लार्ड कर्जन से हुआ। लार्ड कर्जन की अकड़ तो मशहूर है। अपने इस घमंड में कि यह दुनिया के सबसे शक्ति-संपन्न साम्राज्य के प्रतिनिधि हैं, तुर्की प्रतिनिधियों पर रोब जमाने के लिए राष्ट्रवादी तुर्कों पर खूब हमले किये। लार्ड कर्जन का यह ढंग देख कर असमत पाशा ने ऐसा मुँह बना लिया, मानों लार्ड कर्जन बोल ही नहीं रहे हैं। जब लार्ड कर्जन डेढ-दो घंटे तक डीगें मार कर बैठ गये, तो गाजी असमत पाशा चौंककर उठ खड़े हुए और कान पर हाथ रखकर बोले, “क्या आप तुर्की के विषय में कुछ कह रहे हैं। मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। दूसरे विचारों में डूबा हुआ था।” लार्ड कर्जन पर घड़ों पानी पड़ गया।
(‘हंस’ पत्रिका के दिसम्बर 1934 अंक में प्रकाशित’)