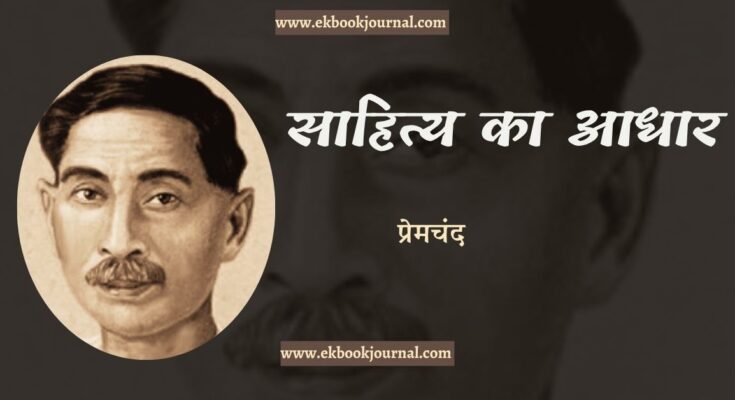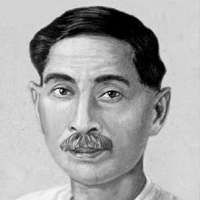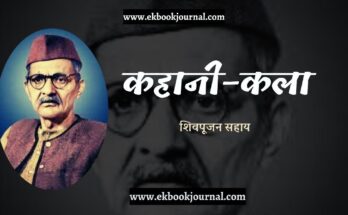साहित्य का सम्बंध बुद्धि से उतना नही जितना भावों से है। बुद्धि के लिए दर्शन है, विज्ञान है, नीति है। भावो के लिए कविता है, उपन्यास है, गद्यकाव्य है।
आलोचना भी साहित्य का एक अंग मानी जाती है, इसीलिए कि वह साहित्य को अपनी सीमा के अंदर रखने की व्यवस्था करती है। साहित्य में जब कोई ऐसी वस्तु सम्मिलित हो जाती है,जो उसके रस प्रवाह में बाधक होती है, तो वहीं साहित्य में दोष का प्रवेश हो जाता है। उसी तरह जैसे संगीत में कोई बेसुरी ध्वनि उसे दूषित कर देती है। बुद्धि और मनोभाव का भेद काल्पनिक ही समझना चाहिए। आत्मा में विचार, तुलना, निर्णय का अंश, बुद्धि और प्रेम, भक्ति, आनंद, कृतज्ञता आदि का अश भाव है। ईर्ष्या, दम्भ, द्वेष, मत्सर आदि मनोविकार हैं। साहित्य का इनसे इतना ही प्रयोजन है कि वह भावो को तीव्र और आनंदवर्द्धक बनाने के लिए इनकी सहायता लेता है, उसी तरह, जैसे कोई कारीगर श्वेत को और श्वेत बनाने के लिए श्याम की सहायता लेता है। हमारे सत्य भावों का प्रकाश ही आनंद है। असत्य भावो में तो दुःख का ही अनुभव होता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को असत्य भावो में भी आनंद का अनुभव हो। हिंसा करके, या किसी के धन का अपहरण करके या अपने स्वाथ के लिए किसी का अहित करके भी कुछ लोगो को आनंद प्राप्त होता है, लेकिन यह मन की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है। चोर को प्रकाश से अँधेरा कहीं अधिक प्रिय है। इससे प्रकाश की श्रेष्ठता में काई बाधा नही पड़ती। हमारा जैसा मानसिक सगठन है, उसमें असत्य भावों के प्रति घृणामय दया ही का उदय होता है। जिन भावों द्वारा हम अपने को दूसरो में मिला सकते है, वही सत्य भाव हैं, प्रेम हमें अन्य वस्तुओं से मिलाता है, अहंकार पृथक् करता है। जिसमें अहंकार की मात्रा अधिक है वह दूसरो से कैसे मिलेगा? अतएव प्रेम सत्य भाव है, अहंकार असत्य भाव है। प्रकृति से मेल रखने में ही जीवन है। जिसके प्रेम की परिधि जितनी ही विस्तृत है, उसका जीवन उतना ही महान है।
जब साहित्य की सृष्टि भावोत्कर्ष द्वारा होती है, तो यह अनिवार्य है कि उसका कोई आधार हो। हमारे अंतःकरण का सामंजस्य जब तक बाहर के पदार्थों या वस्तुओं या प्राणियों से न होगा, जागृति हो ही नहीं सकती। भक्ति करने के लिए कोई प्रत्यक्ष वस्तु चाहिए। दया करने के लिए भी किसी पात्र की आवश्यकता है। धैर्य और साहस के लिए भी किसी सहारे की जरूरत है। तात्पर्य यह है कि हमारे भावों को जगाने के लिए उनका बाहर की वस्तुओ में सामंजस्य होना चाहिए। अगर बाह्य प्रकृति का हमारे ऊपर कोई असर न पड़े, अगर हम किसी को पुत्र शोक में विलाप करते देखकर आँसू की चार बूँदें नहीं गिरा सकते, अगर हम किसी आनंदोत्सव में मिलकर आनंदित नहीं हो सकते, तो यह समझना चाहिए कि हम निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। उस दशा के लिए साहित्य का कोई मूल्य नहीं। साहित्यकार तो वही हो सकता है जो दुनिया के सुख-दुःख से सुखी या दुखी हो सके और दूसरो में सुख या दुःख पैदा कर सके। स्वयं दुःख अनुभव कर लेना काफी नहीं है। कलाकार में उसे प्रकट करने का सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन परिस्थितियाँ मनुष्य को भिन्न दिशाओ में डालती हैं। मनुष्य मात्र में भावों की समानता होते हुए भी परिस्थिातयों में भेद होता ही है। हमें तो मिठास से काम है, चाहे वह ऊख में मिले या खजूर में या चुकंदर में। अगर हम किसानों में रहते हैं या हमे उनके साथ रहने के अवसर मिले है, तो स्वभावतः हम उनके सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समझने लगते हैं और उससे उसी मात्रा में प्रभावित होते हैं जितनी हमारे भावों में गहराई है। इसी तरह अन्य परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। अगर इसका अर्थ यह लगाया जाय कि अमुक प्राणी किसानों का, या मजदूरों का या किसी आंदोलन का प्रोपागेंडा करता है, तो यह अन्याय है। साहित्य और प्रोपागेंडा में क्या अंतर है, इसे यहाँ प्रकट कर देना जरूरी मालूम होता है। प्रोपागेंडे में अगर आत्म-विज्ञापन न भी हो तो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने की वह उत्सुकता होती है जो साधनों की परवाह नहीं करती। साहित्य शीतल, मंद समीर है, जो सभी को शीतल और श्रानदित (प्रसन्न) करती है। प्रोपागेंडा आँधी है, जो आँखों में धूल झोंकती है, हरे-भरे वृक्षो को उखाड़-उखाड़ फेंकती है, और झोपड़े तथा महल दोनो को ही हिला देती है। वह रस-विहीन होने के कारण आनंद की वस्तु नहीं। लेकिन यदि कोई चतुर कलाकार उसमें सौंदर्य और रस भर सके, तो वह प्रोपागेंडा की चीज न होकर सद्साहित्य की वस्तु बन जाती है। ‘अंकल टॉम्स केबिन’ दास प्रथा के विरुद्ध प्रोपागेंडा है, लेकिन कैसा प्रोपागेंडा है? जिसका एक एक शब्द में रस भरा हुआ है। इसलिए वह प्रोपागेंडा की चीज नहीं रहा। बर्नार्ड शा के ड्रामे, वेल्स के उपन्यास, गाल्सवर्दी के ड्रामे और उपन्यास, डिकेंस, मेरी कारेली, रोमा रोला, टॉल्स्टाय, चेस्टरटन, दोस्तोवस्की, मैक्सिम गोर्की, सिंक्लेयर, कहाँ तक गिनाये। इन सभी की रचनाओं में प्रोपागेंडा और साहित्य का सम्मिश्रण है। जितना शुष्क विषय-प्रतिपादन है वह प्रोपागेंडा है, जितनी सौंदर्य की अनुभूति है, वह सच्चा साहित्य है। हम इसलिए किसी कलाकार से जवाब तलब नहीं कर सकते कि वह अमुक प्रसंग से ही क्यों अनुराग रखता है। यह उसकी रुचि या परिस्थितियो से पैदा हुई परवशता है। हमारे लिए तो उसकी परीक्षा की एक ही कसौटी है: वह हमे सत्य और सुंदर के समीप ले जाता है या नहीं? यदि ले जाता है तो वह साहित्य है, नहीं ले जाता तो प्रोपागेंडा या उससे भी निकृष्ट है।
हम अकसर किसी लेखक की आलोचना करते समय अपनी रुचि से पराभूत हो जाते हैं। ओह, इस लेखक की रचनाएँ कौड़ी काम की नहीं, यह तो प्रोपागेंडिस्ट है, यह जो कुछ लिखता है, किसी उद्देश्य से लिखता है, इसके यहाँ विचारो का दारिद्रय है। इसकी रचनाओं में स्वानुभूत दर्शन नही, इत्यादि। हमे किसी लेखक के विषय में अपनी राय रखने का अधिकार है, इसी तरह औरों को भी है, लेकिन सद्साहित्य की परख वही है जिसका हम उल्लेख कर आये हैं। उसके सिवा कोई दूसरी कसौटी हो ही नहीं सकती। लेखक का एक एक शब्द दर्शन में डूबा हो, एक एक वाक्य में विचार भरे हो, लेकिन उसे हम उस वक्त तक सद्साहित्य नहीं कह सकते, जब तक उसमें रस का स्रोत न बहता हो, उसमें भावों का उत्कर्ष न हो, वह हमे सत्य की ओर न ले जाता हो, अर्थात्… बाह्य प्रकृति से हमारा मेल न कराता हो। केवल विचार और दर्शन का आधार लेकर वह दर्शन का शुष्क ग्रंथ हो सकता है, सरस साहित्य नहीं हो सकता। जिस तरह किसी आंदोलन या किसी सामाजिक अत्याचार के पक्ष या विपक्ष में लिखा गया रसहीन साहित्य प्रोपागेंडा है, उसी तरह किसो तात्विक विचार या अनुभूत दर्शन से भरी हुई रचना भी प्रोपागेंडा है। साहित्य जहाँ रसों से पृथक् हुआ, वहीं वह साहित्य के पद से गिर जाता है और प्रोपागेंडा के क्षेत्र में जा पहुँचता है। ओस्कर वाइल्ड या शा आदि की रचनाएँ जहाँ तक विचार प्रधान हो, वहाँ तक रसहीन है। हम रामायण को इसलिए साहित्य नहीं समझते कि उसमें विचार या दर्शन भरा हुआ है, बल्कि इसलिए कि उसका एक एक अक्षर सौंदर्य के रस में डूबा हुआ है, इसलिए कि उसमें त्याग और प्रेम और बंधुत्व और मैत्री और साहस आदि मनोभावों की पूर्णता का रूप दिखाने वाले चरित्र हैं। हमारी आत्मा अपने अंदर जिस अपूर्णता का अनुभव करती है, उसकी पूर्णता को पाकर वह मानो अपने को पा जाती है और यही उसके आनंद की चरम सीमा है।
इसके साथ यह भी याद रखना चाहिए कि बहुधा एक लेखक की कलम से जो चीज प्रोपागेंडा होकर निकलती है, वही दूसरे लेखक की कलम से सद्साहित्य बन जाती है। बहुत कुछ लेखक के व्यक्तित्व पर मुनहसर है। हम जो कुछ लिखते है, यदि उसमें रहते भी हैं, तो हमारा शुष्क विचार भी अपने अंदर आत्म प्रकाश का संदेश रखता है और पाठक को उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। वह श्रद्धा जो हममें है, मानो अपना कुछ अंश हमारे लेखों में भी डाल देती है। एक ऐसा लेखक विश्व बंधुत्व की दुहाई देता हो, पर तुच्छ स्वार्थ के लिये लड़ने पर कमर कस लेता हो, कभी अपने ऊँचे आदर्श की सत्यता से हमें प्रभावित नहीं कर सकता। उसकी रचना में तो विश्व बंधुत्व की गंध आते ही हम ऊब जाते हैं, हमें उसमें कृत्रिमता की गंध आती है। और पाठक सब कुछ क्षमा कर सकता है, लेखक में बनावट या दिखावा या प्रशंसा की लालसा को क्षमा नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसे लेखक में कुछ श्रद्धा है, तो वह उसके दर्शन, विचार, उपदेश, शिक्षा, सभी असाहित्यिक प्रसंगो में सौंदर्य का आभास पाता है। अतएव बहुत कुछ लेखक के व्यक्तित्व पर निर्भर है। लेकिन हम लेखक से परिचित हो या न हों, अगर वह सौंदर्य की सृष्टि कर सकता है, तो हम उसकी रचना में आनंद प्राप्त करने से अपने को रोक नहीं सकते। साहित्य का आधार भावों का सौंदर्य है, इससे परे जो कुछ है वह साहित्य नहीं कहा जा सकता।
(प्रेमचंद द्वारा संपादित ‘जागरण‘ नामक साप्ताहिक पत्रिका में 12 अक्टूबर 1932 में प्रकाशित)