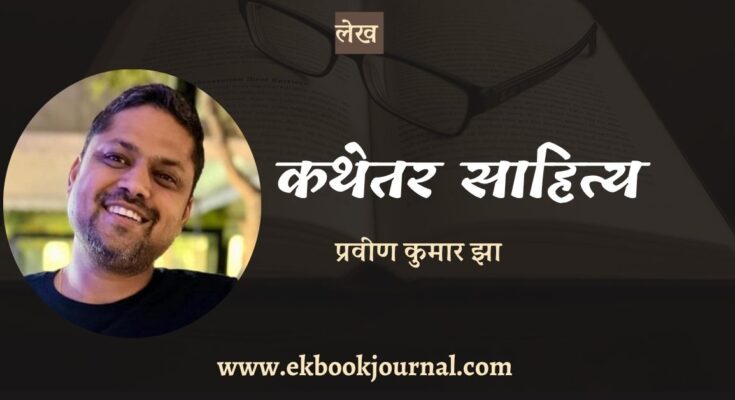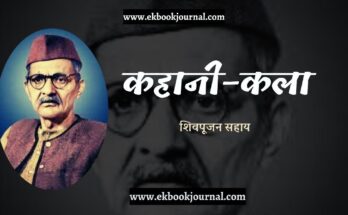लेखक प्रवीण कुमार झा ने साहिंद वेबसाइट में कथेतर विधा के ऊपर दो टिप्पणियाँ प्रकाशित की थीं। यह टिप्पणियाँ चूँकि एक दूसरे से सम्बंधित हैं तो हमने सोचा एक बुक जर्नल पर प्रकाशित करते समय इन्हें एक साथ ही रखा जाए। आप भी पढ़िए:
1
कथेतर विधा का लेखन ही वास्तव में कालजयी होता है
कथेतर विधाओं में लेखन सुलभ भी है और कठिन भी। वाकई कालजयी अगर पुस्तकाकार कुछ होता है, तो वह कथेतर ही अमूमन होता है। और वह भाषा के भेद से परे होता है। अब अगर किसी को हज़ार वर्ष पुराना इतिहास ढूँढना हो तो वह हज़ार वर्ष पुरानी किताब ही टटोलेगा। अगर यह पता करना हो कि वेस्ट-इंडीज़ जब पहली वर्ल्ड-कप जीती तो कैसे पिच-कंडीशन थे तो वह आज की पत्रिका में शायद न मिले। तो वह पत्रिका ढूँढी जाती है। उस वक्त के एक रूपए की खेल-पत्रिका भी आज बिक रही है, या ढूँढी जा रही है। गांधी के पुराने ‘इंडियन ओपिनियन’ अखबार रामचंद्र गुहा सरीखे लोग छान रहे है। कहानियों में ऐसा कम होता है, हालाँकि आदम साहित्य पढ़ा जाता है अगर उस पर कहानी बुननी हो या ऐतिहासिक फ़िक्शन लिखना हो। लेकिन ऐतिहासिक फ़िक्शन के लिए भी इतिहास की किताब ही खुलेगी।
कथेतर लिखने का सबसे बड़ा फायदा लेखक को यही है कि वह एक किताब के लिए सैकड़ों किताब पढ़ जाता है। और सिर्फ पढ़ता ही नहीं, किताबों के सागर में गोते लगाकर ढूँढ कर पढ़ता है। अब अशोक कुमार पाण्डेय जी की कश्मीरनामा में ही लगभग पाँच सौ किताब/लेख के संदर्भ होंगे। लेखक ने कल्हण राजतरंगिणी से लेकर राहुल पंडिता की किताब (अवर मून हैस ब्लड क्लॉट्स/मेरी माँ के बीस कमरे) तक पढ़ डाली। और इन सबको पढ़ कर सजाया, अपने निष्कर्ष बनाए, प्रश्न रखे, उत्तर ढूँढे, तब जाकर बनी किताब।
जब किताब खत्म होने को हुई, तब लगा कि पाँच सौ पृष्ठ लिख डाले और कश्मीरी पंडितों की बात तो अधूरी रह गयी। फिर एक नयी किताब बननी शुरू हुई, कई साक्षात्कार शुरू हुए, और अगले पुस्तक मेला तक एक उस मुद्दे पर भी किताब (कश्मीर और कश्मीरी पंडित) आ जाएगी। और फिर कुछ बात रह जाएगी।
रामचंद्र गुहा तो मात्र गांधी पर एक के बाद एक रचते जा रहे हैं। और अब जब भी, जहाँ भी (पूरे विश्व में) गांधी पर चर्चा होगी, गुहा मंच पर मिल जाएँगे।
यह स्थिति कथाकारों की कम होती है। और यह बात बता दूँ कि इन दोनों में कोई इतिहासकार नहीं। एक विधा के साहित्यकार ही हैं।
दिनकर भी ‘संस्कृति के चार अध्याय’ से कालजयी बने, जब एक कवि को इतिहासकार बनना पड़ा।
2
कथेतर पर आगे की बात
नॉन-फ़िक्शन (कथेतर) पर आगे की बात करते हुए। यह कुछ हिन्दी या अन्य भाषा प्रकाशकों की दुविधा जरूर है कि यह पढ़ेगा कौन, खरीदेगा कौन? इस सम्बंध में नॉर्वे के राष्ट्रीय पुस्तकालय का रिकॉर्ड छाना तो लगभग 65 % किताबें कथेतर ही संकलित हैं, और सबसे अधिक पढ़ी गयी। यह आँकड़ा चौंकाता है, लेकिन ध्यान देने पर ठीक नजर आता है।
दूसरी बात कि यह पुस्तकें कथाओं के दस गुणे दाम पर उपलब्ध होती हैं, और एक बड़ा हिस्सा हार्ड-बाउंड भी होती हैं। एक और बात जो लोकप्रिय पुस्तकों में है कि वह एक शृंखला बनती है, या नये संस्करण में तथ्य जुड़ते रहते हैं। इसलिए लेखकों से लम्बा करार भी होता है। मसलन रामचंद्र गुहा को गांधी जैसे बहुलिखित पुस्तक-शृंखला के लिए अस्सी लाख रुपए का एडवांस मिलना एक घटना मानी जाती है। ख़ास कर तब जब गांधी-वांग्मय बाज़ार में कई वॉल्यूम में उपलब्ध हो, और गांधी पुस्तकालय उन पर पुस्तकों से भरा हो। इस एडवांस का मतलब था कि अभी भी इस मुद्दे पर स्कोप बचा था। गांधी के पहले, गांधी के बाद, फिर नेहरु के बाद, मोदी के पहले, मोदी के बाद… इसका कोई अंत नहीं। और यह करार उसी लेखक को मिलेंगे तो यह लेखकीय बीमा भी है, ख़ास कर जब लेखक विशेषज्ञ बनता जा रहा हो।
इसमें तीन रास्ते फूटते हैं। एक, जो ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वगैरा से गहरे शोध आधारित पुस्तकें आती हैं, जिसके पाठक विश्व-स्तर पर बहु-अनूदित हैं लेकिन किताबें जनमानस से दूर हैं। दूसरी, जो लोकप्रिय प्रकाशकों से रोचक अंदाज में लिख कर आती हैं। यह कथात्मक कथेतर भी हो सकती है, या कसा हुआ रोचक लेखन भी। जैसे एस हुसैन जैदी की मुंबई अंडरवर्ल्ड पर किताबें छा गयीं। और तीसरी, जिसमें फ़िक्शन या संस्मरण का हिस्सा अधिक है। जैसे अमिताव घोष की पुस्तकें।
एक पाठक के तौर पर मैं जब एक मुद्दे पर पढ़ता हूँ तो उस पर लिखी एक के बाद एक किताबें खरीदता-पढ़ता चला जाता हूँ। ख़ास कर अगर कुछ रहस्य पहली किताब में नहीं खुले। और ताज्जुब यह है कि जो एक कथेतर लेखक है, वह भी यही करता है।
(कथेतर विधा का लेखन ही वास्तव में कालजयी होता है साहिंद में अक्टूबर 4 2018 को और कथेतर पर आगे की बात अक्टूबर 8 2018 को प्रकाशित हुआ था।)