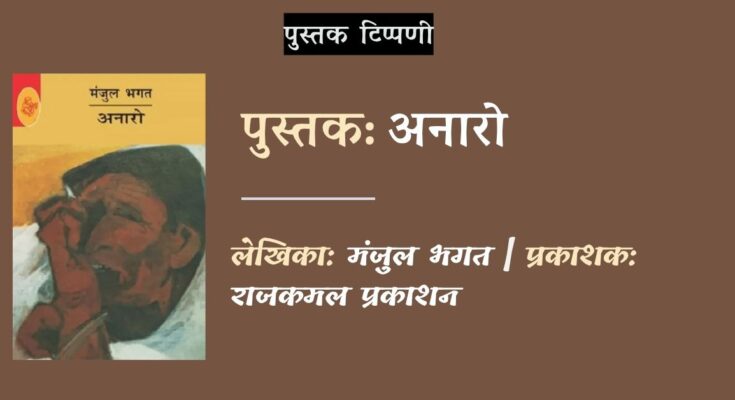संस्करण विवरण:
फॉर्मेट : पेपरबैक | पृष्ठ संख्या: 101 | प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन
पुरस्कार : यशपाल प्रतिष्ठान और उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा पुरस्कृत
पुस्तक लिंक: अमेज़न
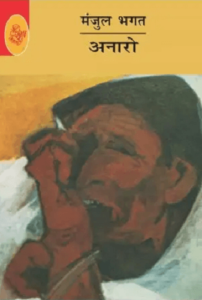
पहला वाक्य:
अनारो आज बेहद खुश थी।
कहानी
दिल्ली की मदनगीर बस्ती में रहती है अनारो। पास ही पोश कॉलोनी में मौजूद घरों में चूल्हा चौका करती है और अपने परिवार का भरण पोषण करती है। नन्दलाल नाम का एक पति है जिसका होना न होना बरबार है। दो बच्चे हैं जिनको पालने की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही है। अपने बच्चों की ज़िन्दगी के चारो ओर ही अनारो की ज़िन्दगी कटती है। वही उसका संसार है और उन्हीं के लिए वो हाड़तोड़ मेहनत करती है।
उसकी कुछ इच्छाएँ है, कुछ सपने हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती हैं।
क्या उसकी वो इच्छाएँ पूरी होती हैं?
आखिर उसकी आकांक्षाएँ क्या हैं?
और उन इच्छाओं की पूर्ती के लिए उसे क्या करना पड़ता है?
मुख्य किरदार:
अनारो – उपन्यास की नायिका
नन्दलाल – अनारो का पति
गंजी उर्फ़ शांति – अनारो की बेटी
छोटू – अनारो का बेटा
रामभरोसे – अनारो का पड़ोसी और बहनोई
चम्पा – अनारो की बहन
छबीली – एक महिला जिसके साथ नन्दलाल का रिश्ता था
मोटी, बंगालन,टीचर – यह वह महिलाएं थीं जिनके घर पर अनारो काम करने जाती थी
टिप्पणी
राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित मंजुल भगत का उपन्यास ‘अनारो’ मूलतः एक संघर्ष की कहानी है। अनारो इसका केंद्रीय पात्र है जिसे अपने परिवार को चलाने के लिए घर-घर जाकर काम करना पड़ता है। उसका पति है लेकिन उसका होना न होना बराबर है। फिर भी अनारो अपनी जीवटता और अपने हौसले से अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष करती है। यह संघर्ष पूरी ज़िन्दगी चलना है वह यह भी जानती है।
उपन्यास पढ़ते हुए हम अनारो के इन्हीं संघर्षों के भागीदार बनते हैं। अनारो का किरदार एक आम महिला का किरदार है। अब की अनारो एक तेज तर्रार औरत है जो कई बार तीखा भी बोल देती है लेकिन वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। वह क्या परिस्थितियाँ थी जिसने उसे ऐसा बनाया यह भी इधर देखने को मिलता है। अनारो के यादों के झरोखे के माध्यम से उसकी गुजरी ज़िन्दगी के विषय में पता पाठक को चलता है। वह अभी जैसी है वैसे वो कैसे बनी यह देखने को इधर मिलता है। यह चीज कथानक को पठनीय बनाती है।
अनारो जिस परिवेश से आती है उधर की सोच उस पर दिखती है। कई बार पढ़ते हुए लगता है कि वो अपने विचारों और सोच की बेड़ियों से जकड़ी हुई है पर यही बात उसे यथार्थ के नज़दीक ले आती है। उसे लगता है कि पति मारता है तो प्यार भी करता है। उसे लगता है कि बेटी का ब्याह हो तो धूम धाम से हो भले ही इस धूम धाम के चक्कर में वो कर्जे के बोझ तले दब जाए। यह बोझ वह नाम और इज्जत के लिए ढोने को तैयार है। फिर अपने पति के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित करते हुए वह ऐसे मौके पर गर्भवती हो जाती है जो कि उसके लिए शर्मसार करने वाली बात होती है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम आजकल चलाए जाते हैं लेकिन कैसे उनका ज्ञान न होने के चलते उसे परेशानी उठानी पड़ती है यह हम देखते हैं।
उपन्यास का अंत बेहद मार्मिक है। अपने पति,ऐसे पति जिसने शायद कष्ट के सिवा उसे कुछ न दिया हो, के तारीफ के दो बोल सुनकर वो जिस तरह निहाल हो जाती है और गर्व से फूली नहीं समाती है उसे देख उस वक्त मुझे लगा कि अनारो को एक बेहतर पति मिलना चाहिए था। ऐसा पति जो उसका ख्याल रख सके और उसके सुख दुःख में हाथ बाँट सके।
अनारो का मन तो आज पहले से ही ऐसा दुखी हो रहा था कि बस, कोई दो शब्द प्यार के उससे बोल ले, तो वह जी जाय….वह खिंची चली आयी नन्दलाल के पास। एक सहारा..कोई थामनेवाला.. दो बोल प्यार के …एक धूल भरी राह पे…थकी हारी अनारो छइयाँ तले बैठकर,पेड़ से टेक लगा रही है…
पृष्ठ 76
कैसा मीठा हो गया है? चाहिए…अनारो को भी प्यार चाहिए.. छाँव चाहिए…नन्दलाल, तू मीठा बना रहे..अपना बना रहे तो जी जाएगी अनारो….झले जायेगी जिनागानों को… भूख प्यास को पी जाएगी…बीमारी-हारी को भी जीत लेगी….अब तुझसे लड़ने का दम मुझमे नहीं है रे…
अनारो की ज़िन्दगी के अलावा हम उसके कर्मस्थली को देखते हैं। अनारो के माध्यम से उस समाज को भी पाठक देखता है। जिन घरों में वो काम करती है उधर उसे हर तरह के लोग मिलते हैं। ऐसे लोग जो उसकी मदद भी करते है, तो कभी उसे दो बातें सुना भी देते हैं। कभी वो उनसे लड़ती-झगड़ती भी हैं तो कभी उनके प्रेम पर निहाल भी हो जाती है। अक्सर अमीरों को कहानी में दुष्ट दिखाया जाता है लेकिन इधर चित्रण ऐसा नहीं किया है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। इधर भी यही देखने को मिलता है।
जितने तरह के घर,उतनी ही रकम की मालकिने। उतनी ही हिदायते,नसीहतें। कोई किसी बात से खुश, कोई किसी काम से। किसी का मिजाज कोई, तो किसी का कुछ। कोई सारंगी तो कोई तबला।बस, एक अनारो ही थी, जो थी एक, पर कई जगह बँट बँट कर काम करती थी। सांझ पड़ती, तो अपने को सबों घरों से समेटकर, फिर से एक ईकाई बना लेती थी, इसी छप्पर में घुसने के लिए। जीना इसे नहीं कहते हैं, इतना उसे भी पता है। जीना वही है, जो ढेर सारे घरों में होता है,जहाँ वह बरतन घिसने,कपड़े धोने, या फर्श बुहारने जानती है।
पृष्ठ 23
उधर ही एक घर में वो देखती है कि जैसी हालत उसकी है वैसी ही उस घर की मालकिन की भी है। भले ही दोनों के बीच में धन की दीवार हो लेकिन जैसे उसका पति उसे धोखा देता है वैसे ही उस मालकिन का पति भी है। यह देखकर वह द्रवित हो जाती है और उसे अहसास होता है कि औरत किधर भी हो उसकी नियति एक जैसी है।
उसे सब पता है। कोई बतला गया होगा। चटखारा लेनेवालों की कमी थोड़ी है। भला बताओ, जो दुःख अनारो के, वही क्लेश इत्ती बड़ी सेठानी के। बस, औरत जात यहीं मार खा जाती है। पैसा भी किस काम का। इससे तो अनारो भली। आदमी भागा भी तो दोनों को ही तज के। सौत के पास जाके रह तो नहीं गया1 मोटी बेचारी तो रोये-पीटेगी भी तो दरवाज़ा बंद करके। इज्जत के मारे मरी जायेगी।
पृष्ठ 26
उपन्यास के बाकी किरदार कहानी के अनुसार हैं। सभी जीवंत प्रतीत होते हैं। हाँ, नन्दलाल से मुझे कोफ़्त हुई थी। लेकिन ऐसे किरदारों को मैंने देखा है। वो शादी तो कर लेते हैं लेकिन उसकी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना नहीं जानते हैं। घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं और फिर अपने बेटे पर दोष न रखकर नयी आयी लड़की को ही टोकते हैं वो पति को काबू में न रख सकी। यही चीज इधर भी होती दिखती है। कई बार समाज पुरुष को वरीयता देता है और उसका होना परिवार में जरूरी होता है। यह तब जबकि वो जिंदा हो। यह बात अनारो भी समझती है और न चाहते हुए भी अपने परिवार के लिए कदम उठाती है।
बस, दस रोज किसी तरह गुजारा कर लो,फिर आकर मैं सब सम्भाल लूँगी। अपने लिए तो सौ जन्म भी न जाती, पर बेटी के लिए बाप को खोजकर लाना ही पड़ेगा।
पृष्ठ 55
उसके ऐसे ही फैसलों से उसके प्रति इज्जत और बढ़ जाती है। उसका यह काम आम फ़िल्मी नायिकाओं जैसा नहीं है। फिल्म होती तो नायिका विद्रोह करती और सब कुछ अच्छे से निपटता। लोग तालियाँ भी बजाते लेकिन असल ज़िन्दगी में ऐसा नहीं होता है। न जाने से जाना एक मेरी नज़र में बड़ी बात है क्योंकि इसमें वो खुद के अभिमान को किनारे रख वह काम कर रही है जो उसके बच्चों की ख़ुशी के लिए जरूरी है।
अनारो की ज़िन्दगी में यही बच्चे हैं। एक लड़का और एक लड़की हैं। इनको लेकर उसके बड़े ख्वाब नहीं है। लड़का पढ़कर चपरासी की नौकरी करने लगे और लड़की का ब्याह अच्छे घर में हो जाये। वह यही अपनी ज़िम्मेदारी समझती है। जिस परिवेश से वह आयी है उधर वो जानती है कि यही बड़े सपने हैं।
अनारो के माध्यम से हम उस परिवेश को भी देखते हैं। वहाँ जीवन कैसे चलता है उसका भी खाका लेखिका ने हमारे सामने खींचा है।
वह झुग्गी थी सुनहरे पुल पर। वहाँ तो कितनी ही स्वयम्भू सासें और मुँह बोली ननदें निकल आईं, जिन्होंने चौदह वर्ष की अनारो को सब कुछ सिखा दिया।
पृष्ठ 91
अब जैसी तेज तर्रार कहाँ थी अनारो। वह सब तो उसने बाद में सीखा। मदनगीर के टोले की थी भी यही रीत। खाने को चाहे हो न हो, बीमारी चाहे सब खून चूस ले, पर लड़ते समय तो सबके तन में नये प्राण भर जाते। जिसने भी ईंट का जवाब पत्थर से न दिया, वही सबसे बड़ा मूर्ख। लड़े न तो जी कैसे लगे?
कहानी का अंत ऐसे मोड़ पर होता है जहाँ वो अपना एक सपना हासिल कर लेती है। अनारो की ज़िन्दगी तो चलती रहेगी और उसके संघर्ष भी। वो खुद को साबित कर देती है और जो सोचा था उसका कुछ हिस्सा तो पा ही लेती है। पाठक को उसके संघर्ष अपने संघर्ष लगते लगते हैं और उसकी जीत अपनी जीत लगती है। उपन्यास खत्म करने के यही आशा रहती है कि अनारो अपने बाकी सपने भी पूरे कर सके। आशा के सिवा और पाठक कर क्या सकता है।
अंत में यही कहूँगा कि यह एक साधारण सी लगने वाली स्त्री की जिजीविषा की कहानी है। एक जीवट औरत के संघर्ष की कहानी है जो उसे साधारण से असाधारण बना देती है। यह शायद अनारो जैसी कई और स्त्रियों की कहानी है जिनके लिए सामान्य जीवन जीना भी किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। आप उन्हें देखेंगे तो उनमें असाधारण कुछ नहीं लगेगा। लेकिन असाधारण रूप से मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी साधारण और सामान्य बना रहना ही उनके विषय में काफी कुछ कह जाता है। एक पठनीय उपन्यास। अगर पढ़ा नहीं है जरूर पढ़ा जाना चाहिए।
उपन्यास के कुछ अंश:
‘हुउँ!’ पिच्च से अनारो ने पीक थूक दी,’ मरे मेरे काम को नज़र लगाते हैं। कभी कहेंगी, दस-दस घर तो पकड़ रखे हैं। लेट नहीं आएगी तो और क्या होगा! छोड़ क्यों नहीं देती एक आध काम? अजी वाह! क्यों छोड़ दूँ दो-एक काम? अपने हाड़-गोड़ तोड़कर कमाती हूँ, तुम्हारी छातियों पे साँप काहे लोटता है?’ और वो तो गंजी का बाप अगर भगोड़ा न होता तो काहे को अनारो को इतना खटना पड़ता! काम न करे तो क्या बच्चों को खाने गुरुद्वारे भेज दे?
सारे शरीर में दो चीजें ही ऐसी थीं, जिनकी गति और शक्ति का मिलान अनारो के खान-पान, रहन-सहन से कतई न था- एक उसकी बाजू और दूसरी उसकी तीखी-तुर्श जुबान। बाकी उसका पेट तो कमर से इस तरह लगा रहता कि वहाँ, उसकी फटी साड़ी की मलगुजी पटलियों का खुंसा रहना ही दूभर हो जाता; पर इस पिचके पेट की क्षुधायुक्त दुर्बलता का कुप्रभाव उसके बाजुओं पर कभी न पड़ा। न जाने कौन सी चाबी उनमें भरी रहती कि वे सदा ही द्रुतगति से संचालित रहते। उसकी तेज़ ज़बान भी तो गुरबत की कड़ी मार खाकर कुंद नहीं पड़ी। कहीं कुछ थोड़ा सा आत्मसम्मान भी बचा पड़ा था, जो अपमान की चोट लगते ही, पत्थर की रगड़ खाकर तेज हुए चाकू की मानिंद उसकी जुबान को और भी पैनी और बेधक बना देता।
सवेरा हुआ। अनारो उठी, तो उसे लगा -वह सोकर नहीं, मरकर उठी है। बदन में वही पहलेवाली बासी कसमसाहट अब भी भरी थी। अंग-अंग पिरा रहा था। न सवेरा सवेरापन लिए था, न दिन के उजाले में उसे कोई रोशनी नज़र आई। न कहीं कोई ताजगी थी, न आस। मुख की बासी बू की तरह दिन उगा था।
पुस्तक लिंक: अमेज़न