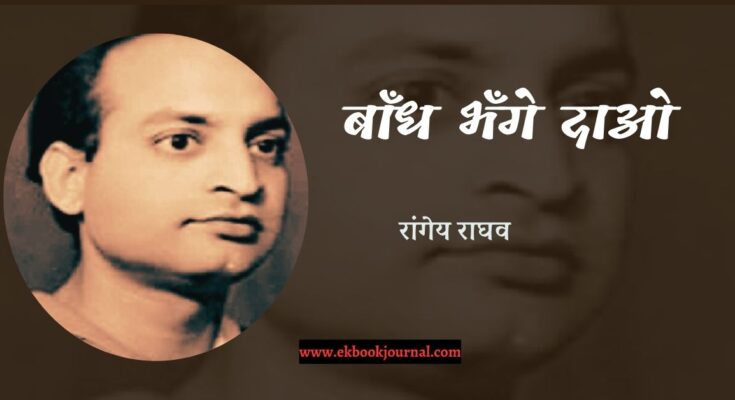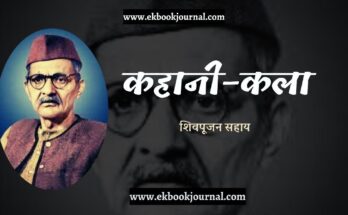रेल रुक गयी। इम लोग बेहद फुर्ती से सामान उतारने लगे। एक बक्स, एक बिस्तर, एक बक्स एक बिस्तर – दवाओं के बड़े-बड़े बक्स… सब कुल एक डेढ़ मिनट में।
भुइयाँ लम्बी-लम्बी साँसे लेता हुआ मुस्कराता जाता था। वह अपनी आसामी उच्चारण की अंग्रेजी में कहने लगा, “सब उतार लिया! सब! मगर गाड़ी तो अभी तक खड़ी है!”
जसवंत अभी तक अदद गिन रहा था। उसने एकाएक ही सिर उठाकर कहा, “अरे हाँ, गाड़ी तो अभी तक खड़ी है।”
हम चारों ने देखा खिड़की पर खड़े वृद्ध महाशय बार-बार अपनी गलती के लिए क्षमा माँग रहे थे। उन्होंने कहा था गाड़ी यहाँ केवल एक मिनट रुकेगी। सब हँस पड़े। गाड़ी चली गयी, ठीक दस मिनट रुककर। चला गया वह आफ़त का गुबार जब आदमी को एक फुट भर जगह के लिए अपनी सत्ता की गवाही पुकार-पुकारकर देनी पड़ती है, जहाँ सब परेशान, सब कठोर मुसाफिर, परवश, अपने आपके गुलाम!
कलकत्ते की चने की दुकानों से लेकर छोटे पवित्र भोजनालय जहाँ मैले कपड़ेवाले बदबूदार निचुड़े हुए इंसान बैठते हैं, हमने अनेक स्थल देखे थे, किंतु अब जो पेट की आग धधकने लगी थी उसने याद दिलाया, कल कुछ खा-पी नहीं पाये सिवाय एक प्याले चाय के, तो उसी का यह परिणाम था। मानो यदि मनुष्य खुद लड़कर खाना नहीं खायेगा तो और कोई यहाँ पूछने तक को नहीं।
हम पश्चिमी अपने प्रांत की याद में थे । यहाँ स्टेशनों पर पूरी तो मिलती थी, मगर साथ में केवल मिठाई जिनके भाव सुनकर एकाएक विचार बदल देना पड़ा था। चली गयी वह रेल जिसे एक दिन भारतीयों ने देवता कहा था। जिसने भारत में एक दिन नवीन जागृति फैलायी थी, और आज जो जीवन की विषमता का फुँकारता अजगर बनकर शून्य को डसती चली जाती थी।
वह भीड़, वह गर्मी, वह भिंचाव! क्षण भर के लिए जैसे यह कुष्टिया (नदिया जिले का एक कस्बा) स्वर्ग था। कलकत्ते के विराट वैभव के बाद यह छोटा टाउन जैसे मशीनों के देश के बाद आदमी का निवासस्थान था। विशाल ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर होकर भी जैसे सब कुछ ऊपर की तड़क-भड़क था और मैंने देखा, कलकत्ता वास्तव में बंगाल नहीं था।
रेल में से देखी थी वही भागती हुई हरियाली, वही झिलमिलाते ताल किंतु अब देखा कि यहाँ हँसने में भी उदासी की एक कराह थी, हिलते हुए पत्तों का-सा एक कम्पन था।
आकाश में सुहावने बादल छा रहे थे। घटाओं का क़ातिल सुरूर ताल की झिलमिलाती पुतलियों में अक्षय मरोर-सी भर कर बहती हवा में किलकारी बनकर गूँज उठता था। कितना-कितना विश्राम, कितनी-कितनी शांति, जीवन का अपनापन उस नीरवता में बार-बार जैसे सुबक रहा हो, भीख माँग रहा हो, जहाँ प्यार, प्यार रहकर भी दुराशा था, अलगाव था, हाहाकार था…
हम लोगों के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गयी थी। बच्चे शोर कर रहे थे। दवाओं का डिब्बा और बक्स खोलकर रख दिये गये। एक विद्यार्थी आकर अंग्रेजी में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। अनेकों ने उससे पूछा और हम लोगों के बारे में ज्यों ही सुना, भीड़ में से कुछ व्यक्ति निकल आये।
एक साँवला-सा पतला-दुबला युवक बोल उठा, “आप लोगों के लिए ही हम यहाँ आये हैं। स्वागत!”
अभी वह बात समाप्त भी नहीं कर पाया था कि एक आदमी दौड़ता हुआ आया। एकदम बँगला में उसने कहा, “कब शुरू करेंगे यह लोग अपना काम?”
ज़ियाउद्दीन ने कहा, “कल।”
आदमी करीब-करीब चिल्ला ही उठा, “तब तो कोई फ़िक्र नहीं, कोई फ़िक्र नहीं।” और वह अफ़सरों को कुछ गंदी गालियाँ दे उठा।
हम लोग चलने लगे। युवक कह रहा था, “हॉस्टल है एक स्कूल का, उसमें आप लोग ठहर जाइए, पास ही है…”
सचमुच ही मैंने देखा लोग इन डॉक्टर विद्यार्थियों को देखकर एकबारगी निश्चिंत-से हो गये थे। उनके चेहरों पर जैसे दुःख की खुली किताब थी। जो भी इंसानियत का थोड़ा-बहुत माद्दा रखता है, वह आसानी से पढ़ सकता है उस सबको।
साँझ घिर चली थी। बादल झूम उठते थे जैसे लुढ़कने के अतिरिक्त उनके पास और कोई काम ही न था। घास फरफरा रही थी। समस्त वातावरण में एक कल्लोल लहरा रहा था जैसे वेदना से भरे श्वास बंशी में गूँज उठते हैं।
हम लोग होस्टल की ओर धीरे-धीरे चल रहे थे। एक व्यक्ति जसवंत से कह रहा था, “एक समय था जब कुष्टिया कभी हाथ नहीं, पसारता था। तो आज तो वह बात नहीं है।” कहनेवाला चुप हो गया। और मुझे लगा जैसे आते अँधकार की ढाल पर वह तीव्र बाण टकराकर झनझनाते हुए टूट गये। “एका नहीं बाबू, एका नहीं, एका नहीं है। एका नहीं है तभी तो आज कुष्टिया की यह हालत है। ऊँची-ऊँची लहरें जब उठती हैं तब किसकी खेया में पानी नहीं भर जाता किंतु क्या बिना पानी निकालें नाव, जल में सुरक्षित चल सकती है?”
यह प्रश्न आज उसकी सत्ता का प्रश्न है, उसके जीवन की माँग का प्रश्न है।
मोहिनी टेक्सटाइल मिल में एक मज़दूर कहने लगा, “हम क़रीब तीन हज़ार मज़दूर हैं। हमारी अपनी एक यूनियन है, जिसमें हम क़रीब हज़ार आदमी हैं।”
वह तो बात ही और है । एक और ने कहा, “सरकार ने कह दिया हम बीज नहीं देंगे, मगर किसानों के संयुक्त मोर्चे के सामने उसको देना पड़ा। और बाबू पूरे ढाई सौ मन में से जब और यूनियनों को अपने-अपने हिसाब से दस-दस मन मिले तब अकेली बारखड़ा यूनियन को मिले पूरे 75 मन। सरकार आज भी कोई ठोस ‘राशनिंग’ नहीं लगाये है, मगर क्या हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ हो सकेगा?” उसका प्रश्न स्वयं उत्तर था। रात आ गयी थी, दुकानों पर धुँधले चिराग जल रहे थे। बादलों के फट जाने से एक झिलमिलाता-सा प्रकाश काँप रहा था।
होस्टल के दरवाज़े पर सब लोग लौट गये। छोटे-बड़े अनेक विद्यार्थियों ने आकर हमें घेर लिया। उनके अधरों पर एक तरल हँसी थी। पर आँखों में एक भय-उदासी की छाया भी एक अदभुत वास्तविकता थी। दीपक की शिखा जल रही थी। किंतु निर्धूम नहीं, निश्शंक नहीं। क्षणभर पहले ही तो वह लौ तूफ़ान में काँप उठी थी। बुझते-बुझते बची थी। मैंने सोचा और समझा कि यह बालक इसलिए नहीं मुस्करा रहे हैं कि उन्हें उस अकाल के भयानक पिशाच से लड़कर बच रहने का गर्व था बल्कि इसलिए कि उनके सामने आज ऐसे मनुष्य खड़े थे, जिन्होंने उनके मनुष्य बने रहने के अधिकार को स्वीकार किया था, उस समय जब कि उनके अपने उनके नहीं थे। जब वह घृणा और स्वार्थ के कारण एक दूसरे पर विश्वास कर सकने तक की श्रद्धा को भल चुके थे।
हम लोग हरी-भरी दूब पर बैठ गये। लड़कों ने हमें चारों ओर से घेर लिया। बात चल पड़ी।
हवा मतवाली चल रही थी। प्रकाश ऊना-ऊना हो उठता था। गोधूलि की तंद्रा प्रतिध्वनित-सी पृथ्वी पर अलसा उठती थी।
एक आठ या नौ वर्ष का बालक एकाएक कह उठा, “चावल तो मिलता ही नहीं। अकाल में तो हमने बाजरा खाया था, बाजरा।” और सब हँस पड़े। सचमुच यह हँसी नहीं थी। जब मनुष्य निराशाओं से घिरा अपने ऊपर रोने के स्थान पर मुस्करा उठता है, तब उस के हृदय का प्रत्येक स्वर गीत बनकर निकलता है। उसकी एक वही वेदना अँधकार में एक क्षण भर का जुगुनू बनकर टिमटिमा उठती है।
साँवला युवक कहने लगा, “मार्च 1942 में कुष्टिया में अन्न-संकट प्रारम्भ हुआ। अप्रैल में कीमत 12 से 20 हो गयी और जून में तो पूरे 40। तीन महीने तक यही हालत रही। बाज़ार में चिड़िया तक के लिए एक दाना चावल नहीं था। 60 फीसदी गाँववाले और ‘टाउन’ में आधे से भी ज्यादा लोग अरहर, मसूर और चने की दाल पर ज़िंदा थे। लोग घरों से बाहर आते डरते थे कि एक नहीं, दो नहीं, सड़कों पर अनेक भूखे दम तोड़ते होंगे। और डरते थे घर जाते हुए, जहाँ बच्चे, अपने बच्चे भूखे बैठे होंगे। माँ बेटी को देखती थी, पति पत्नी को देखता था। पिता की आँखें डूबते हुए अरमानों सी बच्चों से टकराकर तड़पकर भीग उठती थीं। किंतु कहीं कोई राह न थी। घर खाली थे। बाजार ख़ाली थे। चारों ओर प्राणों की ममता दोनों हाथ उठाकर हाहाकार कर रही थी। लोग घर में मरते थे। बाज़ार में मरते थे। राह में मरते थे। जैसे जीवन का अंतिम ध्येय मुट्ठी भर अन्न के लिए तड़प-तड़पकर मर जाना ही था। बंगाल का सामाजिक जीवन कच्चे कगार पर खड़ा होकर काँप रहा था। और वही लोग जो अकाल के ग्रास बन रहे थे, मरने के बाद पथों पर भीषणता के पगचिह्न बने सभ्यता पर, मानवता पर भयानक अट्टहास-सा कर उठते थे।
युवक उत्तेजित था। वह कह रहा था, “हमें आज इस बात में लज्जा नहीं है कि हमने हिंदुस्तान से भीख माँगी है। यह जीवन की भीख हमने अपने लिए नहीं माँगी। बंगाल का इसमें अपमान नहीं है। आज हिंदुस्तानी और बंगाली का भेद नहीं किया जा सकता है आज एक ओर मनुष्य हैं, दूसरी ओर वे नर-पिशाच जो मनुष्य को तड़प-तड़पकर मरते हुए देखकर भी चुप रह जाते हैं और रुपए की खनखन में अपनी सारी सभ्यता और मनुष्यत्व को डुबाकर अपनी राक्षसी आँखें तरेरा करते हैं। हमारी कराह कोई पराजय नहीं है। दुनिया हमें नहीं मर जाने देना चाहती। तभी तो आये हैं आप लोग, कोई आगरे से, कोई आसाम से। जिस जनता ने आपको भेजा है वह हमारी है, हम उनके हैं और आज जो यह कच्चे चने ढेर लगाये बैठे हैं, कल जब हम लोगों का एका भट्टी की भीषण आग बनकर धधक उठेगा तब यह चने निस्सहाय से तड़प-तड़पकर इधर-उधर भागेंगे। हमने इतिहास पढ़ा है। हिंदुस्तान बार-बार इसलिए गुलाम होता गया कि कोई किसी की मदद नहीं करता था, मगर आज तो वह बात नहीं। यह अकाल जो गुलामी है, जो एक भीषण आक्रमण है, उसे हमें आस्तीन के साँप की तरह कुचलकर खतम कर देना होगा। आज यदि हमें लज्जा हो सकती है तो यही कि हमारी ही भूमि में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने हमें इस दशा पर मजबूर किया है। किंतु मैं पूछता हूँ कि क्या आपके यहाँ ऐसे नरपिशाच नहीं हैं? बात इतनी ही है। कि संसार में दो ही लोग हैं। एक हम, एक वह। और दोनों में कभी सामंजस्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह रुपए से नापना चाहते हैं और कौन कहता है कि हमें उससे बगावत करने का अधिकार नहीं है।”
युवक लम्बी-लम्बी साँसे लेने लगा। एक लड़का जो मुसलमान था, कहने लगा, “ठीक कहा है, दादा ने बिलकुल ठीक कहा है… आपको मालूम नहीं मगर हमने अपनी आँखों से देखा है।
“पार साल की बात है। मई का महीना था।
“लोग महाजनों के पास बाज़ार जाते थे और वे कहते थे, ‘चावल? कहाँ है चावल? कुछ छोड़ती है यह फ़ौज? हम तो कह-कहके मर गये। मगर सरकार ने ले ले जाकर सब डाल ही दिया न उस अनंत भट्टी में? और… बाबू तुम समझते हो कि अगर होता तो मैं तुम्हें नहीं देता? किसके लिए दुकान खोली है आख़िर, कोई बाँधके तो ले नहीं जाऊँगा मैं सब?
“और जब बहुत खुशामद होती तो महाजन कहता, ‘क्या करूँ, तुम्हारा तो दुख देखा नहीं जाता अब। मगर लाचार हूँ। कितनी बुरी चीज़ है यह मजबूरी भी। खैर भाई। व्यापार करने को तो मेरे पास कुछ नहीं। मेरे पास अपना, अपने बाल-बच्चों का पेट पालने को 3 मन चावल ज़रूर ज्यादा है। तुम्हें दे दूँगा। आख़िर पुरखों की लाज निभानी ही होगी। मैं तो ऊपरवाले का भरोसा किये हूँ। वह उबारे तो मर्जी उसकी। तुम रात में आना। मगर शर्त है पता न चले किसी को और देखो दाम की क्या बात है? जो दाम है उससे एक पैसा कम ही दे देना…।
“और इसी तरह बात खुलने लगी। पचासों आदमियों ने जब एक ही बात सुनी तो उन लोगों के कान खड़े हुए।
“एक दिन, मई की अँधेरी रात, बीस क़दम पर कोई कुछ करे, दिखना असम्भव था। हवा तेज़ी से चल रही थी। और हमारी अन्न कमिटी के वालंटियर्स ने एक छिपा हुआ गोदाम ढूँढ निकाला। वह महाजन हिंदू था, पूरे कुष्टिया का एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति। चावल, गेहूँ, दाल, उसमें करीब ढाई हजार मन सामान था।
“दारोगा मुसलमान था। उसने आते ही परिस्थिति को भाँप लिया। जानते हैं, उसने क्या कहा? कि तुमने बिना इजाज़त किसी दूसरे के घर में घुसने की जुर्रत की तो कैसे? …मैं तुम लोगों का चालान करूँगा।
“विक्षोभ से भर गया था हमारा मन! 10-15000 महीना कम नहीं होता बाबू रिश्वत का। और हड्डी डालकर कुत्ते का मुँह बंद करके ही तो चोरी की जा सकती है, और वह भी तब जब कि घर के पहरेदार सब गाफ़िल हों।”