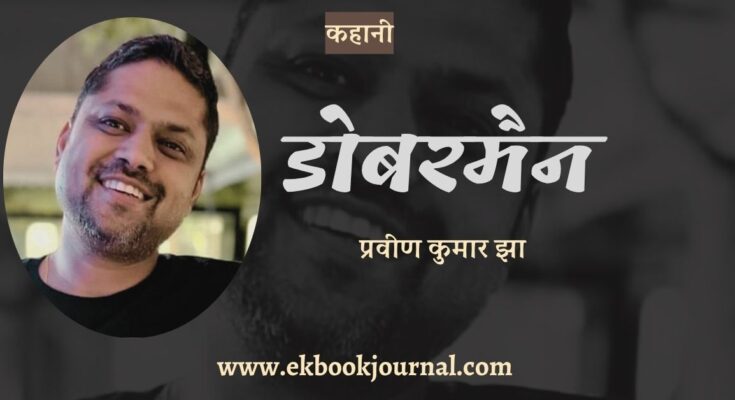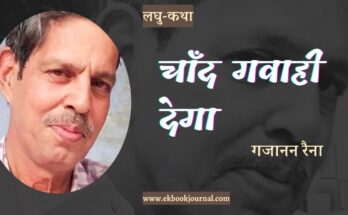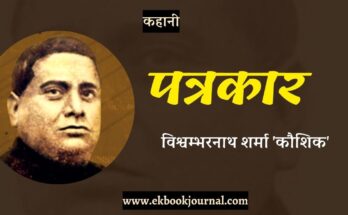मेरे क़स्बे में दो ही तरह के लोग डॉक्टर बनते। पहले वे, जिनके ख़ानदान में सभी डॉक्टर हुए। और दूसरे वे, जिनके ख़ानदान में कोई डॉक्टर ना हुआ। मैं दूसरी कैटेगरी में था।
मेरा घर मुहल्ले के केंद्र में था। यानी मुहल्ले से सड़क तक आने के लिए मुझे सभी चक्रव्यूह तोड़ कर ही आना पड़ता। ये नहीं कि गाड़ी घर से निकाली और सड़क पर आ गये। गाड़ी निकल पाएगी, तब तो सड़क पर आएगी। इसलिए गाड़ी रखने का कोई मतलब ही नहीं था। गाड़ी तो छोड़िए, रिक्शा भी आख़िरी तोरण-द्वार पर आकर बिदक जाता, की इससे आगे नहीं जा पाएगी। हम रिक्शे से उतर कर अपने शाही मकान तक का सफ़र पैदल तय करते।
गली उतनी भी सँकरी नहीं थी। मेरे ख़याल से पाँच फ़ीट चौड़ी तो ज़रूर थी, लेकिन उसके पहले मुहाने पर एक बिजली का खम्भा गड़ा था, जहाँ चार फ़ीट हो गयी होगी। उसके बाद वह बायीं मुड़ती तो एक तालाब के उफनते पानी और जलकुम्भियों ने उसे तीन फ़ीट का कर दिया होगा। आख़िर एक पतली कीच-सेतु से हम अपने महल पहुँचते, जो तीन ओर तालाब से घिरा था। ऐसा अद्भुत भूगोल मुझे अपने घर के बाद सीधे बम्बई के हाजी अली दरगाह में मिला। उस वक्त जब मुहल्ले का हर दूसरा युवक बिहार से निकल कर बम्बई-दिल्ली जाने की तैयारी में था, मेरी ज़द्दो-ज़हद बस उस प्रायद्वीप से निकल कर सड़क तक पहुँचने की थी। और उसका एक ही हल था – डॉक्टर बनना। वही निकास-बिंदु था।
मुहल्ले के सभी लोग जब अपने-अपने घर से निकल कर सड़क पर पहुँचते तो सड़क किनारे आमने-सामने बने दो मकान नज़र आते। उन दोनों आलीशान मकानों के बीच से निकलते ही, अचानक सड़क चौड़ी हो जाती। जैसे वे देवदूतों के मकान हों, और हमें मोक्ष मिल गया हो। और वे वाक़ई फ़िल्मी देवदूत थे। दोनों मकान डॉक्टर के थे। यह कोई छुपी बात नहीं थी। उनके घर के दरवाज़े पर एक संगमरमर की पट्टी थी, जिस पर डॉक्टर साहेबानों की पूरी वंशावली लगी थी। उसे पट्टी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह पूरा खम्भा ही डॉक्टरों के नाम, उनकी डिग्रियों से पटा पड़ा था। बड़े डॉक्टर साहब, बड़ी डॉक्टरनी साहिबा, तीन बेटे डॉक्टर साहब, एक बेटी डॉक्टर साहिबा, तीन पतोहू डॉक्टरनी साहिबा। अब यह मालूम नहीं कि सभी एक ही घर में रहते थे, या अलग-अलग घर में। मैंने तो उस घर में बस डोबरमैन कुत्ता ही देखा, जिसे देखना-सुनना सहज था। वह इन देवदूतों का द्वारपाल था।
खैर, यह कहानी इन मकानों, उन गलियों, इन कुत्तों के बहुत बाद की है। जब मैं आखिर डॉक्टर बन गया। मेरे शहर में भगवान की दया से इतने डॉक्टर मौजूद थे, कि अगर मैं एक सड़क किनारे मकान बना कर, संगमरमर की पट्टी लगवा कर, डोबरमैन कुत्ता पाल कर बैठ भी जाता, तो भी यह कोई बचपन का फ़िल्मी प्रतिशोध ही कहलाता। दरअसल जहाँ वे मकान बने थे, वहाँ पहले एक तालाब हुआ करता। उस तालाब को जब मिट्टी डाल-डाल कर भर दिया गया, तो मुहल्ले का पहला क्रिकेट मैदान तैयार हुआ। नयी मिट्टी थी, तो बाउंस कम होती, और गेंद की गति भी धीमी। खेलना वाकई कठिन होता। लेकिन, स्कूल छूटते ही न जाने कितनी टीम और कितने मैच एक साथ चल रहे होते। किसी के शॉट पर किसी और खेल का फ़ील्डर कैच पकड़ ले रहा है। वहीं लड़ाई-झगड़ा चल रहा है। ऑडियो-कैसेट के रील से मैदान बाँटे जा रहे हैं। फिर, कुछ दिनों में वहाँ रेत गिराए जाने लगी। सीमेंट-कंक्रीट मिलाने वाले दैत्याकार मशीन आने लगे, मकान बनने लगे। वे देवदूत शहर को निरोग करने अवतरित हुए होंगे, लेकिन हमारे क्रिकेट-मैदान पर आसुरी अतिक्रमण कर गए। फ़्लैशबैक में यूँ लगता है कि उस प्रतिशोध की ज्वाला में तप कर, मैं क्रिकेटर बनने की बजाय डॉक्टर बन गया।
डिग्री पूरी कर ली। डॉक्टर ‘बनना’ अभी बाकी था। वह रोब, वह शह, वह व्यस्तता, वह पके बाल, वह ऐनक, वह गम्भीरता, वह ममत्व, वह ब्रह्मसत्यवादिता, वह नेटवर्क, वह असमाजिकता, वह नये ब्रांड की नयी गाड़ी, वह उठने-बैठने का शऊर, वह अकड़, वह चमक, वह आत्मविश्वास, वह अनुभव, वह खानदानी हुनर, वह अकूत धन। कुछ भी तो नहीं था।
उन्हीं दिनों मेरी उनसे मुलाकात हुई। वह जो इस डिग्रीधारी को डॉक्टर बना सकती थी, जैसे सामंत-पुत्रों को परिचारिकाएँ पौरुष प्रदान करती थी। यह दीक्षा-संस्कार है, जो हार्वर्ड वाले भी नहीं सिखाते। मैं तो छोटे-मोटे सरकारी मेडिकल कॉलेज से फूट कर अभी निकला ही था।
मैंने एक भीड़-भाड़ मुहल्ले की रेकी कर एक खोली ढूँढ ली। नीचे अंडे की दुकान थी, महिलाओं का कस्बाई ब्यूटी पॉर्लर था, एक स्टेशनरी दुकान, और एक छुटभैया प्रोपर्टी-ब्रोकर। सड़क के दूसरी तरफ एक मोची बैठता था, और एक सरकारी ऊँची दीवाल थी, जो अनौपचारिक पेशाबखाना भी बन गयी थी। अंडे के दुकान के बगल से ही सीढ़ी ऊपर जाती, और सबसे पहले मेरी खोली मिलती। मेरे साथ की खोली में एक दाँत के डॉक्टर, और उनकी अगली खोली में एक कम्प्यूटर-मोबाइल ठीक करने वाला। एक और खोली थी, जो अक्सर बंद ही रहती। वहाँ कोई बोर्ड भी नहीं टँगा था। मैं वहाँ से पाँच सौ मीटर दूर एक बड़े अस्पताल में नौकर भी था। वहाँ के मालिक को जब मालूम पड़ा कि मैंने अपनी खोली डाल ली है, तो कमरे में बुला कर मिठाई का डब्बा और निलम्बन-पत्र साथ ही पकड़ा दिया। डाकसाब बड़े दिलदार व्यक्ति थे, और मुझे कई बार मालदीव ले जाकर सुंदरियों के साथ मौज करने का प्रस्ताव देते रहे थे। मैं इस फेर में रोज वर्जिश भी करता, लेकिन उनकी विजय माल्या जैसी तस्वीरें ही देखता रहा। कभी उन्होंने इस व्यसन में मुझे भागी नहीं बनाया। वह जितने दिलदार थे, उनके पिता उतने ही मितव्ययी। वह अपने अस्पताल की फोटोकॉपी मशीन के बजाय बाज़ार की एक फोटोकॉपी दुकान से ही कॉपी कराते। उनका गणित था कि इससे चालीस प्रतिशत तक बचत होती है। और इसके लिए वह किसी स्वास्थ्यकर्मी को नहीं दौड़ाते, वह खुद अपने एक पुराने स्कूटर पर बैठ कर जाते, और फोटोकॉपी करा लाते। वह अक्सर मुझे कहते कि मैंने एक राशन की दुकान से शुरुआत की, बेटे को डॉक्टर बनाया और आज इतना बड़ा अस्पताल खड़ा किया। मैं निलम्बन के बाद भी उनसे गूढ़-ज्ञान लेता रहा। उनके पास बाज़ार को मैनिपुलेट करने की सभी चाभियाँ थी। जब अस्पताल के सभी रिसेप्शनिस्ट युवतियों को घुटनों तक की स्कर्ट दी गयी, मुझे लगा कि यह उनके ठरकी बेटे का दिमाग है। लेकिन मालूम पड़ा कि यह तो सत्यनारायण भगवान के नियमित पूजक उन बुढ़ऊ का आइडिया है। और यह मास्टर-स्ट्रोक था। उस मुहल्ले क्या, दूर-दराज से लोग कुछ-न-कुछ बीमारी का बहाना बना कर अस्पताल आने लगे।
अस्पताल में मैंने बस एक अच्छा काम यह किया था कि डॉक्टरों के साथ कम और नर्स-वार्डबॉय के साथ अधिक उठता-बैठता। वजह वही थी कि मैं डॉक्टर ‘बना’ नहीं था। मेरी बातें, मेरी चाल-ढाल, और मेरी जेब इतनी ही थी कि वे सर पर बिठा कर रखते। डॉक्टर तो अपनी टशन में रहते। खोली खुलने में यह रणनीति खूब काम आयी, और अस्पताल से छुप-छुप कर मेरी मदद करने वे लोग आने लगे। कोई सफाई कर जाती, कोई मरीज सँभाल लेती, तो कोई बाहर का काम देख लेता। परिवार सा माहौल था। लेकिन, मुझे अभी कुछ काग़ज़ी काम पूरे करने थे। दुकान का लाइसेंस, प्रदूषण का लाइसेंस, मशीन का लाइसेंस, लाइसेंस ही लाइसेंस। जहाँ लाइसेंस, वहाँ रिश्वत। ऐसा मुझे कहा जा रहा था। जब दो-तीन बार यही संदेश मिला, तो सोचा खुद मिल आऊँ।
और यूँ कहिए कि पहली रिश्वत में ही इश्क हो गया।
सरकारी महकमे की हालत तो एक जैसी ही होती है। ग्राहकों की भीड़। एक घनघोर व्यस्तता, और एक मादक सुस्ती कि नींद आ जाए। मैं भी वहीं बेंच पर इंतजार करते ऊँघने लगा। मेरी समस्या है कि पहले मिनट में मेरे आँखों के डोले नींद में घूमने लगते हैं, स्वप्न-संसार में प्रवेश कर जाते हैं। और दूसरे मिनट में खर्राटे का शंखनाद हो जाता है। मुझे कोलाहल में ही नींद आती है। इसकी वजह शायद यह रही हो कि मैं बाल्यकाल से छात्रावास में रहा हूँ। अगर चारों तरफ शांति हो, तो मैं रेडियो या कोई यंत्र जोर से बजा देता हूँ, फिर नींद आ जाती है। उस राजकीय कार्यालय की अराजकता में जो नींद मिली, वैसी फिर न मिली। मेरे सहयोगी ने झकझोर कर जगाया कि मैडम बुला रही है।
मैं हकबका कर पसीना पोछते आधी नींद में ही उठा, और मैडम के कमरे में दाखिल हुआ। न जाने क्यूँ यह लगा कि अभी-अभी इनसे ही तो मिल कर आ रहा हूँ। स्वप्न में। वह मुझे समझा रही थी कि रिश्वत न तुम्हें देना है, न मुझे लेना है। ये अफ़वाह न जाने कौन फैलाता है? आगे की बात चैम्बर में उन्होंने बतायी कि आपके काग़ज़ पूरे नहीं हैं। मैंने अपनी दलील रखी कि मैं पूरे कर देता हूँ। वह मुस्कुरायीं।
मुझसे चार-पाँच साल बड़ी होंगी। छोटी भी हो सकती थी। डिग्री पूरे हुए मेरे दस साल तो यूँ ही निकल गए थे। इनकी तो ग्रैजुएट होते ही नौकरी में लग गयी होगी। ऐनक टेबल पर पड़ी थी, लेकिन नाक पर ऐनक के निशान नहीं पड़े थे। माथे के दोनों छोरों पर, कान के कुछ ऊपर पसीने की बूँदें ज़रूर थी, लेकिन चेहरा रस से लबालब। बाल बेतरतीबी से एक डंडी के सहारे टिके हुए, जैसे किसी फौजी बम में अटका हुआ पिन। साड़ी ऐसी कि कभी धुली न हो, और न कभी पहनी गयी हो। न कोई रंग उतरा था, और न कोई रंग चढ़ा था। गला खाली, मांग खाली। मैं उन्हें निहारता रहा, वह मुझे समझाती रही। और न जाने कब एक रजिस्टर मेरी तरफ बढ़ा, और कब उसके पन्नों के मध्य खाली लिफ़ाफ़े को अलट-पलट कर देखा। यह सब जादुई था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं बाहर भाग कर जाऊँ, फुटपाथ से गुलदस्ता खरीदूँ, और प्रणय-प्रस्ताव रख दूँ। फिर मेरे घर लाइसेंस ही लाइसेंस होंगे। भला जीवन-संगीनी भी मुझसे क्या रिश्वत लेगी? और लेगी भी, तो यह उसका अधिकार होगा। स्त्रीधन। तलाक़ के बाद भी उसकी गिनती नहीं होगी। और यह पुरुष-सत्ता पर कितनी दमदार चोट होगी कि स्त्रियाँ भी रिश्वत लेती हैं। लेकिन स्त्रियाँ रिश्वत रखती कहाँ हैं? पुरुष तो पैंट के अंदर अंत:वस्त्र के करीब एक जेब सिलवाते हैं, और उसमें नोट मोड़ कर खोंस लेते हैं। यह शायद ब्लाउज के अंदर डालेंगी। नोट का उभार स्तन के उभार से मिश्रित हो जाएगा। मजाल है कोई सवाल करे?
मैं कब कमरे से बाहर आया, कब मोटरसाइकिल के पीछे बैठ अपने खोली में पहुँचा, मुझे स्मरण नहीं। न मुझे यह स्मरण है कि मैंने कितनी रिश्वत दी। कुछ होश सँभलने के बाद मैंने फ़ोन लगाया। फिर चल कर अस्पताल तक गया, और वहाँ अपने मित्र स्वास्थ्यकर्मी को पूछा कि कहीं मैंने ग़लती से उन मैडम को चूम तो नहीं लिया? वह हँसने लगा।
उसने कहा, “सर! आप तो पूरे सम्मोहन में थे। न जाने क्या कर जाते? मैं आपको खींच लाया।”
मैंने पूछा, “फिर मैंने क्या किया?”
“मैडम आपसे पैसे की बात कर रही थी, आप कुछ क्रिकेट के मैदान की बात कर रहे थे। आप नशा तो नहीं करते?”
“हाँ! करता हूँ।”
“सर! आप फिर मजाक कर रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा।”
“मैंने भी एक सुंदरी को यूँ रिश्वत माँगते पहली बार देखा”
“अरे सर! क्या सुंदरी? पैसा सबको सुंदर बना देता है। इधर देखो! घुटने तक की स्कर्ट पहना दी, और वेतन सात हज़ार। सबके बाल झाँक रहे हैं टाँगों से।”
“बाल में क्या बुराई है?”
“साहब बोल के गए हैं कि शेव करके आना है, नहीं तो इधर ही कर देंगे। लड़की लोग का छोटा कपड़ा में बाल शेव तो चाहिए सर।”
“तो कपड़े लम्बे कर दो।”
“फिर कस्टमर कम हो जाएगा।”
“भारत में मरीज कभी कम न होंगे। किसे फ़ुरसत है रिसेप्शनिस्ट की टाँगे देखने की?”
“सर! आप अपना आदर्श झोले में डालो और इधर से निकल जाओ। मैडम भी यही बोला। लाइसेंस नहीं मिलेगा।”
“मैं दुबारा मिलूँगा। शिकायत करूँगा।”
“लेकिन आपका काग़ज़ पूरा नहीं है सर। वो बिल्डिंग इल्लीगल है, जिसमें आपका खोली है।”
“रिश्वत देकर लीगल हो जाएगा?”
“सर! बिना रिश्वत तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन है। आप मैडम से दो बार नहीं, दस बार मिलो, शादी कर लो।”
“वह मुझसे शादी क्यों करेगी?”
“सर! प्यार में क्या रिश्वत-विश्वत?”
“एक्जैक्टली! तभी मैंने नहीं दिए।”
शहर में डेंगी बुखार पसरा। मैं एक मिशन अस्पताल जाने लगा था, मुझे भी डेंगी हो गया। यह बात मुझे डेंगी के जाँच से पहले ही मालूम थी, क्योंकि मुझे यह भी मालूम था कि जिसे पूरी दुनिया डेंगू कहती फिरती है, उसका असल नाम डेंगी है। जिसे दुनिया ने प्लेग कहा था, वह भी प्लेग नहीं था। जो मेरे खोली के साथ दुकान बंद रहती थी, वह रात को खुलती थी। वह सस्ता वेश्यालय था, जहाँ घंटे के हिसाब से कमरा मिलता था। वहाँ कोई भी बोर्ड नहीं था। महिला हो या पुरुष, रिश्वत ब्लाउज या पैंट में छुपा कर नहीं रखते। वहाँ तो तरकारीवाली मेहनत की कमाई रखती है, या वह बस में खड़ा मुसाफिर रखता है कि कोई जेब न काट ले। जो तालाब भरा गया था, वह क्रिकेट का मैदान तो कभी था ही नहीं। कौन बेवकूफ़ एक मछली-मखाने के जलाशय को भर कर बाल-क्रीड़ा केंद्र बनाना चाहेगा? और मैडम? वह तो शादी-शुदा थी, और पति-पत्नी मिला कर खूब कमाते थे।
“सर! आपके शटर में ऑयलिंग कर दूँ? इधर सब दुकान के शटर में मैं ही करता हूँ। सौ रुपया में साल भर कोई परेशानी नहीं।”
“हाँ! हाँ! कर दो। लेकिन आधे घंटे में मरीज आने शुरू हो जाएँगे। जल्दी करना। मैं जरा टहल कर आता हूँ।”
मैं सड़क के दूसरी ओर मोची के पास अपने जूते पॉलिश कराने लगा, और अपने क्लिनिक को देखने लगा। इस अंडे की दुकान की भीड़, इस ब्यूटी पार्लर में जमा महिलाएँ, ये स्टेशनरी खरीदते बच्चे, ये मोबाइल रिपेयर कराते लोग, सब कितने नॉर्मल थे। मेरे पीछे की दीवाल जिसका निचला हिस्सा पीला पड़ गया था, वहाँ मच्छर भिनभिना रहे थे। शहर में डेंगी फैला था। क्लिनिक की शुरुआत का इससे शुभ मुहूर्त भला और क्या था?
कुछ महीनों बाद डोबरमैन कुत्ता खरीदने निकला, तो एजेंसी वाले ने कहा कि कुत्ते तो मँगाने पड़ेंगे। फिर पड़ोस के दंत-चिकित्सक ने सुझाया कि कुत्तों के भी अनाथालय होते हैं, और आप कुत्ता मुफ्त में गोद ले सकते हैं।
मैंने पूछा, “डोबरमैन मिलेगा?”
उसने कहा, “मिल सकता है, लेकिन उसकी हालत अच्छी न होगी। यह तो समाजसेवी लोग खरीदते हैं।”
“फिर तो यह मेरे काम की नहीं। जिसने रिश्वत देकर क्लिनिक खड़ा किया हो, वह किस मुँह से अनाथ कुत्ता पालेगा? उसे तो वह एक नजर में काट लेगा।”
“लेकिन डोबरमैन ही क्यों?”
“यह बात अब पुरानी हुई। खैर, अगले हफ्ते मालदीव जा रहा हूँ। लौट कर सुनाता हूँ।”
“अबे, कहाँ मालदीव? अपने तो पड़ोस में ही…”
“तुमने क्या पूछा था? डोबरमैन ही क्यों?”
और हम फूहड़ हँसी हँसने लगे। हम दोनों क्लिनिक में बैठे गणेश जी के सामने एलइडी का दिया ऑन कर, सीढ़ीयों से छत पर गए, और पानी टंकी के पीछे छुप कर सिगरेट फूँकने लगे। उस दिन कमाल हो गया, मेरे सिगरेट से धुएँ के छल्ले बनने लगे, जो इतने सालों से नहीं बन पा रहे थे। आखिर मैं वह बनने लगा था, जो इतने सालों से नहीं बन पा रहा था।
(यह रचना साहिंद में अप्रेल 5 2020 को प्रकाशित हुई थी।)