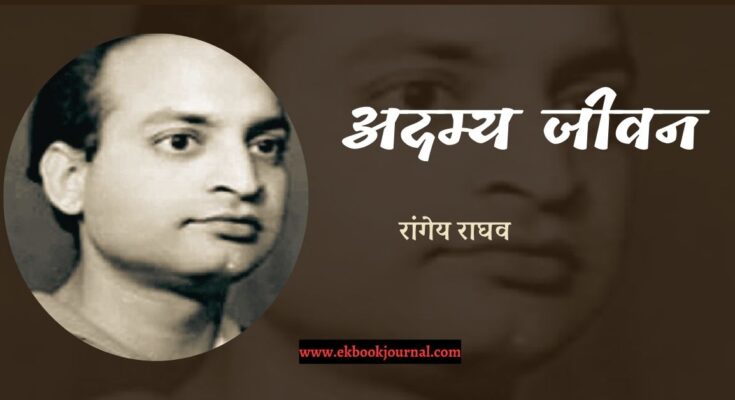हम पगडंडियों से बढ़ते जा रहे थे। सूर्य आकाश में चढ़ने लगा था। कहीं-कहीं कोई किसान किसी पेड़ की छाया में बैठा दिख पड़ता था। सर्वत्र नीरवता छा रही थी। आकाश में बादल तैर रहे थे, जिन्हें देखकर खेतों से एक सोंधी-सी उसाँस उमंग उठती थी। दूर हरियाली की लहर तेज चलती हवा की तरंगों पर गूँज-सी उठती थी। हरी-भरी पृथ्वी पर कभी-कभी बादलों के छा जाने से कहीं धूप और कहीं छाया, बरबस ह्रदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। किंतु मेरे साथी को जैसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बायाँ हाथ उठाकर वह कह रहा था, “वही है शिद्धिरगंज, देख रहे हो न वह ताड़ का पेड़?”
दूर – लगभग मील भर की दूरी पर – कालनेमि की तरह खड़ा था लम्बा ताड़ का पेड़। जैसे-जैसे हम उस पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, आकाश के बादल लहरों की तरह उस पर केंद्राकार आ-आकर फैल जाते थे। वर्षों से ताड़ का पेड़ वह इसी तरह खड़ा है और वर्षों से उसके हिलते पत्तों ने बादलों की मर्मर सुनी है, किंतु आज उसकी छाया में मनुष्य विक्षुब्ध हैं।
मेरा साथी चुपचाप बढ़ता चला आ रहा था। एकाएक वह ठिठककर खड़ा हो गया। मैं उसके पीछे था। मैंने उसका कन्धा पकड़कर कहा, “भट्टाचार्यजी, क्या हुआ?”
“कुछ नहीं, गाँव आ गया।”
“गाँव! पर यहाँ तो कोई बस्ती शुरू ही नहीं हुई।”
साथी की आँखों में निराश मुस्कराहट काँप उठी, “नहीं क्यों कहते हैं आप? वह देखिए, वह…!” और उसने अपना हाथ सामने की ओर उठा दिया। मिट्टी का एक छोटा सा ढूह घास में से अपना अनगढ़ सिर निकाले चुपचाप पड़ा था। मैं समझ नहीं सका कि क्या यही गाँव है? मैंने कहा, “यह तो मिट्टी का एक ढूह मात्र है।”
“इस गाँव की यही तारीफ है। आदमी मिलने से पहले यहाँ कब्रें शुरू हो जाती हैं।”
मैंने देखा, वह सचमुच कब्र थी। कच्ची मिट्टी, सिर पर कोई साया नहीं, चारों तरफ कोई घेरा नहीं। हम लोग बढ़ चले। प्रतीक्षा की-सी नीरवता में प्रायः हर पाँच-दस कदम पर एक-न-एक कब्र थी। मेरा ह्रदय काँप उठा।
सामने एक टूटा घर था– भग्न, विध्वस्त, मानो तूफ़ान में उसका वैभव नष्ट हो गया था। और उसके सामने केले के पेड़ों की शीतल और मनोरम छाया में चौदह कब्रें आँखें मूंदे पड़ी थीं। एक लड़का, जो वहीं बैठा एक आम की गुठली का सब-कुछ खा जाने में लगा था, अपने आप चिल्ला उठा, “बाबू, एक-एक में दो-दो, तीन-तीन हैं। एक-एक में दो-दो तीन-तीन।”
और वह फिर गुठली को मुँह मारने लगा। भट्टाचार्यजी पेड़ों की घनी छाया में एक पेड़ से सटकर खड़े विश्राम कर रहे थे। वे कहने लगे, “बाहर से तुम्हारी तरह ही बहुत-से लोग आते हैं। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ की एक-एक कब्र से बात करो और हिंदुस्तान के कोने-कोने में जाकर कहो कि जिस ढाके की मलमल एक दिन शहंशाह पहनते थे, आज वहाँ जुलाहे चूहों की तरह मर रहे हैं। बोलो, सुना सकोगे संसार को यह?”
छोटी-छोटी पगडंडियों से होता हुआ यह स्वर कब्रों से टकराकर गूँज उठा और मानो कब्रों से आवाज़ें आने लगीं। चौदह कब्रें– आँखों के सामने एकबारगी उनमें सोए कंकाल तड़प उठे और नाच उठे यातना से व्याकुल, भूख से तड़प-तड़पकर मरते हुए प्राणियों के चित्र।
राह में एक वृद्ध अपनी चटाई पर बैठा करघा चला रहा था। हम लोग उसी के पास जाकर रुक गए। वृद्ध ने हमारी ओर दृष्टि उठायी। भट्टाचार्यजी ने कहा, “दादा, आगरे से आए हैं यह, यहाँ का हाल देखने।”
“जियो बेटा, जियो!” वृद्ध ने गदगद स्वर से कहा, “यह आगरा कहाँ है?”
“हिंदुस्तान में?”
“हिंदुस्तान से आए हो आओ, बैठो बेटा, आओ।” उसने चटाई की ओर इशारा किया। हम लोग बैठ गए। वृद्ध कहने लगा, “जो देखने लायक था, वह तो ख़त्म हो गया। मगर तुम आए हो, तो देखो, आगे जाने क्या हो?” वह क्षण-भर चिंतित-सा दिखाई दिया। फिर भी एकाएक स्वर बदलकर उसने कहा, “तुम हमारे मेहमान हो, भैया! आराम से बैठो ज़रा। हम भूखे हैं; मगर तुमने जो इतना कष्ट किया है, किसलिए? हमें अपना समझकर ही न? फिर तुम समझते हो, हमें इसका ज्ञान नहीं है?”
मैं चुप बैठा रहा। भट्टाचार्यजी कहने लगे, “दादा, कष्ट-वष्ट की बात छोड़ो; इन्हें इस गाँव के कुछ हालचाल बताओ।”
वृद्ध एक क्षण चुप रहा। फिर बोला, “हालचाल? वह देखो….!” और उसने एक कब्र की ओर इशारा किया और कहता गया, “शिद्धिरगंज के हालचाल सुनना चाहते हो? एक-दो-तीन, गाँव के एक छोर से दूसरे छोर तक गिनते चले जाओ। कसम है, अगर तुम किसी को हाय-हाय करते पाओ। नहीं, आज कुछ नहीं है। था एक दिन, जब गाँव में रात-दिन रोने-कराहने से सिवा और कुछ भी सुनाई नहीं देता था, मगर अब तो वह सब-कुछ नहीं।”
वास्तव में हमें कोई भी रोता नहीं दिखा। सब मानो अपने-अपने काम में लगे थे। मैंने देखा, डॉक्टर चुपचाप घरों की ओर देख रहा है। बांस के सुंदर-सुंदर झोपड़ें! सदियों से बंगाल – हम लोगों – पर बार-बार बाहरी हमले हो रहे, मगर आक्रमणकारी कभी भी यहाँ की शस्य-श्यामला पवित्र भूमि को नहीं रौंद सके। यहाँ मनुष्य को इतना समय मिल चुका था कि वह बैठकर आराम से इतने सुंदर और स्वच्छ घर बना सकता। और आज वही घर निर्जनता की अर्गला लगाए मूक खड़े थे! अकाल ने उनपर अपनी जो वीभत्स छाया डाली थी, उसका धुँधलका अभी तक भी मानो कोनों में छिपा बैठा था।
मैं देख रहा था, जिनके शरीर में केवल हड्डियाँ ही शेष थीं आज भी उनमें जीवित रहने का साहस था। अकाल आया, बीमारी आई और फिर दूसरे अकाल की गहरी आँधी भी क्षितिज पर सिर उठाने लगी है, किंतु अविचलित हैं यह! किसलिए? इसीलिए न कि वह जनता किसी से भी दब नहीं सकती। एक दिन विजेताओं ने इन्हें कुचला था, आज भी मनुष्य का स्वार्थ और भीषण व्यापार इन्हें निचोड़ रहा है, किंतु यह तो अभी तक अदम्य, अविजेय हैं!
बूढ़ा फिर कहने लगा। अबके उसका स्वर दृढ़ था, “इस गाँव में आज घरों पर किसकी दृष्टि ठहरेगी, भैया? इधर देखो, वे जो छाया में सो रही हैं चुपचाप, वे मिट्टी की कच्ची कब्रें, गिनकर देख लो, अगर पाँच सौ से कम दिखाई पड़ें! और एक-एक में एक ही आदमी दफनाया गया हो, यह भी कोई ज़रूरी बात नहीं है। यह है हम मुसलामानों की बात। और अगर तुम सुनना चाहते हो कि हिंदू क्यों नहीं मरे, तो जाकर शीतलक्खा की धारा से पूछो कि क्यों तू शिद्धिरगंज के सैकड़ों किसानों को बहा ले गयी, जिनकी हड्डियों तक का आज पता नहीं?”
और वह सहसा मुस्करा उठा। मैंने देखा और समझने की चेष्टा की। मृत्यु ने उसे विक्षुब्ध कर दिया था। उसने कहा, “इस गाँव में करीब-करीब हर घर में मौत हो चुकी है। हज़ारों व्यक्ति मर चुके हैं, मगर सब तो नहीं मर सकते थे, और शायद सब नहीं मरेंगे, मगर कौन जाने, आगे क्या होगा?”
इस समय कुछ और लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए थे। रहमत, जो अपने ताने को एक दफा ठोककर उठ आया था, आकर वहीं बैठ गया था। चर्चा चल पड़ी। रहमत कहने लगा, “हाँ, काफी लोग मर गए हैं।”
“तुम्हारे घर में कितने आदमी थे?”
“पच्चीस थे, जिनमें बीस मर गए। अब पाँच बाकी हैं।” और उसने अब्दुल के हाथ से हुक्का लेकर धुआँ उगलना शुरू कर दिया। बोला, “यह मिल जाती है, भैया बस!” उसने तम्बाकू की ओर इशारा किया। और मुस्करा उठा। पहले वृद्ध की वह क्षुब्ध आकृति अब कुछ दीन-सी हो गई थी – मानो पहले जो व्यक्तिगत दुःख सजीव होकर चारों ओर हाहाकार कर उठा था, अब सामूहिक रूप में केवल साधारण-सा होकर चक्कर काटने लगा है। कुछ देर बाद रहमत ने एक लम्बी साँस छोड़ी और फिर गम्भीर भाव से कहा, “आने दो, जो-कुछ आएगा, उसे झेलेंगे।”
पगडंडी पर मरियल भुखमरे कुत्ते भूँक उठे, मानो रहमत की बात को समझकर उन्होंने उसका समर्थन किया हो। रहमत ने फिर कहा, “उन दिनों तीस-चालीस आदमी रोज़ मरते थे। अकाल तो खत्म हो गया, मगर बीमारियों ने जो पकड़ा, तो उनसे अभी तक गला नहीं छूटा।”
डॉक्टर ने पूछा, “क्या-क्या बीमारियाँ हैं यहाँ?”
रहमत बिना सोचे ही रटी हुई-सी बात बतला गया, “मलेरिया, बसंत (चेचक) और चर्म-रोग।”
मैंने चारों और दृष्टि उठाकर देखा। लोगों के गालों की हड्डियाँ उभर आयी थीं, आँखों में सूजी-सी ललाई छा रही थी, किसी-किसी के गले में सूजन थी। उन्हें लक्ष्य कर डॉक्टर ने मुझसे कहा, “करीब-करीब सभी या तो मलेरिया के शिकार रह चुके हैं या अब भी मलेरिया-ग्रस्त हैं।”
एक चंचल लड़का कहने लगा, “आपको अकाल की बात कुछ नहीं मालूम। यहाँ चावल किसी भी दाम पर नहीं मिलता था। तीन-साढ़े-तीन सौ आदमी तो इस गाँव को छोड़ गए। भुखमरे नहीं, तो….।” और उसकी झँकारती हँसी एकबारगी ठिठुरती-सी फैल गयी। उसकी बगल में एक लड़की खड़ी थी, कोई नौ-दस बरस की। यह बीच में ही बोल उठी, “भूल गया न कि अभी भी कई भुखमरे हैं, जो यहाँ लंगरखाने में खा रहे हैं।”
सहसा रहमत ने कहा, “अब्दुर्रहमान, आओ, इधर बैठो।”
अब्दुर्रहमान आया ही था कि एक आदमी कह उठा, “इसके घर में सोलह आदमी थे, जिनमें से यह अकेला बचा है।” अब्दुर्रहमान ने निराश नयनों से हमारी ओर देखकर कहा, “क्या बताऊँ बाबू, अफसोस सिर्फ यह है कि अब घर भी नहीं रहा। रहमत के यहाँ पड़ा रहकर इन्हें दुःख देता हूँ।”
रहमत हँस पड़ा। वह बोला, “क्या बात, कहते हो, अब्दुर्रहमान? तुम तो एक आये हो, मगर और जो उन्नीस की जगह बाकी है…।” और सब हँस पड़े। इतने में सामने से घूँघट काढ़े एक स्त्री निकली। हठात पूछ बैठा, “रहमत, क्या तुम्हारे गाँव में स्त्रियों को अपनी इज्जत बेचने पर भी उतारू होना पड़ा था?”
रहमत के मुँह पर एक काली छाया फैल उठी। उसने पल-भर कुछ नहीं कहा। फिर गम्भीर स्वर में कुछ सोचकर बोला, “बाबू, बात तो बुरी है, मगर है सच। कुछ थीं ऐसी, मगर बुरा कहकर भी कितनी बुरी थीं वे, मैं नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि जैसे इतने मरे, वे भी मर जातीं, तो हर्ज ही क्या था? पर मैं सोचता हूँ, मर जाना क्या सहज है? कोई क्या अपने-आप मार जाना चाहता है? खैर, जाने दीजिए, इस बात को जाने ही दीजिए।”
अब्दुर्रहमान हर बार कह उठता था, “क्या करेंगे हम? क्या, बताइए न? उसके स्वर में अथाह निराशा और विवशता गूँज उठती थी। “चावल का भाव अब भी 18 या 19 रुपये में है। कहाँ से खरीदें हम? गाँव में अधिकांश अब भी एक वक्त ही खाते हैं। और चावल खरीदने वाले भी सब ही तो चावल नहीं खाते, कई तो शकरकंद के सहारे ही जी रहे हैं।”
“इतनी आमदनी नहीं, फिर बताओ”, रहमत कहने लगा, “कोई कैसे खरीदे? अकाल खत्म हुआ ही कब, जो दूसरा शुरू होगा? हमने कच्ची कब्रों में कई लाशों को बिना कफन में गाड़ दिया। आपको शायद मालूम न हो, हम मुसलमानों के यहाँ लाश को कफन में बाँधकर गाड़ने का कायदा है। मगर कायदा क्या करे, जब ज़िंदों के लिए भी कपड़ा नहीं है, तो मरों की क्या कीमत है बाबू?”
उसका यह प्रश्न उसका अपना नहीं था। उसने अनजाने नहीं, जानबूझकर ही उँगली उठाई थी उधर, जिधर मनुष्य को नंगा रखकर मनुष्य ने अपने मुनाफों के लिए बेशुमार कपड़ा तालों में बंद कर रखा था, जहाँ वस्तु मनुष्य के लिए न होकर पैसे के लिए थी। कितना बड़ा व्यंग्य और विद्रूप था यह कि आज कपड़ा बनानेवाले स्वयं नंगे थे!
हम लोग काफी देर तक बैठ चुके थे। एक लड़का कह उठा, “चलिए बाबू, गाँव देखिए।” और हम लोग उठे। वहाँ एकत्र हुए लोगों में से कुछ ने हमें प्रणाम किया, कुछ ने आशीर्वाद दिया और हम लोग चल दिए।
कहीं-कहीं कब्रें टूट गयी थीं। सामने के दो घर बिलकुल टूट गए थे, उनके केवल चबूतरे बाकी थे। सामने एक गाय घास चर रही थी। पेड़ों की छाया में अनेक कब्रें सोयी पड़ी थीं। लड़के ने कहा, “यह है आदू मियाँ का घर। मर गया बेचारा! उसके घर में उन्नीस आदमी थे, अब कोई भी नहीं बचा है।” वायु सनसनाती हुई बह गई। आदू मियाँ यहाँ बैठकर हँसता था, आज उसका कोई पता नहीं। लड़के को घर का एक-एक प्राणी याद था – अभी कल ही की तो बात थी। मगर निर्विकार खड़ा था। मानवी भावनाएँ कितनी कठोर हो गयी थीं। सहसा आगे चलकर वह एक कब्र पर खड़ा होकर कहने लगा, “बाबू, यह मेरे बाप की कब्र है। बस, मैं इतनी कब्रों में से इसे पहचानता हूँ। वह मुझे बहुत प्यार करता था। सचमुच वह मेरे लिए ही मर गया।” लड़का कुछ ठिठुर गया। मैंने देखा, डॉक्टर चौंक उठा। वह मुझसे बोला, “यह मुसलमान होकर कब्र पर खड़ा है? हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता।”
भट्टाचार्यजी मुस्करा उठे। उन्होंने लड़के से वही प्रश्न दुहरा दिया। लड़का क्षण-भर चुप रहा। फिर हँस पड़ा, “यहाँ तो सब ऐसा ही करते हैं, बाबू! कहीं पैर रखने की भी तो जगह नहीं है। कहाँ तक कोई कब्रों को बचाता हुआ, उनका चक्कर देकर चले? इतनी ताकत है कितनों में?”
हम लोग आगे बढ़े। भट्टाचार्यजी एक आदमी से कुछ बातें करने लगे। वह आदमी कह उठा, “गाँव-कमेटी के, यूनियन-बोर्ड के मेम्बर सब चोर हैं, चोर! कोई हमारी परवाह करता है? रिश्तेदारों को कारड देते हैं, अपनों को देते हैं, हमारी क्या पूछ…?” दूसरा आदमी चलते-चलते रूककर कह उठा, “हममें एकता नहीं है, वर्ना क्या मजाल कि वह अपनी मनमानी करें!”
तब तो बंगाल अभी जीवित है! आज भी वह अपना रास्ता खोज निकालना जानना और चाहता है। भूख से व्याकुल होकर भी यह भारत का संस्कृति-जनक सिर झुकाने को तैयार नहीं है। आज भी वह इन सब आँधी-तूफानों को झेलकर फिर से विराट रूप में फूट निकलना चाहता है। सचमुच कोई इनका कुछ नहीं कर सकता। यदि जनता में चेतना है, तो इन्हें भूखों मारनेवाले नर-पिशाच अनाज-चोरों का अंत दूर नहीं है।
एकाएक लड़का एक झोंपड़े के पास पहुँचकर रुक गया। हमने देखा, भीतर कुछ जुलाहे साड़ियाँ बुन रहे थे। लड़के ने कहा, “ढाके की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं न, बाबू! अब यही दो-चार घर रह गए हैं, और कुछ दिन बाद शायद….।” वह कहते-कहते चुप हो गया। जुलाहे काम छोड़कर हमारी ओर देख रहे थे। सामने ही एक औरत बैठी थी। वह विधवा थी। उसके घर के दस आदमी मर चुके थे – और सामने केवल तीन अनगढ़ कब्रें थीं।
अधिकांश घरों की टीनें उखड़ गयी थीं। और न जाने कितनों ने भूख से लड़ने के लिए अपनी टीनें बेच दी थीं। भट्टाचार्यजी ने उँगली से दिखाते हुए कहा, “वह सामने एक भद्रलोक का घर था। उसे भी टीन बेच देनी पड़ी क्योंकि…!” सहसा वह रुक गए। बात पलटकर उन्होंने कहा, “वे जो टीनें दिखाई दे रही हैं उखड़ी-उखड़ी, इसकी वजह यह नहीं कि उसके मालिक उन्हें बेचना नहीं चाहते थे, मगर इसलिए कि उनमें इतनी ताकत ही नहीं रही थी कि उठाकर इन्हें बाजार तक ले भी जाते और यही कारण है कि…।”
मैंने देखा, घर के चबूतरे के बीचोंबीच एक कब्र थी। यह भी एक मनुष्य था, जो अपने घर का वक्षस्थल फाड़कर सो रहा था। फोड़ों की तरह वे कब्रें जगह-जगह सूजी हुई-सी दिखाई दे रही थीं।
धूप तेज हो चली थी। हम हाट में पहुँच गए थे। मछलियों की बू वातावरण को भेद रही थी। एक बूढ़ा व्याकुल-सा भागा जा रहा था। भट्टाचार्यजी ने बताया, “उसे उस समय तीव्र ज्वर था, जिसके कारण उसका दिमाग ठीक नहीं था।” हाट के एक कोने में स्थानीय डॉक्टर की एक डिस्पेंसरी थी, छोटी-सी, गमगीन-सी। डॉक्टर के दिल में यह मुफ्त दवाखाने खोले जाने की बात जमती नहीं थी। आखिर वह फिर क्या खाएगा? हमारे डॉक्टर ने उससे बातचीत की। उसके पास न कुनैन थी, न सिन्कोना, और गाँव में हर घर में मलेरिया का रोगी था, बच्चे की तिल्ली और जिगर बढ़े हुए थे।
दवाखाने की एक बेंच पर बैठा एक आदमी कह रहा था, “हर एक चीज़ चोर-बाजार में है, हर एक चीज़ पर मुनाफाखोरी हो रही है, कोई करे तो क्या करे?”
एक औरत, जो पास में खड़ी थी, कहने लगी, “तुम डॉक्टर हो? पहले क्यों नहीं आए? जाने कितनी जानें बच जाती! यहाँ एक सरकारी दवाखाना है जिसमें कोई खास दवाई नहीं, मरीजों की कोई खास तवज्जोह नहीं। कहाँ, ढाकेश्वरी मिल नं. 2 में तुम्हारा दवाखाना है? अब वहीं आएँगे कल से, चार-पाँच मिल तो हैं ही… ।”
उस समय उस औरत की बात की अनसुनी करके खैराती अस्पताल का एसिस्टेंट डॉक्टर मुझसे कह रहा था, “हमने 75 फीसदी आदमियों की हालत सुधार दी है…।” भट्टाचार्यजी मुस्करा रहे थे। एक ओर हमारे शासक बोल रहे थे, दूसरी ओर वही बात जनता कह रही थी। सामने अनेक जर्जर रोगी खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे – बुझी हुई आँखें, उभरी हुई पसलियाँ और वही भयानक चर्म-रोग!
यहाँ से हम लंगरखानों की ओर चल दिए। लंगरखाने और जगह बंद हो गए हैं, किंतु यहाँ अभी तक खुले हैं। खुले हुए मैदान में, पेड़ों की छाया में, तीन भट्टियाँ खुदी हैं। एक बड़ों का लंगरखाना है, जहाँ खिचड़ी बँटती है। करीब सौ आदमी आज भी उसी पर पलते हैं। मैली-कुचैली औरतों के जमघट में कुछ बैठी चूल्हा फूँक रही थीं। एक औरत ने बताया, कि बच्चों के दो लंगरखाने हैं – एक हिन्दू, एक मुसलमान। दोनों में सौ-सौ बच्चे खाते हैं। साढ़े सात सेर खिचड़ी बँटती है और कुछ मछली, बस इतना ही। किसी तरह लोग जी-भर रहे हैं। भट्टाचार्यजी ने बताया कि फ्रेंड्स एम्बूलेंस यूनिट इन्हें चला रहा है।
मैं और भट्टाचार्यजी आगे चल पड़े। फिर हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भट्टाचार्यजी कहने लगे, “तुमने देखा, साढ़े सात सेर? सौ में कितना पड़ा?”
सामने भट्ठी में से धुआँ निकलकर ऊपर घुमड़ रहा था। आज सारा बंगाल महानाश की आग पर लटका भुन रहा है और चारों ओर से राक्षस मानो उसे चबा जाना चाहते हैं। इतने में डॉक्टर आ गया। उसके साथ एक औरत थी, जो रो रही थी। मुझे बड़ा विस्मय हुआ। यहाँ लोग अभी तक रो सकते हैं। तब तो इनमें ह्रदय है। वह कह रही थी, “दवाखाना, लेकर अब आए हो? पहले आते, तो मेरे बच्चे बच जाते…!” अरे, वह माँ थी। उसके छह बच्चे मर गए थे और सिर्फ दो बचे थे।
“मैं अब यहीं लंगरखाने में काम करती हूँ। किसी तरह पेट भर जाता है। भीख नहीं माँगी जाती, बाबू…!” और वह फिर रो पड़ी, “मेरे बच्चे…!” दिल कड़ा कर हम लोग वहाँ से चल दिए। वह आँखों में आँसू-भरे हमें शत-शत आशीर्वाद देती-सी ज्यों की त्यों खड़ी रही।
खेतों में कब्रें चुपचाप उदास-सी सोयी पड़ी थीं, जिन्हें चिथड़ों में लिपटा एक बुड्ढा एक पेड़ की छाया में बैठा विरक्त भाव से देख रहा था। एक टूटी-सी दीवार में तीन आले अब भी खड़े थे, मगर घर नहीं थे। आठों घर विध्वस्त पड़े थे। उनके सामने बराबर-बराबर में तीस कब्रें पड़ी थीं और एक नवयुवक, जो देखने में बूढ़ा लगता था, उनकी ओर देख-देखकर मुस्करा रहा था। वे सब एक दिन जुलाहों के घर थे, पर अकाल के ताने और बीमारियों के बाने ने सहसा उनके जीवन-व्यापार का अंत कर दिया था।
“दिन में नहीं, दिन में नहीं, रात को”, भट्टाचार्यजी कहने लगे, “गाँव में कब्रिस्तान की-सी छायाएँ नाचने लगती हैं। शिद्धिरगंज कभी भी नहीं भूलेगा कि एक दिन आदमी के बनाये अकाल ने उसका सत्यानाश कर दिया था। जो आदमी अपनी हड्डियों से – दधीचि की हड्डियों से यह अमर कथा लिख गए हैं, बंगाल उनकी ज्वलंत स्मृति को कभी नहीं भुलाएगा।”
मेरे मुँह से हठात निकल गया, “उसे हिंदुस्तान कभी नहीं भुलाएगा भट्टाचार्य जी, मानवता उसे कभी नहीं भुला सकेगी।”
डॉक्टर आगे-आगे चल रहा था। हम लोग लौट रहे थे। नदी की पतली धारा में कुछ नंगे लड़के नहा रहे थे, जिनकी पतली हड्डियों से टकराकर छोटी-छोटी लहरें मानो निराश-उदास लौट जाती थीं। उन्होंने हमें देखा और समवेत स्वर से चिल्ला उठे, ‘इंकलाब ज़िंदाबाद! इंकलाब ज़िंदाबाद!!’
गर्व से मेरी छाती फूल उठी। कौन कहता है कि बंगाल मर गया है? जहाँ भूख और बीमारियों से लड़कर भी मनुष्यों के बालकों में क्रांति को चिरजीवी रखने का अपराजित साहस है, वह राष्ट्र कभी भी नहीं मर सकेगा। हड्डी-हड्डी से लड़नेवाले यह योद्धा जीवन की महान शक्ति को अभी तक अपने में जीवित रख सके हैं। संसार कहता है, स्टालिनग्राड में लोग खंडहरों में से लड़े थे और उन्होंने दुश्मन के दाँत खट्टे कर दिए। उन्होंने बर्बरता की धारा को रोककर रूस को गुलाम होने से बचा दिया। किंतु मैं पूछता हूँ, क्या शिद्धिरगंज दूसरा स्टालिनग्राड नहीं? मनुष्य भूख से तड़प-तड़पकर यहाँ जान दे चुके हैं, वे भीषण रोगों का शिकार हो चुके हैं, उनके घर खंडहर हो गए हैं, कब्रों से ज़मीन ढक गयी है, नदियों में लाशों की सड़ांध एक दिन दूर-दूर तक फैल गयी थी, किंतु मनुष्य का साहस जीवित है। आज भी बंगाल के बच्चे क्रांति को नहीं भूले हैं। क्या इन योद्धाओं ने भारतीय संस्कृति की जड़ों पर होने वाले आघात को सहकर आज संसार को यह नहीं दिखला दिया कि जनशक्ति कभी पराजित नहीं हो सकती, वह कभी मर नहीं सकती? जब फासिस्तवाद से भी बर्बर नर-पिशाच मुनाफाखोरों ने अनाज पर बैठकर जहर उगला, कपड़ा-चोरों ने उनकी बहू-बेटियों को निर्लज्ज होने दिया, तब भी क्या इन्होंने सिर झुकाया? नहीं, ये वीरों की तरह लड़े हैं। आज शिद्धिरगंज की पृथ्वी शहीदों के मजारों से ढक गयी है। युग-युग तक संसार को याद रखना पड़ेगा कि एक दिन मनुष्य के स्वार्थ और असाम्य के कारण, गुलामी और साम्राज्यवादी शासन के कारण, बंगाल जैसी शस्य-श्यामला भूमि में भी मनुष्य को भूख से दम तोड़ना पड़ा था? और लोगों ने उसे पूरी शक्ति से इसलिए झेला था कि मानवता जीवित रहना चाहती थी। उसे कोई मिटा नहीं सकता।
आज अकाल का वह पहला भीषण स्वरुप समाप्त हो चुका है। किंतु रोगों की वर्षा-आंधी के बाद प्रलय उमड़ रही है। और इस समय भी लोग कहते हैं – बंगाल का अकाल समाप्त हो चुका है! पर आज यह कुछ नहीं तो भी महामरण का भीषण नृत्य है। जब हम लोग शिद्धिरगंज से लौट रहे थे, शीतलता की प्रशांत धारा में नहाता हुआ एक आदमी गा रहा था –
‘सोनार बांगला होलो शोंशान, एक साथे सबे चल।’
उसका यह स्वर दूर-दूर तक लहरों पर फैल उठता था।