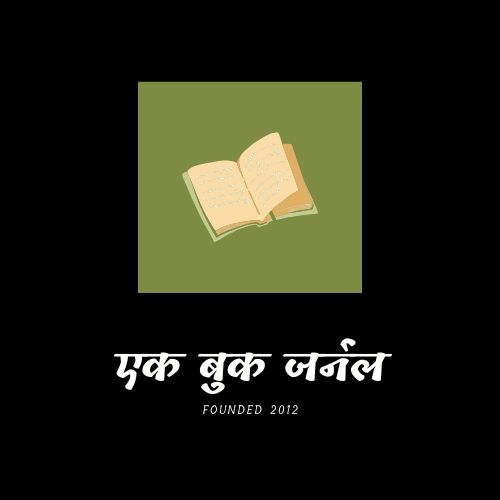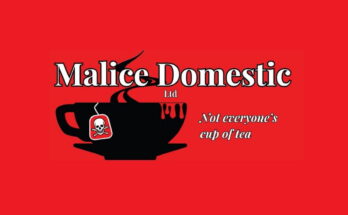- सामाजिक बदलावों के साथ विकसित हो रहे हैं कहानी कहने के तरीके : फहीम अहमद
- छोटी-छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ा बदलाव लाती हैं : कोशी ब्रह्मात्मज
- साहित्य के परस्पर लिप्यंतरण से मजबूत होंगे हिन्दी-उर्दू के संबंध : तसनीफ़ हैदर
01 मार्च, 2025 (शनिवार) नई दिल्ली: उर्दू और हिन्दी के साहित्यकार यदि एक दूसरे के काम को समझते और अपनाते तो हमारे समाज में साहित्यिक-सांस्कृतिक समझ और गहरी हो सकती थी। उर्दू-हिन्दी साहित्य का परस्पर लिप्यंतरण दोनों भाषाओं के सम्बन्ध को मजबूत कर सकता है। जैसे-जैसे समाज में बदलाव हो रहे हैं, वैसे-वैसे कहानी कहने के तरीके भी विकसित हो रहे हैं। हमें अपने समय और समाज को समझते हुए कथा कहने के नए शिल्प को अपनाना होगा। आप छोटी-छोटी चीज़ें करके दुनिया का ध्यान नए तरीकों से सोचने की ओर खींच सकते हैं। यह बातें राजकमल प्रकाशन के स्थापना दिवस पर आयोजित ‘भविष्य के स्वर’ में वक्ताओं ने कही।
राजकमल प्रकाशन दिवस के अवसर पर 28 फरवरी की शाम सहयात्रा उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर विचार-पर्व ‘भविष्य के स्वर’ का पाँचवाँ अध्याय प्रस्तुत किया गया। इस दौरान तीन अनूठी युवा प्रतिभाओं―रंगकर्मी और कहानीकार फहीम अहमद, ज़ाइन मेकिंग और फ़ाइबर आर्ट की आर्टिस्ट कोशी ब्रह्मात्मज और कथाकार तसनीफ़ हैदर ने व्याख्यान दिए। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लेखक, पाठक, संस्कृतिकर्मी, पुस्तकप्रेमी और पत्रकार मौजूद रहे।
व्हाट्सऐप फॉरवर्ड को मिल सकता है आधुनिक लोककथाओं का दर्जा
फहीम अहमद ने अपने व्याख्यान में समकालीन कथा कहन के तरीकों और उसके शिल्प में हो रहे बदलावों की ओर इशारा किया। उनका व्याख्यान ‘बदलते माध्यम और कथा का बदलता चेहरा’ विषय पर केन्द्रित था। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे समाज में बदलाव हो रहे हैं, वैसे-वैसे कहानी कहने के तरीके भी विकसित हो रहे हैं। डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कथाएँ पाठकों तक पहुँच सकती हैं और उन्हें एक नई पहचान मिल सकती है।
उन्होंने एक दिलचस्प सवाल उठाया कि क्या भविष्य में व्हाट्सऐप फॉरवर्ड को आधुनिक लोककथाओं का दर्जा मिल सकता है। यह विचार पहली बार अजीब लग सकता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये संदेश कई लोगों से होते हुए हम तक पहुँचते हैं और हमें लेखक का नाम भी नहीं पता होता, तो यह एक नए प्रकार की कहानी कहने की विधा बन सकती है।
फहीम ने कहा कि जब समाज में अस्थिरता बढ़ी तो उस समय कहानी कहने के तरीकों में भी बदलाव आए। हमें अपने समय और समाज को समझते हुए कहानी के नए शिल्प को अपनाना होगा। यह जरूरी है कि हम अपने कथ्य के लिए उसी समय के अनुसार शिल्प भी तैयार करें।
फहीम ने रंगकर्म और नाटकों की शिल्प संरचना पर विचार करते हुए बताया कि कैसे नाटकों में अस्थिरता और प्रतिरोध का भाव प्रमुख था। उन्होंने सफदर हाशमी के नाटकों का उदाहरण दिया जिसमें शिल्प में स्थिरता की बजाय गतिशीलता दिखाई जाती थी।
उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमारी कहानी और शिल्प की प्रक्रिया को नए रूप में ढाला जाए। युवा लेखक अपने समय के अनुसार कथा और शिल्प में बदलाव ला रहे हैं और अपनी पहचान बना रहे हैं। यह बदलाव न केवल साहित्य में बल्कि समकालीन कला रूपों में भी दिख रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समकालीन लेखक अपने समय की आवश्यकता और समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी रचनाओं का शिल्प और संरचना बदल रहे हैं, जिससे नए आयामों की संभावना बन रही है।
छोटी-छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ा बदलाव लाती हैं
कोशी ब्रह्मात्मज ने अपने व्याख्यान में कहा कि एम्ब्रॉयडरी सिर्फ एक डोमेस्टिक और पैसिव कला नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली प्रतिरोध का माध्यम है जो औरतों द्वारा अनपेड और अंडरएप्रिशिएटेड लेबर की वैल्यू को रीक्लेम करता है। उनका व्याख्यान ‘सोच के शब्द, समझ के धागे’ विषय पर केन्द्रित था।
उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ा बदलाव लाती हैं। मेरा काम यही दिखाता है—कि कैसे आप छोटी-छोटी चीज़ों को करके दुनिया अचम्भित कर सकते हैं, लोगों का ध्यान नए तरीके से सोचने की ओर खींच सकते हैं।
कोशी एक मल्टीडिसिप्लिनरी आर्टिस्ट हैं जो एम्ब्रॉयडरी और ज़ाइन-मेकिंग के माध्यम से व्यक्तिगत अनुभवों और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों को एक्सप्लोर करती हैं। उनका काम ह्यूमर, प्लेफुलनेस, जेंडर, क्रॉनिक इलनेस, और पॉलिटिक्स ऑफ रेस्ट जैसी थीम्स पर आधारित है। उन्होंने कहा कि एम्ब्रॉयडरी, ज़ाइन्स और सेल्फ-पब्लिशिंग जैसे माध्यमों को अक्सर फ्रिंज माध्यम माना जाता है, लेकिन यह मेरे लिए कहानी कहने, प्रतिरोध और विजिबिलिटी के प्रभावशाली माध्यम हैं। मैं अपने काम के जरिए इनविजिबिलिटी को विजिबल करने की कोशिश करती हूँ।
कोशी का काम डिसेबिलिटी, खासकर अपनी खुद की क्रॉनिक इलनेस को विजिबल करने की कोशिश करता है। उनका प्रोजेक्ट SAD (SICK और डिसेबल्ड) एक टैक्टाइल आर्ट है, जो इनविजिबल इलनेस और डिसेबिलिटी को दिखाता है। वे ज़ाइन्स को भी प्रतिरोध और कहानी कहने का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानती हैं। वे खुद कई ज़ाइन्स पब्लिश कर चुकी हैं। उनका काम डिजिटल कल्चर और रियल-टाइम सोशल मीडिया के तेजी से बढ़ते ट्रेंड्स के बीच स्लो और इंटेन्शनल क्रिएशन को बढ़ावा देता है। वे मानती हैं कि आर्ट सिर्फ समाधान नहीं होता, बल्कि एक प्रोसेस होता है, जो इमोशन्स को प्रोसेस करने और सोशल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्स पैदा करने का एक जरिया हो सकता है।
उर्दू साहित्य को लेकर एक नया दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत
तसनीफ़ हैदर ने अपने व्याख्यान में उर्दू और हिन्दी साहित्य के बीच की दूरी, उनके साहित्यिक रिश्ते और समाज में उनके महत्व को रेखांकित किया। उनका व्याख्यान ‘उर्दू-हिन्दी : नया दौर नये सवाल’ विषय पर केन्द्रित था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए उर्दू केवल एक भाषा तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक संस्कृति, एक इतिहास और एक पहचान से जुड़ी हुई थी। घरों में उर्दू अखबारों, किताबों और शायरी के साथ एक गहरी तारतम्यता थी। हम उर्दू साहित्य के बड़े लेखकों, शायरों और कहानीकारों से परिचित थे, लेकिन हिन्दी साहित्य के कई महत्त्वपूर्ण लेखकों से हम अपरिचित रहे।
आज़ादी के बाद, समाज में हिन्दी और उर्दू के बीच एक मानसिक दीवार खड़ी कर दी गई थी। दोनों भाषाओं के साहित्य को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था, हालाँकि दोनों भाषाओं के बोलने वाले एक जैसे लोग थे और दोनों में समान संवेदनाएँ और विचार थे। तसनीफ़ का मानना है कि यदि उर्दू और हिन्दी के साहित्यकार एक दूसरे के काम को समझते और अपनाते तो हमारे समाज में साहित्यिक-सांस्कृतिक समझ और गहरी हो सकती थी।
यह अलगाव सिर्फ़ साहित्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राजनीति और समाज की जड़ों में भी घुस गया। उर्दू को कुछ ख़ास राजनीतिक ताकतों ने धर्म और कट्टरता से जोड़ दिया, जबकि उर्दू साहित्य ने अपनी पहचान हमेशा धर्म से ऊपर रखी है। उन्होंने मीर और मंटो जैसे उर्दू शायरों और लेखकों का उल्लेख किया जिन्होंने धर्म, समाज और राजनीति के खिलाफ़ अपनी रचनाओं में संघर्ष किया।
उर्दू साहित्य को हिन्दी पाठकों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। कई हिन्दी लेखकों के काम उर्दू में नहीं आ सके, जबकि उर्दू के कुछ लेखकों के काम हिन्दी में अनूदित हुए थे। उर्दू-हिन्दी साहित्य का परस्पर लिप्यंतरण दोनों भाषाओं के संबंध को मजबूत कर सकता है।
उन्होंने कहा कि उर्दू साहित्य को लेकर एक नया दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। अगर हम दोनों भाषाओं के लेखकों के विचारों का आदान-प्रदान करें, तो यह हमारे समाज को एक नया दिशा दे सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम दोनों भाषाओं के साहित्य के बीच अनुवाद से ज्यादा लिप्यंतरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करें, जिससे दोनों भाषाओं का सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान-प्रदान आसानी से हो सके।
उर्दू और हिन्दी के रिश्ते पर एक विचारशील नज़रिया प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम उर्दू और हिन्दी को उनके साहित्यिक समृद्धि और सांस्कृतिक महत्त्व के रूप में स्वीकार करें तो हम एक बेहतर समाज की ओर बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें व्यक्तिगत प्रयासों से आगे बढ़कर एक संयुक्त साहित्यिक मंच की आवश्यकता है, जो दोनों भाषाओं के साहित्य को एक जगह लेकर आए और उनके बीच की दूरी को समाप्त कर सके।